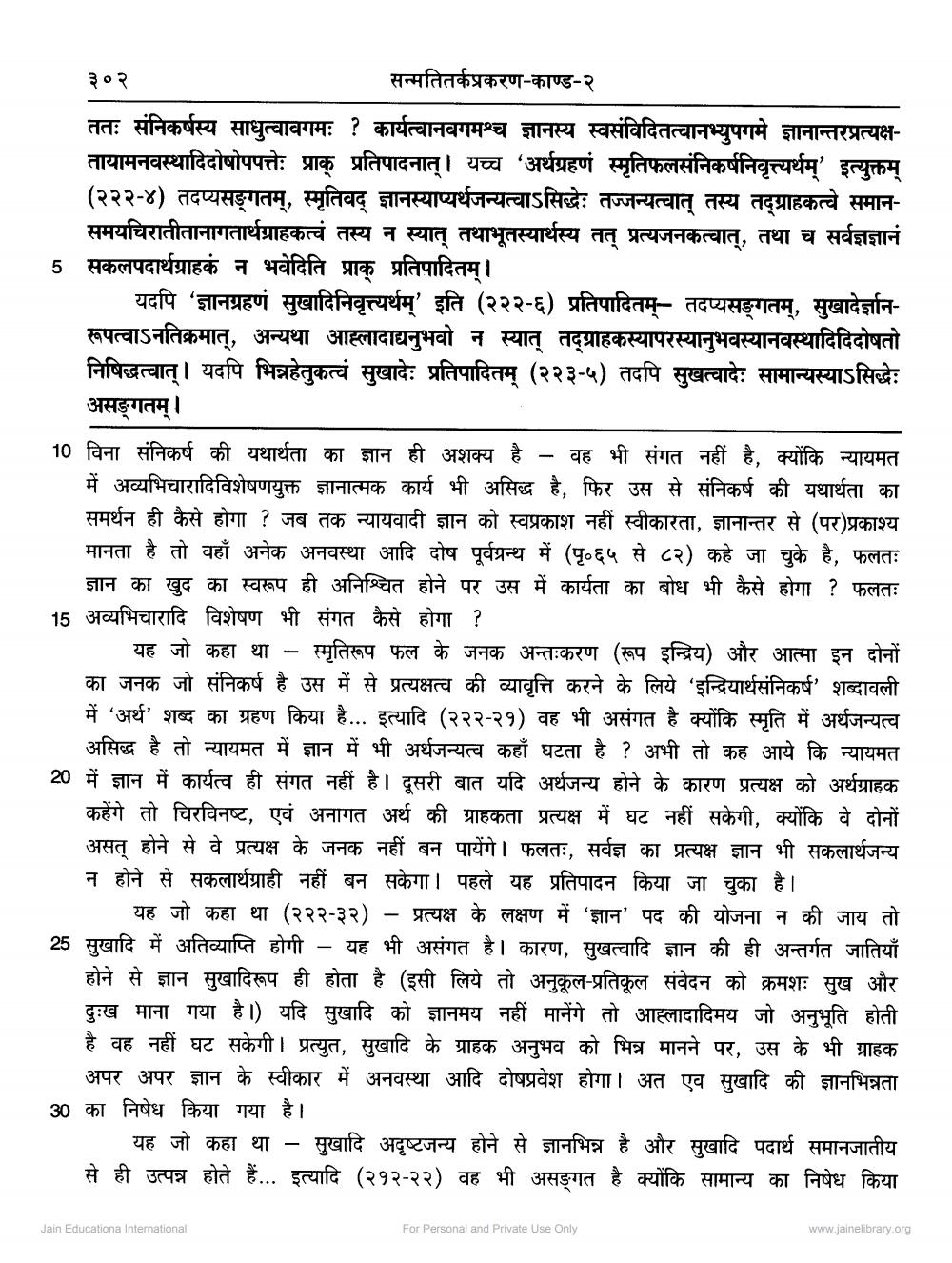________________
३०२
सन्मतितर्कप्रकरण-काण्ड-२
ततः संनिकर्षस्य साधुत्वावगम: ? कार्यत्वानवगमश्च ज्ञानस्य स्वसंविदितत्वानभ्युपगमे ज्ञानान्तरप्रत्यक्षतायामनवस्थादिदोषोपपत्तेः प्राक् प्रतिपादनात्। यच्च ‘अर्थग्रहणं स्मृतिफलसंनिकर्षनिवृत्त्यर्थम्' इत्युक्तम् (२२२-४) तदप्यसङ्गतम्, स्मृतिवद् ज्ञानस्याप्यर्थजन्यत्वाऽसिद्धेः तज्जन्यत्वात् तस्य तद्ग्राहकत्वे समान
समयचिरातीतानागतार्थग्राहकत्वं तस्य न स्यात् तथाभूतस्यार्थस्य तत् प्रत्यजनकत्वात्, तथा च सर्वज्ञज्ञानं 5 सकलपदार्थग्राहकं न भवेदिति प्राक् प्रतिपादितम् ।
यदपि 'ज्ञानग्रहणं सुखादिनिवृत्त्यर्थम्' इति (२२२-६) प्रतिपादितम्- तदप्यसङ्गतम्, सुखादेर्ज्ञानरूपत्वाऽनतिक्रमात्, अन्यथा आह्लादाद्यनुभवो न स्यात् तद्ग्राहकस्यापरस्यानुभवस्यानवस्थादिदिदोषतो निषिद्धत्वात्। यदपि भिन्नहेतुकत्वं सुखादेः प्रतिपादितम् (२२३-५) तदपि सुखत्वादेः सामान्यस्याऽसिद्धेः
असङ्गतम्। 10 विना संनिकर्ष की यथार्थता का ज्ञान ही अशक्य है - वह भी संगत नहीं है, क्योंकि न्यायमत
में अव्यभिचारादिविशेषणयुक्त ज्ञानात्मक कार्य भी असिद्ध है, फिर उस से संनिकर्ष की यथार्थता का समर्थन ही कैसे होगा ? जब तक न्यायवादी ज्ञान को स्वप्रकाश नहीं स्वीकारता, ज्ञानान्तर से (पर)प्रकाश्य मानता है तो वहाँ अनेक अनवस्था आदि दोष पूर्वग्रन्थ में (पृ०६५ से ८२) कहे जा चुके है, फलतः
ज्ञान का खुद का स्वरूप ही अनिश्चित होने पर उस में कार्यता का बोध भी कैसे होगा ? फलतः 15 अव्यभिचारादि विशेषण भी संगत कैसे होगा ?
यह जो कहा था - स्मृतिरूप फल के जनक अन्तःकरण (रूप इन्द्रिय) और आत्मा इन दोनों का जनक जो संनिकर्ष है उस में से प्रत्यक्षत्व की व्यावृत्ति करने के लिये 'इन्द्रियार्थसंनिकर्ष' शब्दावली में 'अर्थ' शब्द का ग्रहण किया है... इत्यादि (२२२-२१) वह भी असंगत है क्योंकि स्मृति में अर्थजन्यत्व
असिद्ध है तो न्यायमत में ज्ञान में भी अर्थजन्यत्व कहाँ घटता है ? अभी तो कह आये कि न्यायमत 20 में ज्ञान में कार्यत्व ही संगत नहीं है। दूसरी बात यदि अर्थजन्य होने के कारण प्रत्यक्ष को अर्थग्राहक
कहेंगे तो चिरविनष्ट. एवं अनागत अर्थ की ग्राहकता प्रत्यक्ष में घट नहीं सकेगी. क्योंकि वे असत् होने से वे प्रत्यक्ष के जनक नहीं बन पायेंगे। फलतः, सर्वज्ञ का प्रत्यक्ष ज्ञान भी सकलार्थजन्य न होने से सकलार्थग्राही नहीं बन सकेगा। पहले यह प्रतिपादन किया जा चुका है।
___ यह जो कहा था (२२२-३२) - प्रत्यक्ष के लक्षण में 'ज्ञान' पद की योजना न की जाय तो 25 सुखादि में अतिव्याप्ति होगी - यह भी असंगत है। कारण, सुखत्वादि ज्ञान की ही अन्तर्गत जातियाँ
होने से ज्ञान सुखादिरूप ही होता है (इसी लिये तो अनुकूल-प्रतिकूल संवेदन को क्रमशः सुख और दाख माना गया है। यदि सखादि को ज्ञानमय नहीं मानेंगे तो आलादादिमय जो अनभति होती है वह नहीं घट सकेगी। प्रत्युत, सुखादि के ग्राहक अनुभव को भिन्न मानने पर, उस के भी ग्राहक
अपर अपर ज्ञान के स्वीकार में अनवस्था आदि दोषप्रवेश होगा। अत एव सुखादि की ज्ञानभिन्नता 30 का निषेध किया गया है।
यह जो कहा था - सुखादि अदृष्टजन्य होने से ज्ञानभिन्न है और सुखादि पदार्थ समानजातीय से ही उत्पन्न होते हैं... इत्यादि (२१२-२२) वह भी असङ्गत है क्योंकि सामान्य का निषेध किया
Jain Educationa International
For Personal and Private Use Only
www.jainelibrary.org