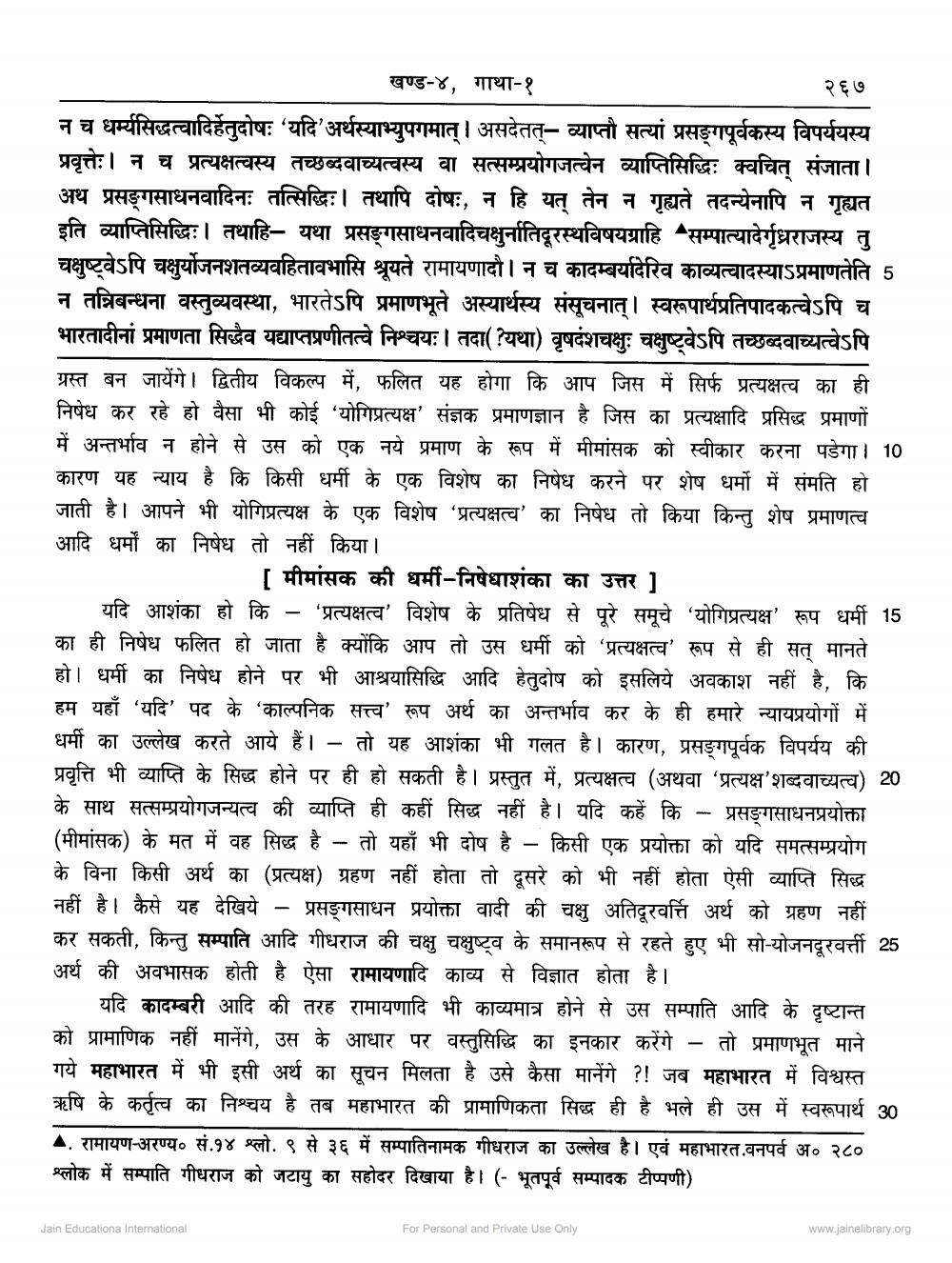________________
खण्ड-४, गाथा-१
२६७ न च धर्म्यसिद्धत्वादिहेतुदोष: 'यदि'अर्थस्याभ्युपगमात् । असदेतत्- व्याप्ती सत्यां प्रसङ्गपूर्वकस्य विपर्ययस्य प्रवृत्तेः। न च प्रत्यक्षत्वस्य तच्छब्दवाच्यत्वस्य वा सत्सम्प्रयोगजत्वेन व्याप्तिसिद्धिः क्वचित् संजाता। अथ प्रसङ्गसाधनवादिनः तत्सिद्धिः। तथापि दोषः, न हि यत् तेन न गृह्यते तदन्येनापि न गृह्यत इति व्याप्तिसिद्धिः । तथाहि- यथा प्रसङ्गसाधनवादिचक्षुर्नातिदूरस्थविषयग्राहि सम्पात्यादेर्गृध्रराजस्य तु चक्षुष्ट्वेऽपि चक्षुर्योजनशतव्यवहितावभासि श्रूयते रामायणादौ । न च कादम्बर्यादेरिव काव्यत्वादस्याऽप्रमाणतेति 5 न तन्निबन्धना वस्तुव्यवस्था, भारतेऽपि प्रमाणभूते अस्यार्थस्य संसूचनात्। स्वरूपार्थप्रतिपादकत्वेऽपि च भारतादीनां प्रमाणता सिद्धैव यद्याप्तप्रणीतत्वे निश्चयः । तदा(?यथा) वृषदंशचक्षुः चक्षुष्ट्वेऽपि तच्छब्दवाच्यत्वेऽपि ग्रस्त बन जायेंगे। द्वितीय विकल्प में, फलित यह होगा कि आप जिस में सिर्फ प्रत्यक्षत्व का ही निषेध कर रहे हो वैसा भी कोई ‘योगिप्रत्यक्ष' संज्ञक प्रमाणज्ञान है जिस का प्रत्यक्षादि प्रसिद्ध प्रमाणों में अन्तर्भाव न होने से उस को एक नये प्रमाण के रूप में मीमांसक को स्वीकार करना पडेगा। 10 कारण यह न्याय है कि किसी धर्मी के एक विशेष का निषेध करने पर शेष धर्मो में संमति हो जाती है। आपने भी योगिप्रत्यक्ष के एक विशेष 'प्रत्यक्षत्व' का निषेध तो किया किन्तु शेष प्रमाणत्व आदि धर्मों का निषेध तो नहीं किया।
[ मीमांसक की धर्मी-निषेधाशंका का उत्तर ] __यदि आशंका हो कि - 'प्रत्यक्षत्व' विशेष के प्रतिषेध से पूरे समूचे ‘योगिप्रत्यक्ष' रूप धर्मी 15 का ही निषेध फलित हो जाता है क्योंकि आप तो उस धर्मी को ‘प्रत्यक्षत्व' रूप से ही सत् मानते हो। धर्मी का निषेध होने पर भी आश्रयासिद्धि आदि हेतुदोष को इसलिये अवकाश नहीं है, कि हम यहाँ 'यदि' पद के 'काल्पनिक सत्त्व' रूप अर्थ का अन्तर्भाव कर के ही हमारे न्यायप्रयोगों में धर्मी का उल्लेख करते आये हैं। - तो यह आशंका भी गलत है। कारण, प्रसङ्गपूर्वक विपर्यय की प्रवृत्ति भी व्याप्ति के सिद्ध होने पर ही हो सकती है। प्रस्तुत में, प्रत्यक्षत्व (अथवा 'प्रत्यक्ष'शब्दवाच्यत्व) 20 के साथ सत्सम्प्रयोगजन्यत्व की व्याप्ति ही कहीं सिद्ध नहीं है। यदि कहें कि - प्रसङ्गसाधनप्रयोक्ता (मीमांसक) के मत में वह सिद्ध है - तो यहाँ भी दोष है – किसी एक प्रयोक्ता को यदि समत्सम्प्रयोग के विना किसी अर्थ का (प्रत्यक्ष) ग्रहण नहीं होता तो दूसरे को भी नहीं होता ऐसी व्याप्ति सिद्ध नहीं है। कैसे यह देखिये - प्रसङ्गसाधन प्रयोक्ता वादी की चक्षु अतिदूरवर्त्ति अर्थ को ग्रहण नहीं कर सकती, किन्तु सम्पाति आदि गीधराज की चक्षु चक्षुष्ट्व के समानरूप से रहते हुए भी सो-योजनदूरवर्ती 25 अर्थ की अवभासक होती है ऐसा रामायणादि काव्य से विज्ञात होता है।
यदि कादम्बरी आदि की तरह रामायणादि भी काव्यमात्र होने से उस सम्पाति आदि के दृष्टान्त को प्रामाणिक नहीं मानेंगे, उस के आधार पर वस्तुसिद्धि का इनकार करेंगे - तो प्रमाणभूत माने गये महाभारत में भी इसी अर्थ का सूचन मिलता है उसे कैसा मानेंगे ?! जब महाभारत में विश्वस्त ऋषि के कर्तृत्व का निश्चय है तब महाभारत की प्रामाणिकता सिद्ध ही है भले ही उस में स्वरूपार्थ 30 ..रामायण-अरण्य. सं.१४ श्लो. ९ से ३६ में सम्पातिनामक गीधराज का उल्लेख है। एवं महाभारत.वनपर्व अ० २८० श्लोक में सम्पाति गीधराज को जटायु का सहोदर दिखाया है। (- भूतपूर्व सम्पादक टीप्पणी)
Jain Educationa International
For Personal and Private Use Only
www.jainelibrary.org