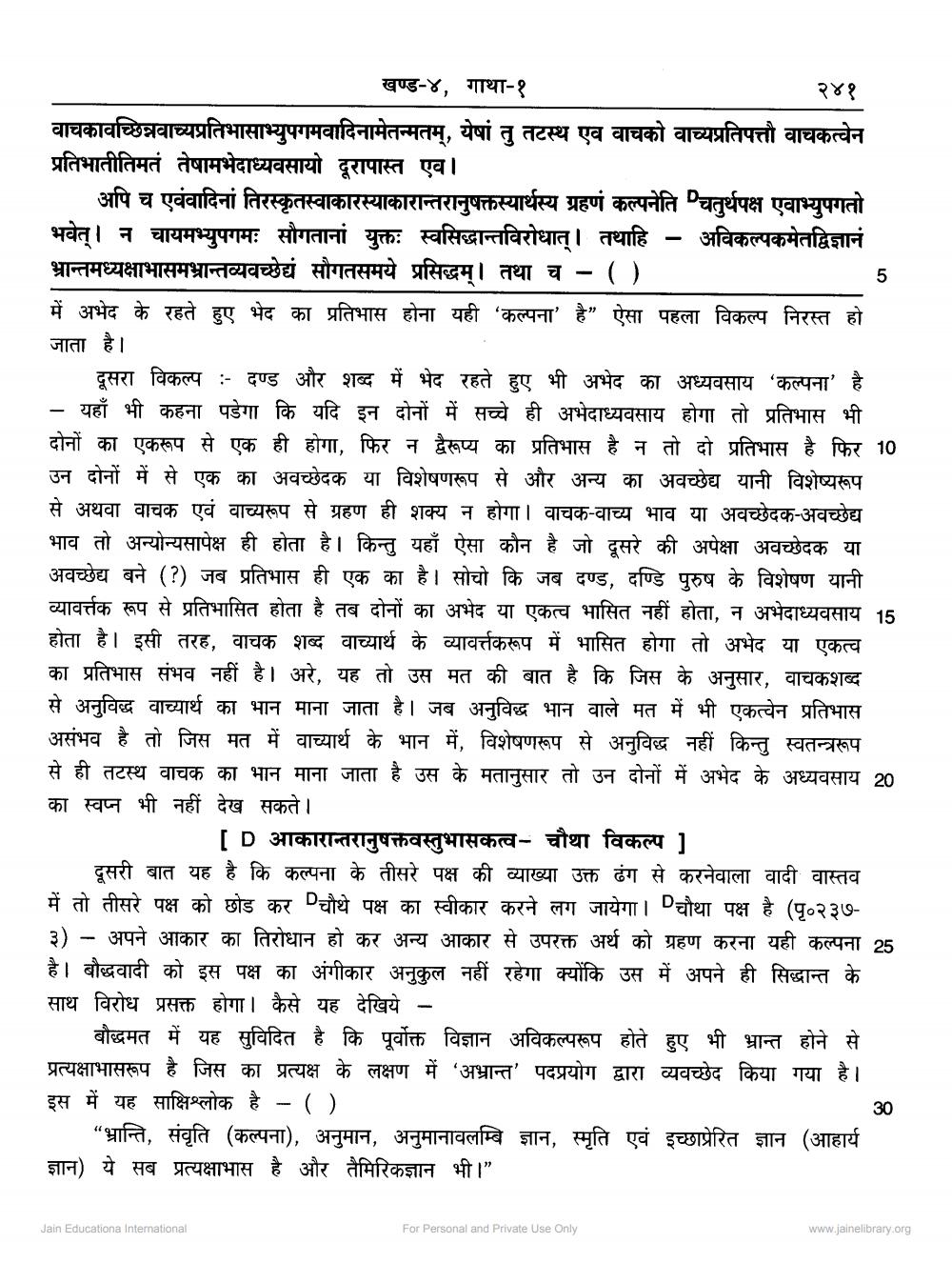________________
5
खण्ड-४, गाथा-१
२४१ वाचकावच्छिन्नवाच्यप्रतिभासाभ्युपगमवादिनामेतन्मतम्, येषां तु तटस्थ एव वाचको वाच्यप्रतिपत्तौ वाचकत्वेन प्रतिभातीतिमतं तेषामभेदाध्यवसायो दुरापास्त एव ।
अपि च एवंवादिनां तिरस्कृतस्वाकारस्याकारान्तरानुषक्तस्यार्थस्य ग्रहणं कल्पनेति चतुर्थपक्ष एवाभ्युपगतो भवेत्। न चायमभ्युपगमः सौगतानां युक्तः स्वसिद्धान्तविरोधात्। तथाहि - अविकल्पकमेतद्विज्ञानं भ्रान्तमध्यक्षाभासमभ्रान्तव्यवच्छेद्यं सौगतसमये प्रसिद्धम्। तथा च - ( ) में अभेद के रहते हुए भेद का प्रतिभास होना यही 'कल्पना' है" ऐसा पहला विकल्प निरस्त हो जाता है।
दूसरा विकल्प :- दण्ड और शब्द में भेद रहते हुए भी अभेद का अध्यवसाय 'कल्पना' है - यहाँ भी कहना पडेगा कि यदि इन दोनों में सच्चे ही अभेदाध्यवसाय होगा तो प्रतिभास भी
एक ही होगा. फिर न द्वैरूप्य का प्रतिभास है न तो दो प्रतिभास है फिर 10 उन दोनों में से एक का अवच्छेदक या विशेषणरूप से और अन्य का अवच्छेद्य यानी विशेष्यरूप से अथवा वाचक एवं वाच्यरूप से ग्रहण ही शक्य न होगा। वाचक-वाच्य भाव या अवच्छेदक-अवच्छेद्य भाव तो अन्योन्यसापेक्ष ही होता है। किन्तु यहाँ ऐसा कौन है जो दूसरे की अपेक्षा अवच्छेदक या अवच्छेद्य बने (?) जब प्रतिभास ही एक का है। सोचो कि जब दण्ड, दण्डि पुरुष के विशेषण यानी
वर्त्तक रूप से प्रतिभासित होता है तब दोनों का अभेद या एकत्व भासित नहीं होता, न अभेदाध्यवसाय 15 होता है। इसी तरह, वाचक शब्द वाच्यार्थ के व्यावर्त्तकरूप में भासित होगा तो अभेद या एकत्व का प्रतिभास संभव नहीं है। अरे, यह तो उस मत की बात है कि जिस के अनुसार, वाचकशब्द से अनविद्ध वाच्यार्थ का भान माना जाता है। जब अनविद्ध भान वाले मत में भी एकत्वेन प्रतिभास असंभव है तो जिस मत में वाच्यार्थ के भान में, विशेषणरूप से अनुविद्ध नहीं किन्तु स्वतन्त्ररूप से ही तटस्थ वाचक का भान माना जाता है उस के मतानुसार तो उन दोनों में अभेद के अध्यवसाय 20 का स्वप्न भी नहीं देख सकते।
[D आकारान्तरानुषक्तवस्तुभासकत्व- चौथा विकल्प ] __ दूसरी बात यह है कि कल्पना के तीसरे पक्ष की व्याख्या उक्त ढंग से करनेवाला वादी वास्तव में तो तीसरे पक्ष को छोड कर चौथे पक्ष का स्वीकार करने लग जायेगा। Dचौथा पक्ष है (पृ०२३७३) - अपने आकार का तिरोधान हो कर अन्य आकार से उपरक्त अर्थ को ग्रहण करना यही कल्पना 25 है। बौद्धवादी को इस पक्ष का अंगीकार अनुकुल नहीं रहेगा क्योंकि उस में अपने ही सिद्धान्त के साथ विरोध प्रसक्त होगा। कैसे यह देखिये -
बौद्धमत में यह सुविदित है कि पूर्वोक्त विज्ञान अविकल्परूप होते हुए भी भ्रान्त होने से प्रत्यक्षाभासरूप है जिस का प्रत्यक्ष के लक्षण में ‘अभ्रान्त' पदप्रयोग द्वारा व्यवच्छेद किया गया है। इस में यह साक्षिश्लोक है - ( )
30 ___भ्रान्ति, संवृति (कल्पना), अनुमान, अनुमानावलम्बि ज्ञान, स्मृति एवं इच्छाप्रेरित ज्ञान (आहार्य ज्ञान) ये सब प्रत्यक्षाभास है और तैमिरिकज्ञान भी।"
Jain Educationa International
For Personal and Private Use Only
www.jainelibrary.org