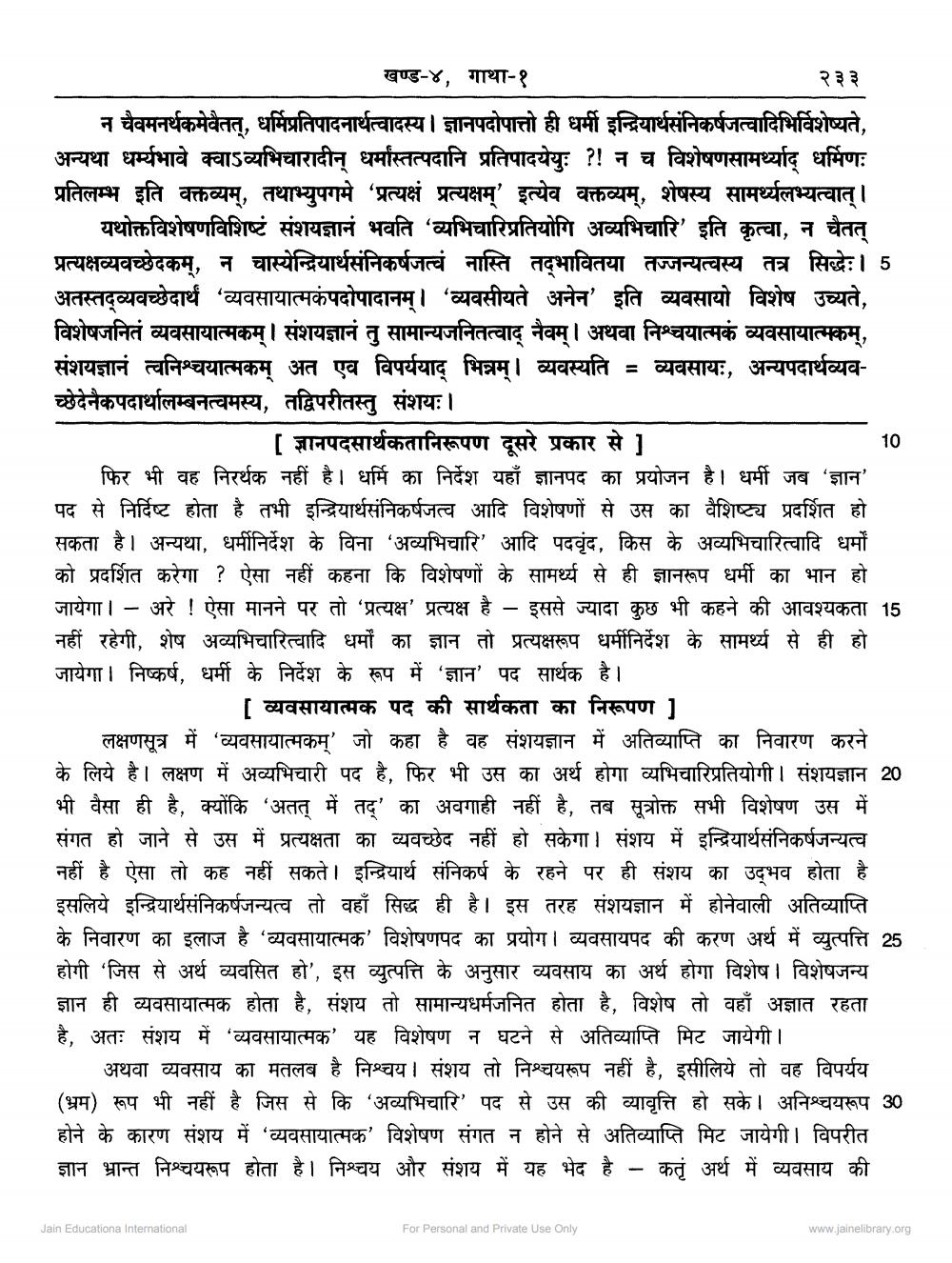________________
खण्ड-४, गाथा-१
२३३ न चैवमनर्थकमेवैतत्, धर्मिप्रतिपादनार्थत्वादस्य । ज्ञानपदोपात्तो ही धर्मी इन्द्रियार्थसंनिकर्षजत्वादिभिर्विशेष्यते, अन्यथा धर्म्यभावे क्वाऽव्यभिचारादीन् धर्मास्तत्पदानि प्रतिपादयेयुः ?! न च विशेषणसामर्थ्याद् धर्मिणः प्रतिलम्भ इति वक्तव्यम्, तथाभ्युपगमे 'प्रत्यक्षं प्रत्यक्षम्' इत्येव वक्तव्यम्, शेषस्य सामर्थ्यलभ्यत्वात् ।
यथोक्तविशेषणविशिष्टं संशयज्ञानं भवति 'व्यभिचारिप्रतियोगि अव्यभिचारि' इति कृत्वा, न चैतत् प्रत्यक्षव्यवच्छेदकम्, न चास्येन्द्रियार्थसंनिकर्षजत्वं नास्ति तद्भावितया तज्जन्यत्वस्य तत्र सिद्धेः। 5 अतस्तद्व्यवच्छेदार्थं 'व्यवसायात्मकंपदोपादानम्। 'व्यवसीयते अनेन' इति व्यवसायो विशेष उच्यते, विशेषजनितं व्यवसायात्मकम् । संशयज्ञानं तु सामान्यजनितत्वाद् नैवम् । अथवा निश्चयात्मकं व्यवसायात्मकम्, संशयज्ञानं त्वनिश्चयात्मकम् अत एव विपर्ययाद् भिन्नम् । व्यवस्यति = व्यवसाय:, अन्यपदार्थव्यवच्छेदेनैकपदार्थालम्बनत्वमस्य, तद्विपरीतस्तु संशयः।
[ ज्ञानपदसार्थकतानिरूपण दूसरे प्रकार से ] फिर भी वह निरर्थक नहीं है। धर्मि का निर्देश यहाँ ज्ञानपद का प्रयोजन है। धर्मी जब 'ज्ञान' पद से निर्दिष्ट होता है तभी इन्द्रियार्थसंनिकर्षजत्व आदि विशेषणों से उस का वैशिष्ट्य प्रदर्शित हो सकता है। अन्यथा, धर्मीनिर्देश के विना 'अव्यभिचारि' आदि पदवृंद, किस के अव्यभिचारित्वादि धर्मों को प्रदर्शित करेगा ? ऐसा नहीं कहना कि विशेषणों के सामर्थ्य से ही ज्ञानरूप धर्मी का भान हो जायेगा। - अरे ! ऐसा मानने पर तो 'प्रत्यक्ष' प्रत्यक्ष है – इससे ज्यादा कुछ भी कहने की आवश्यकता 15 नहीं रहेगी, शेष अव्यभिचारित्वादि धर्मों का ज्ञान तो प्रत्यक्षरूप धर्मीनिर्देश के सामर्थ्य से ही हो जायेगा। निष्कर्ष, धर्मी के निर्देश के रूप में 'ज्ञान' पद सार्थक है।
1 [व्यवसायात्मक पद की सार्थकता का निरूपण ] लक्षणसूत्र में 'व्यवसायात्मकम्' जो कहा है वह संशयज्ञान में अतिव्याप्ति का निवारण करने के लिये है। लक्षण में अव्यभिचारी पद है, फिर भी उस का अर्थ होगा व्यभिचारिप्रतियोगी। संशयज्ञान 20 भी वैसा ही है, क्योंकि 'अतत् में तद्' का अवगाही नहीं है, तब सूत्रोक्त सभी विशेषण उस में संगत हो जाने से उस में प्रत्यक्षता का व्यवच्छेद नहीं हो सकेगा। संशय में इन्द्रियार्थसंनिकर्षजन्यत्व नहीं है ऐसा तो कह नहीं सकते। इन्द्रियार्थ संनिकर्ष के रहने पर ही संशय का उद्भव होता है इसलिये इन्द्रियार्थसंनिकर्षजन्यत्व तो वहाँ सिद्ध ही है। इस तरह संशयज्ञान में होनेवाली अतिव्याप्ति के निवारण का इलाज है 'व्यवसायात्मक' विशेषणपद का प्रयोग। व्यवसायपद की करण अर्थ में व्युत्पत्ति 25 होगी 'जिस से अर्थ व्यवसित हो', इस व्युत्पत्ति के अनुसार व्यवसाय का अर्थ होगा विशेष । विशेषजन्य ज्ञान ही व्यवसायात्मक होता है, संशय तो सामान्यधर्मजनित होता है, विशेष तो वहाँ अज्ञात रहता है, अतः संशय में 'व्यवसायात्मक' यह विशेषण न घटने से अतिव्याप्ति मिट जायेगी।
अथवा व्यवसाय का मतलब है निश्चय । संशय तो निश्चयरूप नहीं है, इसीलिये तो वह विपर्यय (भ्रम) रूप भी नहीं है जिस से कि 'अव्यभिचारि' पद से उस की व्यावृत्ति हो सके। अनिश्चयरूप 30 होने के कारण संशय में 'व्यवसायात्मक' विशेषण संगत न होने से अतिव्याप्ति मिट जायेगी। विपरीत ज्ञान भ्रान्त निश्चयरूप होता है। निश्चय और संशय में यह भेद है - कतुं अर्थ में व्यवसाय की
Jain Educationa International
For Personal and Private Use Only
www.jainelibrary.org