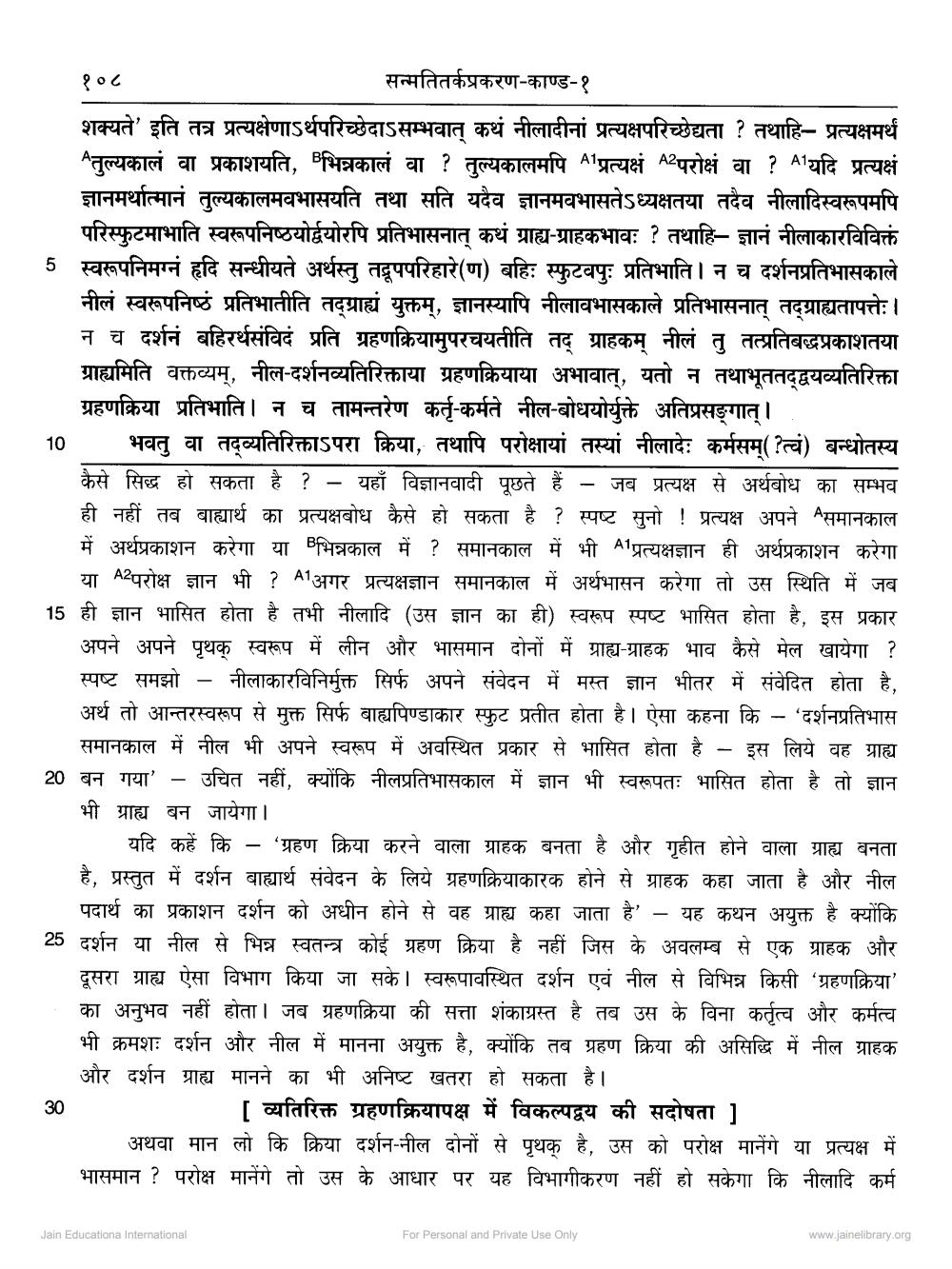________________
१०८
सन्मतितर्कप्रकरण-काण्ड-१
शक्यते' इति तत्र प्रत्यक्षेणाऽर्थपरिच्छेदाऽसम्भवात् कथं नीलादीनां प्रत्यक्षपरिच्छेद्यता ? तथाहि- प्रत्यक्षमर्थ Aतुल्यकालं वा प्रकाशयति, Bभिन्नकालं वा ? तुल्यकालमपि प्रत्यक्षं A2परोक्षं वा ? यदि प्रत्यक्ष ज्ञानमर्थात्मानं तुल्यकालमवभासयति तथा सति यदैव ज्ञानमवभासतेऽध्यक्षतया तदैव नीलादिस्वरूपमपि
परिस्फुटमाभाति स्वरूपनिष्ठयोर्द्वयोरपि प्रतिभासनात् कथं ग्राह्य-ग्राहकभावः ? तथाहि- ज्ञानं नीलाकारविविक्तं 5 स्वरूपनिमग्नं हृदि सन्धीयते अर्थस्तु तद्रूपपरिहारे(ण) बहिः स्फुटवपुः प्रतिभाति। न च दर्शनप्रतिभासकाले
नीलं स्वरूपनिष्ठं प्रतिभातीति तद्ग्राह्यं युक्तम्, ज्ञानस्यापि नीलावभासकाले प्रतिभासनात् तद्ग्राह्यतापत्तेः । न च दर्शनं बहिरर्थसंविदं प्रति ग्रहणक्रियामुपरचयतीति तद् ग्राहकम् नीलं तु तत्प्रतिबद्धप्रकाशतया ग्राह्यमिति वक्तव्यम. नील-दर्शनव्यतिरिक्ताया ग्रहणक्रियाया अभावात, यतो न तथाभततदद्वयव्यतिरिक्ता
ग्रहणक्रिया प्रतिभाति। न च तामन्तरेण कर्तृ-कर्मते नील-बोधयोर्युक्ते अतिप्रसङ्गात् । 10 भवतु वा तद्व्यतिरिक्ताऽपरा क्रिया, तथापि परोक्षायां तस्यां नीलादेः कर्मसम्(?त्वं) बन्धोतस्य
कैसे सिद्ध हो सकता है ? - यहाँ विज्ञानवादी पूछते हैं – जब प्रत्यक्ष से अर्थबोध का सम्भव ही नहीं तब बाह्यार्थ का प्रत्यक्षबोध कैसे हो सकता है ? स्पष्ट सुनो ! प्रत्यक्ष अपने समानकाल में अर्थप्रकाशन करेगा या Bभिन्नकाल में ? समानकाल में भी A1प्रत्यक्षज्ञान ही अर्थप्रकाशन करेगा
या A2परोक्ष ज्ञान भी ? A1अगर प्रत्यक्षज्ञान समानकाल में अर्थभासन करेगा तो उस स्थिति में जब 15 ही ज्ञान भासित होता है तभी नीलादि (उस ज्ञान का ही) स्वरूप स्पष्ट भासित होता है, इस प्रकार
अपने अपने पृथक् स्वरूप में लीन और भासमान दोनों में ग्राह्य-ग्राहक भाव कैसे मेल खायेगा ? स्पष्ट समझो - नीलाकारविनिर्मुक्त सिर्फ अपने संवेदन में मस्त ज्ञान भीतर में संवेदित होता है, अर्थ तो आन्तरस्वरूप से मुक्त सिर्फ बाह्यपिण्डाकार स्फुट प्रतीत होता है। ऐसा कहना कि – ‘दर्शनप्रतिभास
समानकाल में नील भी अपने स्वरूप में अवस्थित प्रकार से भासित होता है - इस लिये वह ग्राह्य 20 बन गया' – उचित नहीं, क्योंकि नीलप्रतिभासकाल में ज्ञान भी स्वरूपतः भासित होता है तो ज्ञान भी ग्राह्य बन जायेगा।
यदि कहें कि – ‘ग्रहण क्रिया करने वाला ग्राहक बनता है और गृहीत होने वाला ग्राह्य बनता है, प्रस्तुत में दर्शन बाह्यार्थ संवेदन के लिये ग्रहणक्रियाकारक होने से ग्राहक कहा जाता है और नील पदार्थ का प्रकाशन दर्शन को अधीन होने से वह ग्राह्य कहा जाता है' – यह कथन अयुक्त है क्योंकि
नील से भिन्न स्वतन्त्र कोई ग्रहण क्रिया है नहीं जिस के अवलम्ब से एक ग्राहक और दूसरा ग्राह्य ऐसा विभाग किया जा सके। स्वरूपावस्थित दर्शन एवं नील से विभिन्न किसी ‘ग्रहणक्रिया' का अनुभव नहीं होता। जब ग्रहणक्रिया की सत्ता शंकाग्रस्त है तब उस के विना कर्तृत्व और कर्मत्व भी क्रमशः दर्शन और नील में मानना अयुक्त है, क्योंकि तब ग्रहण क्रिया की असिद्धि में नील ग्राहक और दर्शन ग्राह्य मानने का भी अनिष्ट खतरा हो सकता है।
[ व्यतिरिक्त ग्रहणक्रियापक्ष में विकल्पद्वय की सदोषता ] अथवा मान लो कि क्रिया दर्शन-नील दोनों से पृथक् है, उस को परोक्ष मानेंगे या प्रत्यक्ष में भासमान ? परोक्ष मानेंगे तो उस के आधार पर यह विभागीकरण नहीं हो सकेगा कि नीलादि कर्म
Jain Educationa International
For Personal and Private Use Only
www.jainelibrary.org