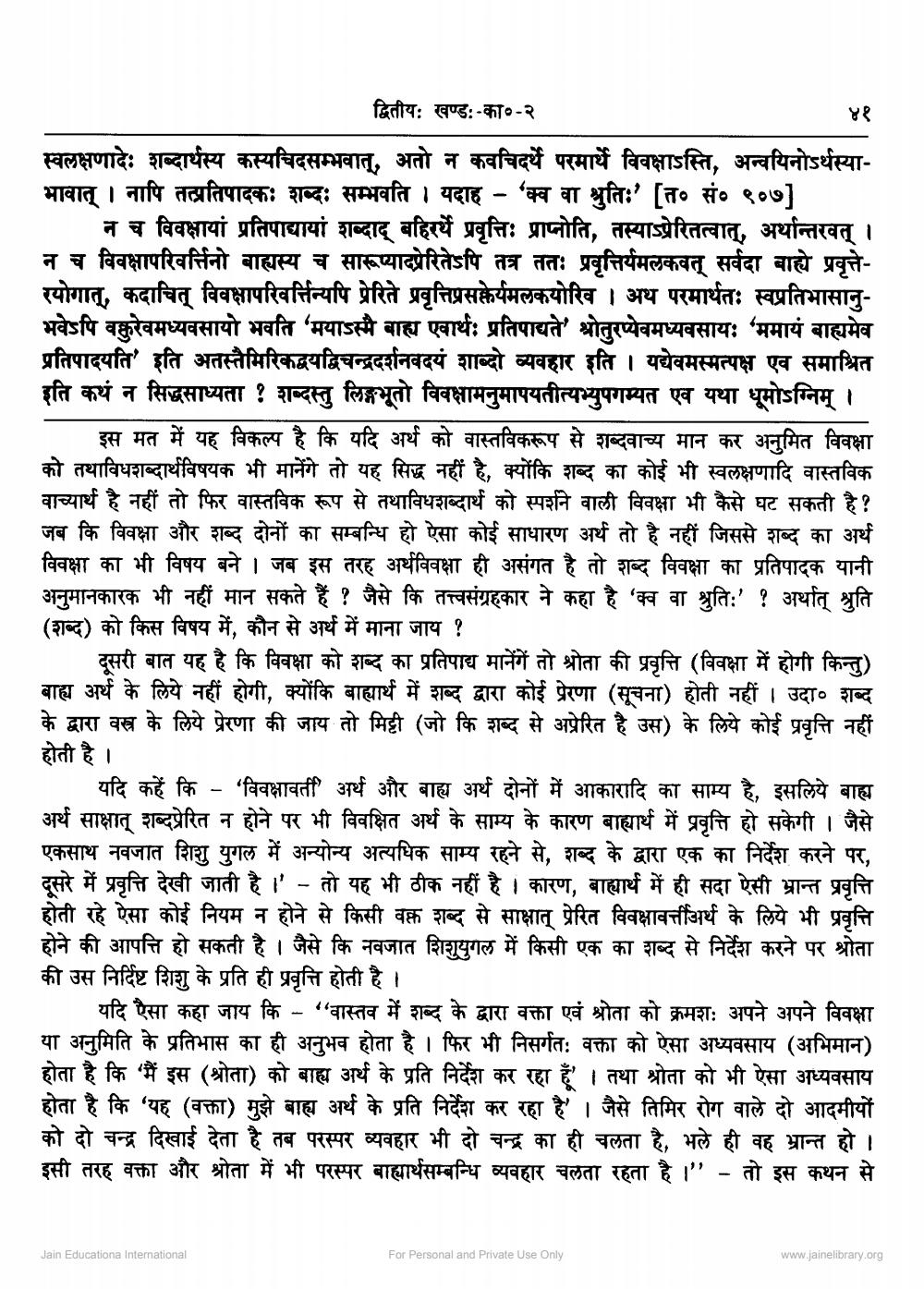________________
द्वितीयः खण्डः का० - २
स्वलक्षणादेः शब्दार्थस्य कस्यचिदसम्भवात्, अतो न कवचिदर्थे परमार्थे विवक्षाऽस्ति, अन्वयिनोऽर्थस्याभावात् । नापि तत्प्रतिपादकः शब्दः सम्भवति । यदाह - 'क्व वा श्रुति:' [त० सं० ९०७ ]
न च विवक्षायां प्रतिपाद्यायां शब्दाद् बहिरर्थे प्रवृत्तिः प्राप्नोति, तस्याऽप्रेरितत्वात् अर्थान्तरवत् । न च विवक्षापरिवर्त्तिनो बाह्यस्य च सारूप्यादप्रेरितेऽपि तत्र ततः प्रवृत्तिर्यमलकवत् सर्वदा बाह्ये प्रवृत्तेरयोगात्, कदाचित् विवक्षापरिवर्त्तिन्यपि प्रेरिते प्रवृत्तिप्रसक्तेर्यमलकयोरिव । अथ परमार्थतः स्वप्रतिभासानुभवेऽपि वक्तुरेवमध्यवसायो भवति 'मयाऽस्मै बाह्य एवार्थः प्रतिपाद्यते' श्रोतुरप्येवमध्यवसायः ‘ममायं बाह्यमेव प्रतिपादयति' इति अतस्तैमिरिकद्वयद्विचन्द्रदर्शनवदयं शाब्दो व्यवहार इति । यद्येवमस्मत्पक्ष एव समाश्रित इति कथं न सिद्धसाध्यता ? शब्दस्तु लिङ्गभूतो विवक्षामनुमापयतीत्यभ्युपगम्यत एव यथा धूमोऽग्निम् ।
इस मत में यह विकल्प है कि यदि अर्थ को वास्तविकरूप से शब्दवाच्य मान कर अनुमित विवक्षा को तथाविधशब्दार्थविषयक भी मानेंगे तो यह सिद्ध नहीं है, क्योंकि शब्द का कोई भी स्वलक्षणादि वास्तविक वाच्यार्थ है नहीं तो फिर वास्तविक रूप से तथाविधशब्दार्थ को स्पर्शने वाली विवक्षा भी कैसे घट सकती है ? जब कि विवक्षा और शब्द दोनों का सम्बन्धि हो ऐसा कोई साधारण अर्थ तो है नहीं जिससे शब्द का अर्थ विवक्षा का भी विषय बने । जब इस तरह अर्थविवक्षा ही असंगत है तो शब्द विवक्षा का प्रतिपादक यानी अनुमानकारक भी नहीं मान सकते हैं ? जैसे कि तत्त्वसंग्रहकार ने कहा है 'क्व वा श्रुतिः' ? अर्थात् श्रुति ( शब्द) को किस विषय में, कौन से अर्थ में माना जाय ?
४१
दूसरी बात यह है कि विवक्षा को शब्द का प्रतिपाद्य मानेंगें तो श्रोता की प्रवृत्ति ( विवक्षा में होगी किन्तु ) बाह्य अर्थ के लिये नहीं होगी, क्योंकि बाह्यार्थ में शब्द द्वारा कोई प्रेरणा (सूचना ) होती नहीं । उदा० शब्द के द्वारा वस्त्र के लिये प्रेरणा की जाय तो मिट्टी (जो कि शब्द से अप्रेरित है उस ) के लिये कोई प्रवृत्ति नहीं होती है ।
यदि कहें कि 'विवक्षावर्ती अर्थ और बाह्य अर्थ दोनों में आकारादि का साम्य है, इसलिये बाह्य अर्थ साक्षात् शब्दप्रेरित न होने पर भी विवक्षित अर्थ के साम्य के कारण बाह्यार्थ में प्रवृत्ति हो सकेगी । जैसे एकसाथ नवजात शिशु युगल में अन्योन्य अत्यधिक साम्य रहने से, शब्द के द्वारा एक का निर्देश करने पर, दूसरे में प्रवृत्ति देखी जाती है तो यह भी ठीक नहीं है। कारण, बाह्यार्थ में ही सदा ऐसी भ्रान्त प्रवृत्ति होती रहे ऐसा कोई नियम न होने से किसी वक्त शब्द से साक्षात् प्रेरित विवक्षावर्त्तीअर्थ के लिये भी प्रवृत्ति होने की आपत्ति हो सकती है। जैसे कि नवजात शिशुयुगल में किसी एक का शब्द से निर्देश करने पर श्रोता की उस निर्दिष्ट शिशु के प्रति ही प्रवृत्ति होती है ।
।'
-
यदि ऐसा कहा जाय कि " वास्तव में शब्द के द्वारा वक्ता एवं श्रोता को क्रमशः अपने अपने विवक्षा या अनुमिति के प्रतिभास का ही अनुभव होता है । फिर भी निसर्गतः वक्ता को ऐसा अध्यवसाय (अभिमान) होता है कि 'मैं इस (श्रोता) को बाह्य अर्थ के प्रति निर्देश कर रहा हूँ' । तथा श्रोता को भी ऐसा अध्यवसाय होता है कि 'यह (वक्ता) मुझे बाह्य अर्थ के प्रति निर्देश कर रहा है' । जैसे तिमिर रोग वाले दो आदमीयों को दो चन्द्र दिखाई देता है तब परस्पर व्यवहार भी दो चन्द्र का ही चलता है, भले ही वह भ्रान्त हो । इसी तरह वक्ता और श्रोता में भी परस्पर बाह्यार्थसम्बन्धि व्यवहार चलता रहता है ।"
तो इस कथन से
Jain Educationa International
For Personal and Private Use Only
www.jainelibrary.org