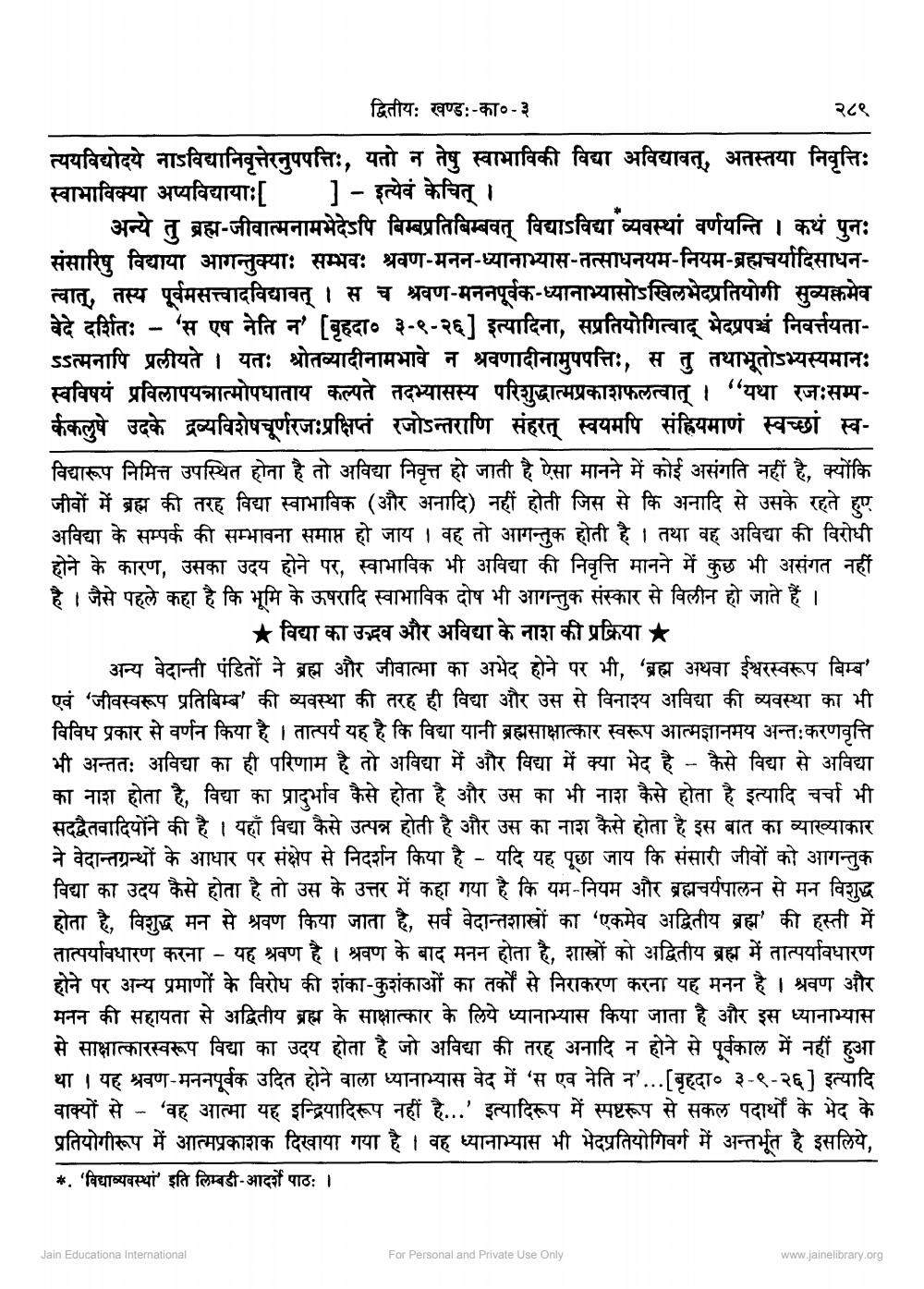________________
द्वितीयः खण्ड:-का०-३
२८९ त्ययविद्योदये नाऽविद्यानिवृत्तेरनुपपत्तिः, यतो न तेषु स्वाभाविकी विद्या अविद्यावत्, अतस्तया निवृत्तिः स्वाभाविक्या अप्यविद्यायाः[ ] - इत्येवं केचित् ।।
अन्ये तु ब्रह्म-जीवात्मनामभेदेऽपि बिम्बप्रतिबिम्बवत् विद्याऽविद्या व्यवस्थां वर्णयन्ति । कथं पुनः संसारिषु विद्याया आगन्तुक्याः सम्भवः श्रवण-मनन-ध्यानाभ्यास-तत्साधनयम-नियम-ब्रह्मचर्यादिसाधनत्वात्, तस्य पूर्वमसत्त्वादविद्यावत् । स च श्रवण-मननपूर्वक-ध्यानाभ्यासोऽखिलभेदप्रतियोगी सुव्यक्तमेव वेदे दर्शितः - ‘स एष नेति न' [बृहदा० ३.९-२६] इत्यादिना, सप्रतियोगित्वाद् भेदप्रपञ्चं निवर्त्तयताऽऽत्मनापि प्रलीयते । यतः श्रोतव्यादीनामभावे न श्रवणादीनामुपपत्तिः, स तु तथाभूतोऽभ्यस्यमानः स्वविषयं प्रविलापयन्नात्मोपघाताय कल्पते तदभ्यासस्य परिशुद्धात्मप्रकाशफलत्वात् । “यथा रजःसम्प
कलुषे उदके द्रव्यविशेषचूर्णरजःप्रक्षिप्तं रजोऽन्तराणि संहरत् स्वयमपि संह्रियमाणं स्वच्छां स्वविद्यारूप निमित्त उपस्थित होना है तो अविद्या निवृत्त हो जाती है ऐसा मानने में कोई असंगति नहीं है, क्योंकि जीवों में ब्रह्म की तरह विद्या स्वाभाविक (और अनादि) नहीं होती जिस से कि अनादि से उसके रहते हए अविद्या के सम्पर्क की सम्भावना समाप्त हो जाय । वह तो आगन्तुक होती है । तथा वह अविद्या की विरोधी होने के कारण, उसका उदय होने पर, स्वाभाविक भी अविद्या की निवृत्ति मानने में कुछ भी असंगत नहीं है । जैसे पहले कहा है कि भूमि के ऊषरादि स्वाभाविक दोष भी आगन्तुक संस्कार से विलीन हो जाते हैं ।
★ विद्या का उद्भव और अविद्या के नाश की प्रक्रिया* अन्य वेदान्ती पंडितों ने ब्रह्म और जीवात्मा का अभेद होने पर भी, 'ब्रह्म अथवा ईश्वरस्वरूप बिम्ब' एवं 'जीवस्वरूप प्रतिबिम्ब' की व्यवस्था की तरह ही विद्या और उस से विनाश्य अविद्या की व्यवस्था का भी विविध प्रकार से वर्णन किया है । तात्पर्य यह है कि विद्या यानी ब्रह्मसाक्षात्कार स्वरूप आत्मज्ञानमय अन्त:करणवृत्ति भी अन्तत: अविद्या का ही परिणाम है तो अविद्या में और विद्या में क्या भेद है - कैसे विद्या से अविद्या का नाश होता है, विद्या का प्रादुर्भाव कैसे होता है और उस का भी नाश कैसे होता है इत्यादि चर्चा भी सदद्वैतवादियोंने की है । यहाँ विद्या कैसे उत्पन्न होती है और उस का नाश कैसे होता है इस बात का व्याख्याकार ने वेदान्तग्रन्थों के आधार पर संक्षेप से निदर्शन किया है - यदि यह पूछा जाय कि संसारी जीवों को आगन्तुक विद्या का उदय कैसे होता है तो उस के उत्तर में कहा गया है कि यम-नियम और ब्रह्मचर्यपालन से मन विशुद्ध होता है, विशुद्ध मन से श्रवण किया जाता है, सर्व वेदान्तशास्त्रों का 'एकमेव अद्वितीय ब्रह्म' की हस्ती में तात्पर्यावधारण करना - यह श्रवण है । श्रवण के बाद मनन होता है, शास्त्रों को अद्वितीय ब्रह्म में तात्पर्यावधारण होने पर अन्य प्रमाणों के विरोध की शंका-कुशंकाओं का तर्कों से निराकरण करना यह मनन है । श्रवण और मनन की सहायता से अद्वितीय ब्रह्म के साक्षात्कार के लिये ध्यानाभ्यास किया जाता है और इस ध्यानाभ्यास से साक्षात्कारस्वरूप विद्या का उदय होता है जो अविद्या की तरह अनादि न होने से पूर्वकाल में नहीं हुआ था । यह श्रवण-मननपूर्वक उदित होने वाला ध्यानाभ्यास वेद में ‘स एव नेति न'...[बृहदा० ३-९-२६] इत्यादि वाक्यों से - 'वह आत्मा यह इन्द्रियादिरूप नहीं है...' इत्यादिरूप में स्पष्टरूप से सकल पदार्थों के भेद के प्रतियोगीरूप में आत्मप्रकाशक दिखाया गया है । वह ध्यानाभ्यास भी भेदप्रतियोगिवर्ग में अन्तर्भूत है इसलिये, *. 'विद्याव्यवस्था' इति लिम्बडी-आदर्श पाठः ।
Jain Educationa International
For Personal and Private Use Only
www.jainelibrary.org