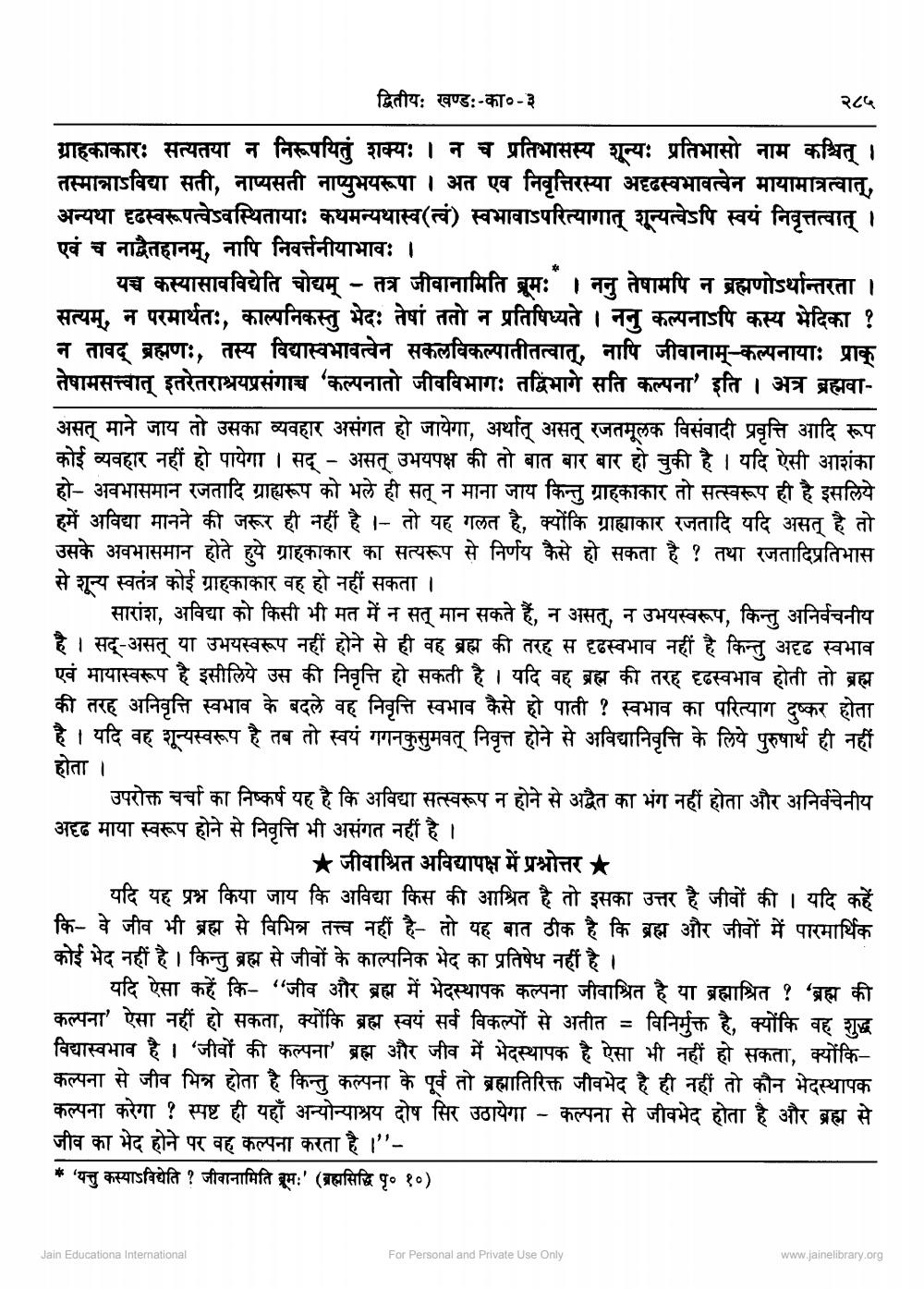________________
द्वितीयः खण्ड:-का०-३
२८५ ग्राहकाकारः सत्यतया न निरूपयितुं शक्यः । न च प्रतिभासस्य शून्यः प्रतिभासो नाम कश्चित् । तस्मानाऽविद्या सती, नाप्यसती नाप्युभयरूपा । अत एव निवृत्तिरस्या अदृढस्वभावत्वेन मायामात्रत्वात्, अन्यथा दृढस्वरूपत्वेऽवस्थितायाः कथमन्यथास्व(त्वं) स्वभावाऽपरित्यागात् शून्यत्वेऽपि स्वयं निवृत्तत्वात् । एवं च नाद्वैतहानम्, नापि निवर्त्तनीयाभावः ।
___यच्च कस्यासावविद्येति चोद्यम् - तत्र जीवानामिति ब्रूमः । ननु तेषामपि न ब्रह्मणोऽर्थान्तरता । सत्यम्, न परमार्थतः, काल्पनिकस्तु भेदः तेषां ततो न प्रतिषिध्यते । ननु कल्पनाऽपि कस्य भेदिका ? न तावद् ब्रह्मणः, तस्य विद्यास्वभावत्वेन सकलविकल्पातीतत्वात्, नापि जीवानाम्-कल्पनायाः प्राक् तेषामसत्त्वात् इतरेतराश्रयप्रसंगाच्च 'कल्पनातो जीवविभागः तद्विभागे सति कल्पना' इति । अत्र ब्रह्मवाअसत् माने जाय तो उसका व्यवहार असंगत हो जायेगा, अर्थात् असत् रजतमूलक विसंवादी प्रवृत्ति आदि रूप कोई व्यवहार नहीं हो पायेगा । सद् - असत् उभयपक्ष की तो बात बार बार हो चुकी है । यदि ऐसी आशंका हो- अवभासमान रजतादि ग्राह्यरूप को भले ही सत् न माना जाय किन्तु ग्राहकाकार तो सत्स्वरूप ही है इसलिये हमें अविद्या मानने की जरूर ही नहीं है ।- तो यह गलत है, क्योंकि ग्राह्याकार रजतादि यदि असत् है तो उसके अवभासमान होते हुये ग्राहकाकार का सत्यरूप से निर्णय कैसे हो सकता है ? तथा रजतादिप्रतिभास से शून्य स्वतंत्र कोई ग्राहकाकार वह हो नहीं सकता।।
सारांश, अविद्या को किसी भी मत में न सत् मान सकते हैं, न असत्, न उभयस्वरूप, किन्तु अनिर्वचनीय है। सद्-असत् या उभयस्वरूप नहीं होने से ही वह ब्रह्म की तरह स दृढस्वभाव नहीं है किन्तु अदृढ स्वभाव एवं मायास्वरूप है इसीलिये उस की निवृत्ति हो सकती है । यदि वह ब्रह्म की तरह दृढस्वभाव होती तो ब्रह्म की तरह अनिवृत्ति स्वभाव के बदले वह निवृत्ति स्वभाव कैसे हो पाती ? स्वभाव का परित्याग दुष्कर होता है । यदि वह शून्यस्वरूप है तब तो स्वयं गगनकुसुमवत् निवृत्त होने से अविद्यानिवृत्ति के लिये पुरुषार्थ ही नहीं होता।
उपरोक्त चर्चा का निष्कर्ष यह है कि अविद्या सत्स्वरूप न होने से अद्वैत का भंग नहीं होता और अनिर्वचेनीय अदृढ माया स्वरूप होने से निवृत्ति भी असंगत नहीं है।
★जीवाश्रित अविद्यापक्ष में प्रश्नोत्तर ★ यदि यह प्रश्न किया जाय कि अविद्या किस की आश्रित है तो इसका उत्तर है जीवों की । यदि कहें कि- वे जीव भी ब्रह्म से विभिन्न तत्त्व नहीं है- तो यह बात ठीक है कि ब्रह्म और जीवों में पारमार्थिक कोई भेद नहीं है। किन्तु ब्रह्म से जीवों के काल्पनिक भेद का प्रतिषेध नहीं है।
यदि ऐसा कहें कि- “जीव और ब्रह्म में भेदस्थापक कल्पना जीवाश्रित है या ब्रह्माश्रित ? 'ब्रह्म की कल्पना' ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म स्वयं सर्व विकल्पों से अतीत = विनिर्मुक्त है, क्योंकि वह शुद्ध विद्यास्वभाव है। 'जीवों की कल्पना' ब्रह्म और जीव में भेदस्थापक है ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकिकल्पना से जीव भिन्न होता है किन्तु कल्पना के पूर्व तो ब्रह्मातिरिक्त जीवभेद है ही नहीं तो कौन भेदस्थापक कल्पना करेगा ? स्पष्ट ही यहाँ अन्योन्याश्रय दोष सिर उठायेगा - कल्पना से जीवभेद होता है और ब्रह्म से जीव का भेद होने पर वह कल्पना करता है ।"* 'यत्तु कस्याऽविद्येति ? जीवानामिति बूमः' (ब्रह्मसिद्धि पृ० १०)
Jain Educationa International
For Personal and Private Use Only
www.jainelibrary.org