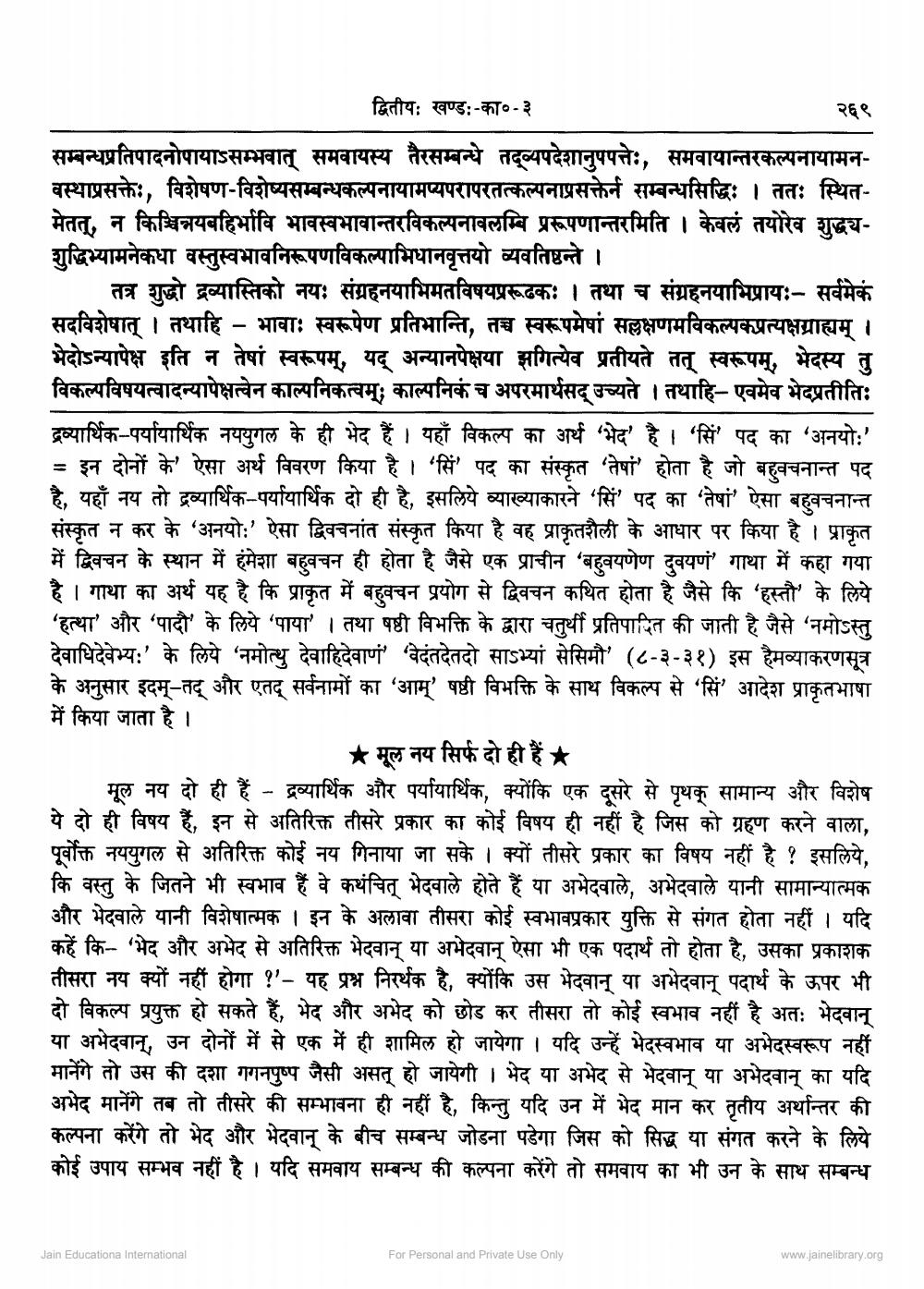________________
द्वितीयः खण्ड:-का०-३
२६९ सम्बन्धप्रतिपादनोपायाऽसम्भवात् समवायस्य तैरसम्बन्धे तद्व्यपदेशानुपपत्तेः, समवायान्तरकल्पनायामनवस्थाप्रसक्तेः, विशेषण-विशेष्यसम्बन्धकल्पनायामप्यपरापरतत्कल्पनाप्रसक्तेर्न सम्बन्धसिद्धिः । ततः स्थितमेतत्, न किञ्चिन्नयवहिर्भावि भावस्वभावान्तरविकल्पनावलम्बि प्ररूपणान्तरमिति । केवलं तयोरेव शुद्धयशुद्धिभ्यामनेकधा वस्तुस्वभावनिरूपणविकल्पाभिधानवृत्तयो व्यवतिष्ठन्ते ।
तत्र शुद्धो द्रव्यास्तिको नयः संग्रहनयाभिमतविषयप्ररूढकः । तथा च संग्रहनयाभिप्राय:- सर्वमेकं सदविशेषात् । तथाहि - भावाः स्वरूपेण प्रतिभान्ति, तच्च स्वरूपमेषां सल्लक्षणमविकल्पकप्रत्यक्षग्राह्यम् । भेदोऽन्यापेक्ष इति न तेषां स्वरूपम्, यद् अन्यानपेक्षया झगित्येव प्रतीयते तत् स्वरूपम्, भेदस्य तु विकल्पविषयत्वादन्यापेक्षत्वेन काल्पनिकत्वम् काल्पनिकं च अपरमार्थसद् उच्यते । तथाहि- एवमेव भेदप्रतीतिः द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिक नययुगल के ही भेद हैं । यहाँ विकल्प का अर्थ 'भेद' है । 'सिं' पद का ‘अनयो:' = इन दोनों के' ऐसा अर्थ विवरण किया है । 'सिं' पद का संस्कृत 'तेषां' होता है जो बहुवचनान्त पद है, यहाँ नय तो द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिक दो ही है, इसलिये व्याख्याकारने 'सिं' पद का 'तेषां' ऐसा बहुवचनान्त संस्कृत न कर के 'अनयोः' ऐसा द्विवचनांत संस्कृत किया है वह प्राकृतशैली के आधार पर किया है । प्राकृत में द्विवचन के स्थान में हमेशा बहुवचन ही होता है जैसे एक प्राचीन 'बहुवयणेण दुवयणं' गाथा में कहा गया है । गाथा का अर्थ यह है कि प्राकृत में बहुवचन प्रयोग से द्विवचन कथित होता है जैसे कि 'हस्तौ' के लिये 'हत्था' और 'पादौ' के लिये 'पाया' । तथा षष्ठी विभक्ति के द्वारा चतुर्थी प्रतिपादित की जाती है जैसे 'नमोऽस्तु देवाधिदेवेभ्यः' के लिये 'नमोत्थु देवाहिदेवाणं' 'वेदंतदेतदो साऽभ्यां सेसिमौ' (८-३-३१) इस हैमव्याकरणसूत्र के अनुसार इदम्-तद् और एतद् सर्वनामों का 'आम्' षष्ठी विभक्ति के साथ विकल्प से 'सिं' आदेश प्राकृतभाषा में किया जाता है।
★ मूल नय सिर्फ दो ही हैं ★ मूल नय दो ही हैं - द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक, क्योंकि एक दूसरे से पृथक् सामान्य और विशेष ये दो ही विषय हैं, इन से अतिरिक्त तीसरे प्रकार का कोई विषय ही नहीं है जिस को ग्रहण करने वाला, पूर्वोक्त नययुगल से अतिरिक्त कोई नय गिनाया जा सके । क्यों तीसरे प्रकार का विषय नहीं है ? इसलिये, कि वस्तु के जितने भी स्वभाव हैं वे कथंचित् भेदवाले होते हैं या अभेदवाले, अभेदवाले यानी सामान्यात्मक
और भेदवाले यानी विशेषात्मक । इन के अलावा तीसरा कोई स्वभावप्रकार युक्ति से संगत होता नहीं । यदि कहें कि- 'भेद और अभेद से अतिरिक्त भेदवान् या अभेदवान् ऐसा भी एक पदार्थ तो होता है, उसका प्रकाशक तीसरा नय क्यों नहीं होगा ?'- यह प्रश्न निरर्थक है, क्योंकि उस भेदवान् या अभेदवान् पदार्थ के ऊपर भी दो विकल्प प्रयुक्त हो सकते हैं, भेद और अभेद को छोड कर तीसरा तो कोई स्वभाव नहीं है अत: भेदवान् या अभेदवान्, उन दोनों में से एक में ही शामिल हो जायेगा। यदि उन्हें भेदस्वभाव या अभेदस्वरूप नहीं मानेंगे तो उस की दशा गगनपुष्प जैसी असत् हो जायेगी । भेद या अभेद से भेदवान् या अभेदवान् का यदि अभेद मानेंगे तब तो तीसरे की सम्भावना ही नहीं है, किन्तु यदि उन में भेद मान कर तृतीय अर्थान्तर की कल्पना करेंगे तो भेद और भेदवान् के बीच सम्बन्ध जोडना पडेगा जिस को सिद्ध या संगत करने के लिये कोई उपाय सम्भव नहीं है। यदि समवाय सम्बन्ध की कल्पना करेंगे तो समवाय का भी उन के साथ सम्बन्ध
Jain Educationa International
For Personal and Private Use Only
www.jainelibrary.org