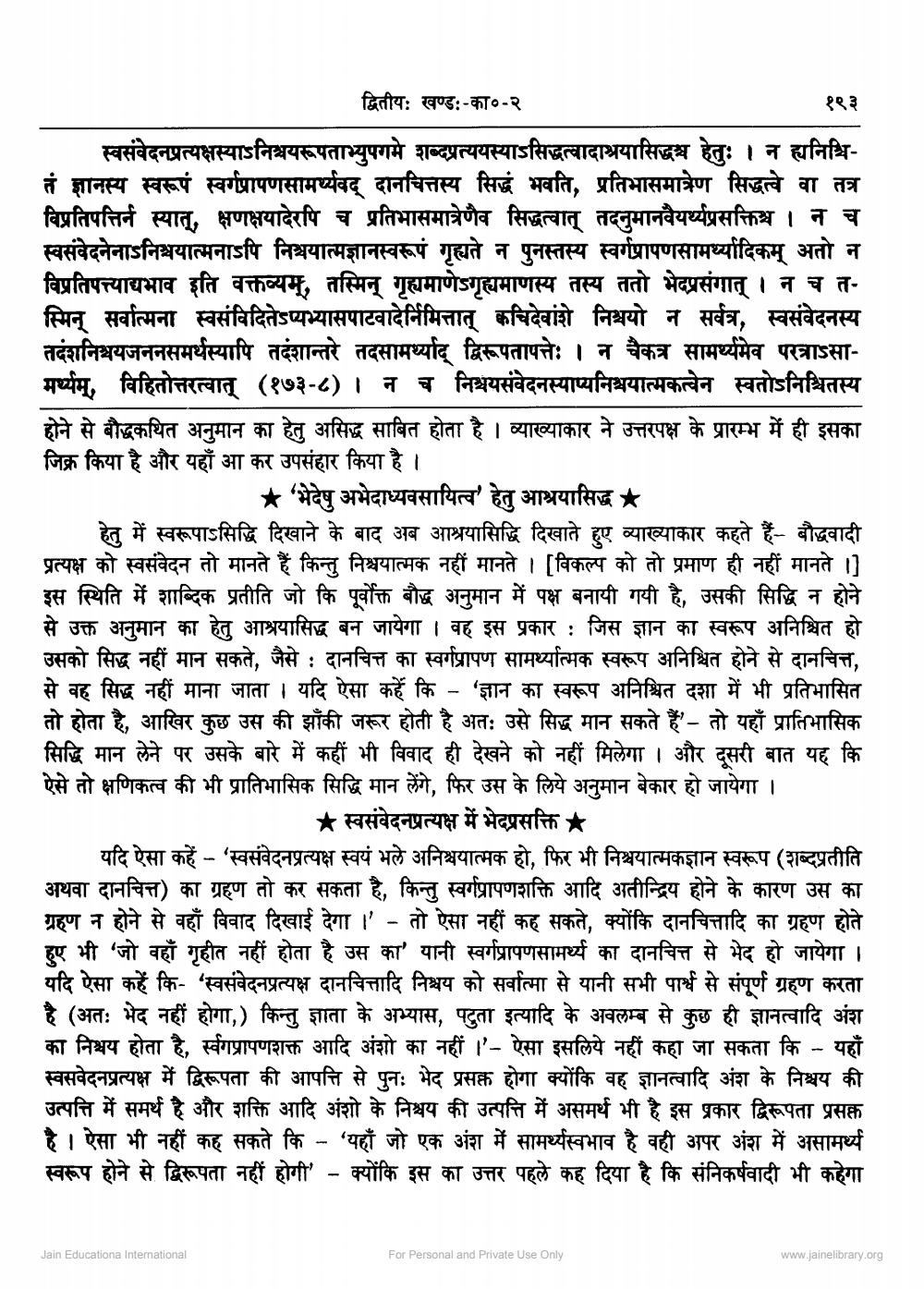________________
१९३
द्वितीयः खण्ड:-का०-२ स्वसंवेदनप्रत्यक्षस्याऽनिश्चयरूपताभ्युपगमे शब्दप्रत्ययस्याऽसिद्धत्वादाश्रयासिद्धश्च हेतुः । न ह्यनिश्चितं ज्ञानस्य स्वरूपं स्वर्गप्रापणसामर्थ्यवद् दानचित्तस्य सिद्धं भवति, प्रतिभासमात्रेण सिद्धत्वे वा तत्र विप्रतिपत्तिर्न स्यात्, क्षणक्षयादेरपि च प्रतिभासमात्रेणैव सिद्धत्वात् तदनुमानवैयर्थ्यप्रसक्तिश्च । न च स्वसंवेदनेनाऽनिश्चयात्मनाऽपि निश्चयात्मज्ञानस्वरूपं गृह्यते न पुनस्तस्य स्वर्गप्रापणसामर्थ्यादिकम् अतो न विप्रतिपत्त्यायभाव इति वक्तव्यम्, तस्मिन् गृह्यमाणेऽगृह्यमाणस्य तस्य ततो भेदप्रसंगात् । न च त. स्मिन् सर्वात्मना स्वसंविदितेऽप्यभ्यासपाटवादेनिमित्तात् कचिदेवांशे निश्चयो न सर्वत्र, स्वसंवेदनस्य तदंशनिश्चयजननसमर्थस्यापि तदंशान्तरे तदसामर्थ्याद् द्विरूपतापत्तेः । न चैकत्र सामर्थ्यमेव परत्राऽसामर्थ्यम्, विहितोत्तरत्वात् (१७३-८)। न च निश्चयसंवेदनस्याप्यनिश्चयात्मकत्वेन स्वतोऽनिश्चितस्य होने से बौद्धकथित अनुमान का हेतु असिद्ध साबित होता है । व्याख्याकार ने उत्तरपक्ष के प्रारम्भ में ही इसका जिक्र किया है और यहाँ आ कर उपसंहार किया है ।
★ 'भेदेषु अभेदाध्यवसायित्व' हेतु आश्रयासिद्ध ★ हेतु में स्वरूपाऽसिद्धि दिखाने के बाद अब आश्रयासिद्धि दिखाते हुए व्याख्याकार कहते हैं- बौद्धवादी प्रत्यक्ष को स्वसंवेदन तो मानते हैं किन्तु निश्चयात्मक नहीं मानते । [विकल्प को तो प्रमाण ही नहीं मानते ।] इस स्थिति में शाब्दिक प्रतीति जो कि पूर्वोक्त बौद्ध अनुमान में पक्ष बनायी गयी है, उसकी सिद्धि न होने से उक्त अनुमान का हेतु आश्रयासिद्ध बन जायेगा । वह इस प्रकार : जिस ज्ञान का स्वरूप अनिश्चित हो उसको सिद्ध नहीं मान सकते, जैसे : दानचित्त का स्वर्गप्रापण सामर्थ्यात्मक स्वरूप अनिश्चित होने से दानचित्त, से वह सिद्ध नहीं माना जाता । यदि ऐसा कहें कि - 'ज्ञान का स्वरूप अनिश्चित दशा में भी प्रतिभासित तो होता है, आखिर कुछ उस की झाँकी जरूर होती है अत: उसे सिद्ध मान सकते हैं'- तो यहाँ प्रातिभासिक सिद्धि मान लेने पर उसके बारे में कहीं भी विवाद ही देखने को नहीं मिलेगा । और दूसरी बात यह कि ऐसे तो क्षणिकत्व की भी प्रातिभासिक सिद्धि मान लेंगे, फिर उस के लिये अनुमान बेकार हो जायेगा ।
★ स्वसंवेदनप्रत्यक्ष में भेदप्रसक्ति* यदि ऐसा कहें - 'स्वसंवेदनप्रत्यक्ष स्वयं भले अनिश्चयात्मक हो, फिर भी निश्चयात्मकज्ञान स्वरूप (शब्दप्रतीति अथवा दानचित्त) का ग्रहण तो कर सकता है, किन्तु स्वर्गप्रापणशक्ति आदि अतीन्द्रिय होने के कारण उस का ग्रहण न होने से वहाँ विवाद दिखाई देगा।' - तो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि दानचित्तादि का ग्रहण होते हुए भी 'जो वहाँ गृहीत नहीं होता है उस का' यानी स्वर्गप्रापणसामर्थ्य का दानचित्त से भेद हो जायेगा । यदि ऐसा कहें कि- 'स्वसंवेदनप्रत्यक्ष दानचित्तादि निश्चय को सर्वात्मा से यानी सभी पार्थ से संपूर्ण ग्रहण करता है (अतः भेद नहीं होगा,) किन्तु ज्ञाता के अभ्यास, पटुता इत्यादि के अवलम्ब से कुछ ही ज्ञानत्वादि अंश का निश्चय होता है, स्र्वगप्रापणशक्त आदि अंशो का नहीं ।'- ऐसा इसलिये नहीं कहा जा सकता कि - यहाँ स्वसवेदनप्रत्यक्ष में द्विरूपता की आपत्ति से पुन: भेद प्रसक्त होगा क्योंकि वह ज्ञानत्वादि अंश के निश्चय की उत्पत्ति में समर्थ है और शक्ति आदि अंशो के निश्चय की उत्पत्ति में असमर्थ भी है इस प्रकार द्विरूपता प्रसक्त है । ऐसा भी नहीं कह सकते कि - 'यहाँ जो एक अंश में सामर्थ्यस्वभाव है वही अपर अंश में असामर्थ्य स्वरूप होने से द्विरूपता नहीं होगी' - क्योंकि इस का उत्तर पहले कह दिया है कि संनिकर्षवादी भी कहेगा
Jain Educationa International
For Personal and Private Use Only
www.jainelibrary.org