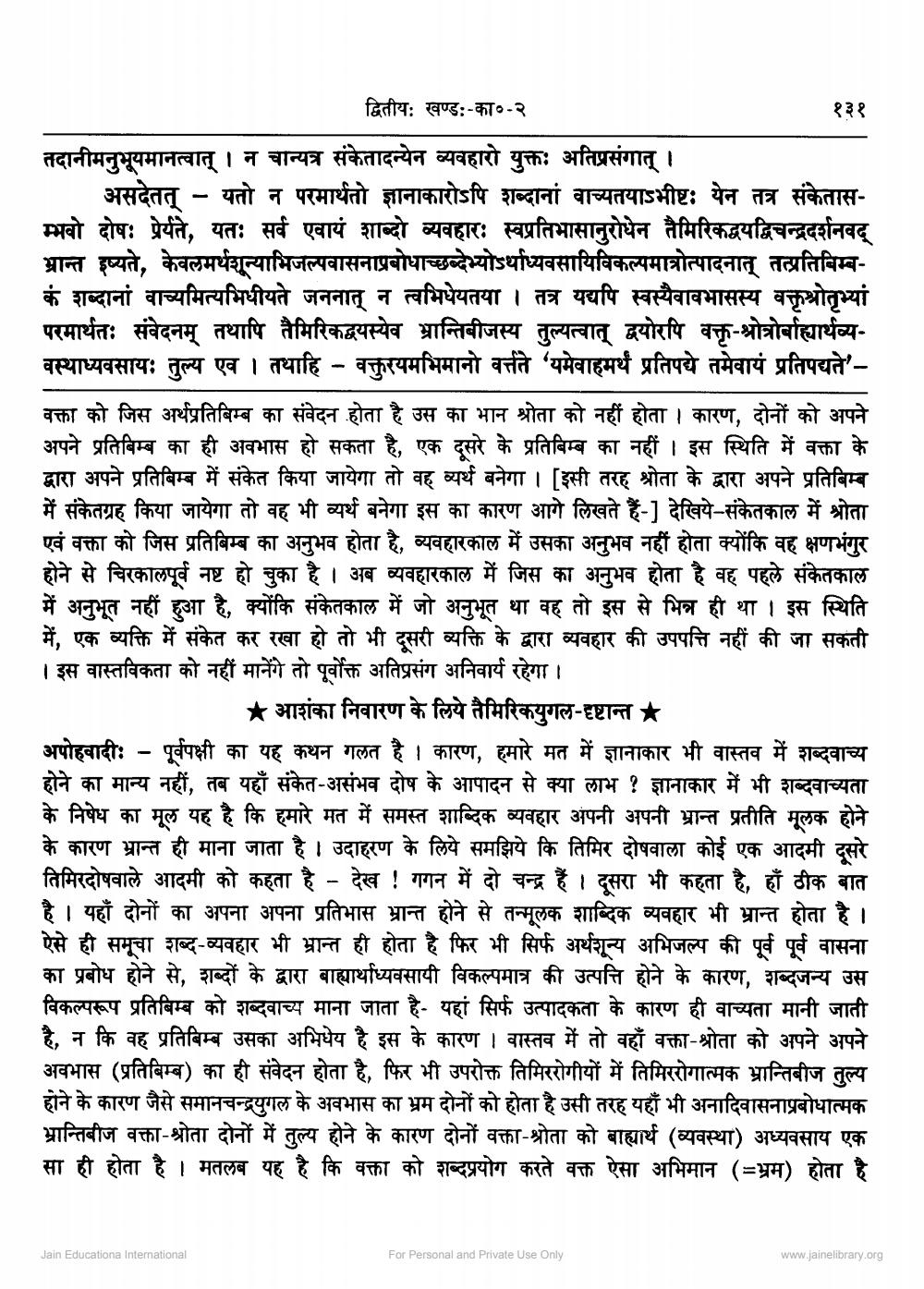________________
द्वितीयः खण्डः - का० - २
तदानीमनुभूयमानत्वात् । न चान्यत्र संकेतादन्येन व्यवहारो युक्तः अतिप्रसंगात् ।
असदेतत् - यतो न परमार्थतो ज्ञानाकारोऽपि शब्दानां वाच्यतयाऽभीष्टः येन तत्र संकेतासम्भवो दोषः प्रेर्यंते, यतः सर्व एवायं शाब्दो व्यवहारः स्वप्रतिभासानुरोधेन तैमिरिकद्वयद्विचन्द्रदर्शनवद् भ्रान्त इष्यते, केवलमर्थशून्याभिजल्पवासनाप्रबोधाच्छब्देभ्योऽर्थाध्यवसायिविकल्पमात्रोत्पादनात् तत्प्रतिबिम्बकं शब्दानां वाच्यमित्यभिधीयते जननात् न त्वभिधेयतया । तत्र यद्यपि स्वस्यैवावभासस्य वक्तृश्रोतृभ्यां परमार्थतः संवेदनम् तथापि तैमिरिकद्वयस्येव भ्रान्तिबीजस्य तुल्यत्वात् द्वयोरपि वक्तृ-श्रोत्रोर्बाह्यार्थव्यवस्थाध्यवसायः तुल्य एव । तथाहि - वक्तुरयमभिमानो वर्त्तते 'यमेवाहमर्थं प्रतिपद्ये तमेवायं प्रतिपद्यते'
वक्ता को जिस अर्थप्रतिबिम्ब का संवेदन होता है उस का भान श्रोता को नहीं होता । कारण, दोनों को अपने अपने प्रतिबिम्ब का ही अवभास हो सकता है, एक दूसरे के प्रतिबिम्ब का नहीं । इस स्थिति में वक्ता के द्वारा अपने प्रतिबिम्ब में संकेत किया जायेगा तो वह व्यर्थ बनेगा । [ इसी तरह श्रोता के द्वारा अपने प्रतिबिम्ब में संकेतग्रह किया जायेगा तो वह भी व्यर्थ बनेगा इस का कारण आगे लिखते हैं-] देखिये- संकेतकाल में श्रोता एवं वक्ता को जिस प्रतिबिम्ब का अनुभव होता है, व्यवहारकाल में उसका अनुभव नहीं होता क्योंकि वह क्षणभंगुर होने से चिरकालपूर्व नष्ट हो चुका है । अब व्यवहारकाल में जिस का अनुभव होता है वह पहले संकेतकाल में अनुभूत नहीं हुआ है, क्योंकि संकेतकाल में जो अनुभूत था वह तो इस से भिन्न ही था । इस स्थि में, एक व्यक्ति में संकेत कर रखा हो तो भी दूसरी व्यक्ति के द्वारा व्यवहार की उपपत्ति नहीं की जा सकती । इस वास्तविकता को नहीं मानेंगे तो पूर्वोक्त अतिप्रसंग अनिवार्य रहेगा ।
★ आशंका निवारण के लिये तैमिरिकयुगल - दृष्टान्त ★
अपोहवादीः पूर्वपक्षी का यह कथन गलत है । कारण, हमारे मत में ज्ञानाकार भी वास्तव में शब्दवाच्य होने का मान्य नहीं, तब यहाँ संकेत - असंभव दोष के आपादन से क्या लाभ ? ज्ञानाकार में भी शब्दवाच्यता के निषेध का मूल यह है कि हमारे मत में समस्त शाब्दिक व्यवहार अपनी अपनी भ्रान्त प्रतीति मूलक होने के कारण भ्रान्त ही माना जाता है । उदाहरण के लिये समझिये कि तिमिर दोषवाला कोई एक आदमी दूसरे तिमिरदोषवाले आदमी को कहता है - देख ! गगन में दो चन्द्र हैं । दूसरा भी कहता है, हाँ ठीक बात है । यहाँ दोनों का अपना अपना प्रतिभास भ्रान्त होने से तन्मूलक शाब्दिक व्यवहार भी भ्रान्त होता है । ऐसे ही समूचा शब्द - व्यवहार भी भ्रान्त ही होता है फिर भी सिर्फ अर्थशून्य अभिजल्प की पूर्व पूर्व वासना का प्रबोध होने से, शब्दों के द्वारा बाह्यार्थाध्यवसायी विकल्पमात्र की उत्पत्ति होने के कारण, शब्दजन्य उस विकल्परूप प्रतिबिम्ब को शब्दवाच्य माना जाता है- यहां सिर्फ उत्पादकता के कारण ही वाच्यता मानी जाती है, न कि वह प्रतिबिम्ब उसका अभिधेय है इस के कारण । वास्तव में तो वहाँ वक्ता - श्रोता को अपने अपने अवभास (प्रतिबिम्ब) का ही संवेदन होता है, फिर भी उपरोक्त तिमिररोगीयों में तिमिररोगात्मक भ्रान्तिबीज तुल्य होने के कारण जैसे समानचन्द्रयुगल के अवभास का भ्रम दोनों को होता है उसी तरह यहाँ भी अनादिवासनाप्रबोधात्मक भ्रान्तिबीज वक्ता - श्रोता दोनों में तुल्य होने के कारण दोनों वक्ता - श्रोता को बाह्यार्थ (व्यवस्था) अध्यवसाय एक साही होता है । मतलब यह है कि वक्ता को शब्दप्रयोग करते वक्त ऐसा अभिमान ( = भ्रम ) होता है
-
१३१
Jain Educationa International
For Personal and Private Use Only
www.jainelibrary.org