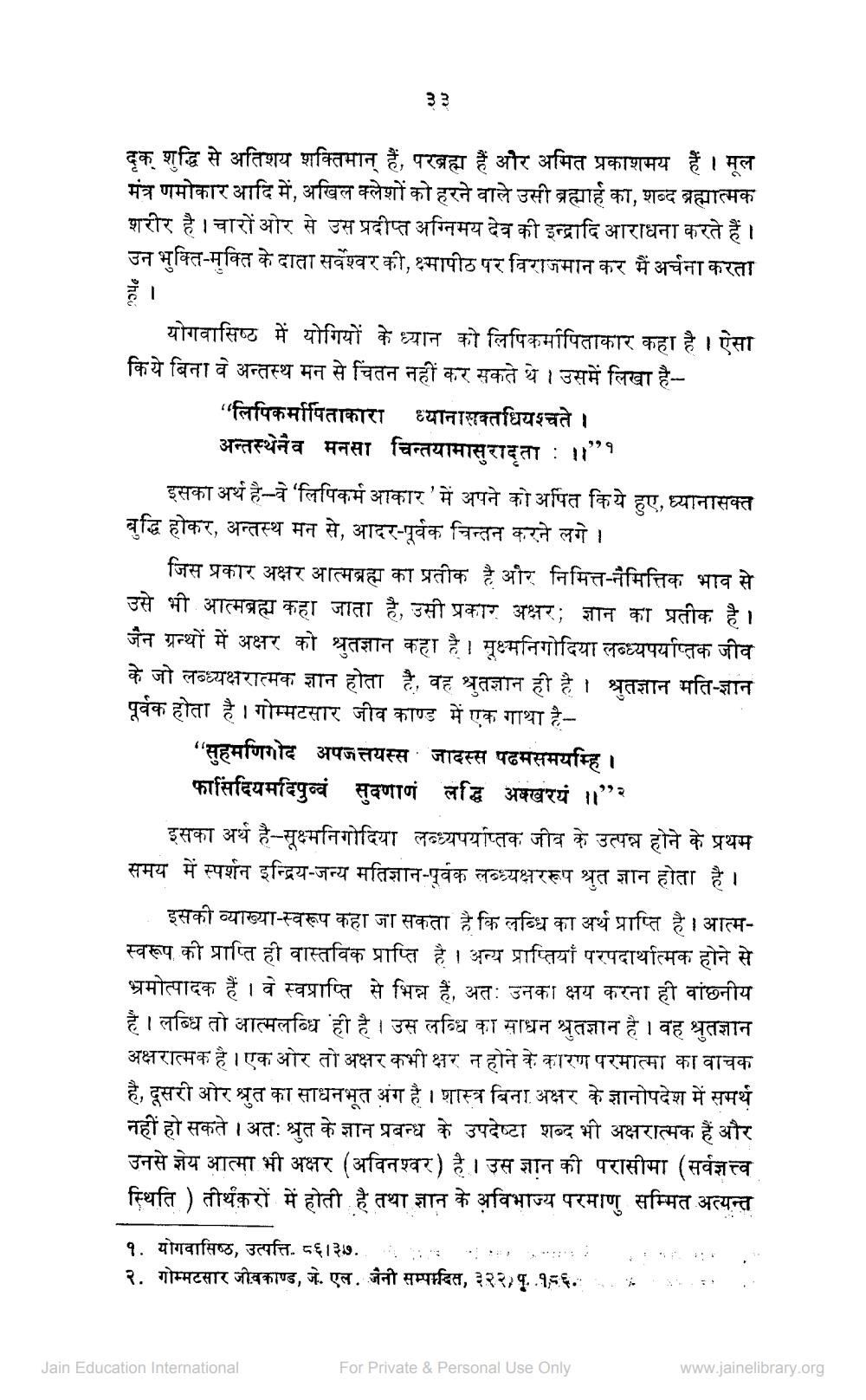________________
३३
दृ शुद्धि से अतिशय शक्तिमान् हैं, परब्रह्म हैं और अमित प्रकाशमय हैं । मूल मकर आदि में, अखिल क्लेशों को हरने वाले उसी ब्रह्मार्ह का शब्द ब्रह्मात्मक शरीर है। चारों ओर से उस प्रदीप्त अग्निमय देव की इन्द्रादि आराधना करते हैं । उन भुक्ति-मुक्ति के दाता सर्वेश्वर की, क्ष्मापीठ पर विराजमान कर मैं अर्चना करता हूँ ।
योगवासिष्ठ में योगियों के ध्यान को लिपिकर्मापिताकार कहा है । ऐसा किये बिना वे अन्तस्थ मन से चिंतन नहीं कर सकते थे। उसमें लिखा है
“लिपिकर्मापिताकारा ध्यानासवतधियश्चते ।
अन्तस्थेनैव मनसा चिन्तयामासुरादृता: ।। " "
इसका अर्थ है - वे 'लिपिकर्म आकार' में अपने को अर्पित किये हुए, ध्यानासक्त बुद्धि होकर, अन्तस्थ मन से, आदर-पूर्वक चिन्तन करने लगे ।
जिस प्रकार अक्षर आत्मब्रह्म का प्रतीक है और निमित्तनैमित्तिक भाव से उसे भी आत्मब्रह्म कहा जाता है, उसी प्रकार अक्षर ज्ञान का प्रतीक है । जैन ग्रन्थों में अक्षर को श्रुतज्ञान कहा है। सूक्ष्मनिगोदिया लब्ध्यपर्याप्तक जीव के जो लब्ध्यक्षरात्मक ज्ञान होता है, वह श्रुतज्ञान ही है। श्रुतज्ञान मति - ज्ञान पूर्वक होता है । गोम्मटसार जीव काण्ड में एक गाथा है
"सुहमणिगोद अपजत्तयस्स जादस्स पढमसमयम्हि । फासिंदियमदिपुवं सुवणाणं लद्धि अक्खरयं ॥ २
इसका अर्थ है - सूक्ष्मनिगोदिया लब्ध्यपर्याप्तक जीव के उत्पन्न होने के प्रथम समय में स्पर्शन इन्द्रिय-जन्य मतिज्ञान- पूर्वक लब्ध्यक्षररूप श्रुत ज्ञान होता है ।
इसकी व्याख्या स्वरूप कहा जा सकता है कि लब्धि का अर्थ प्राप्ति है। आत्मस्वरूप की प्राप्ति ही वास्तविक प्राप्ति है । अन्य प्राप्तियाँ परपदार्थात्मक होने से भ्रमोत्पादक हैं । वे स्वप्राप्ति से भिन्न हैं, अतः उनका क्षय करना ही वांछनीय है । लब्धि तो आत्मलब्धि ही है। उस लब्धि का साधन श्रुतज्ञान है । वह श्रुतज्ञान अक्षरात्मक है । एक ओर तो अक्षर कभी क्षर न होने के कारण परमात्मा का वाचक है, दूसरी ओर श्रुत का साधनभूत अंग है । शास्त्र बिना अक्षर के ज्ञानोपदेश में समर्थ नहीं हो सकते । अतः श्रुत के ज्ञान प्रबन्ध के उपदेष्टा शब्द भी अक्षरात्मक हैं और उनसे ज्ञेय आत्मा भी अक्षर (अविनश्वर ) है । उस ज्ञान की परासीमा ( सर्वज्ञत्त्व स्थिति ) तीर्थंकरों में होती है तथा ज्ञान के अविभाज्य परमाणु सम्मित अत्यन्त
१. योगवासिष्ठ, उत्पत्ति. ८६।३७.
२. गोम्मटसार जीवकाण्ड, जे. एल. जैनी सम्पादित, ३२२, पू. १६६.५
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org