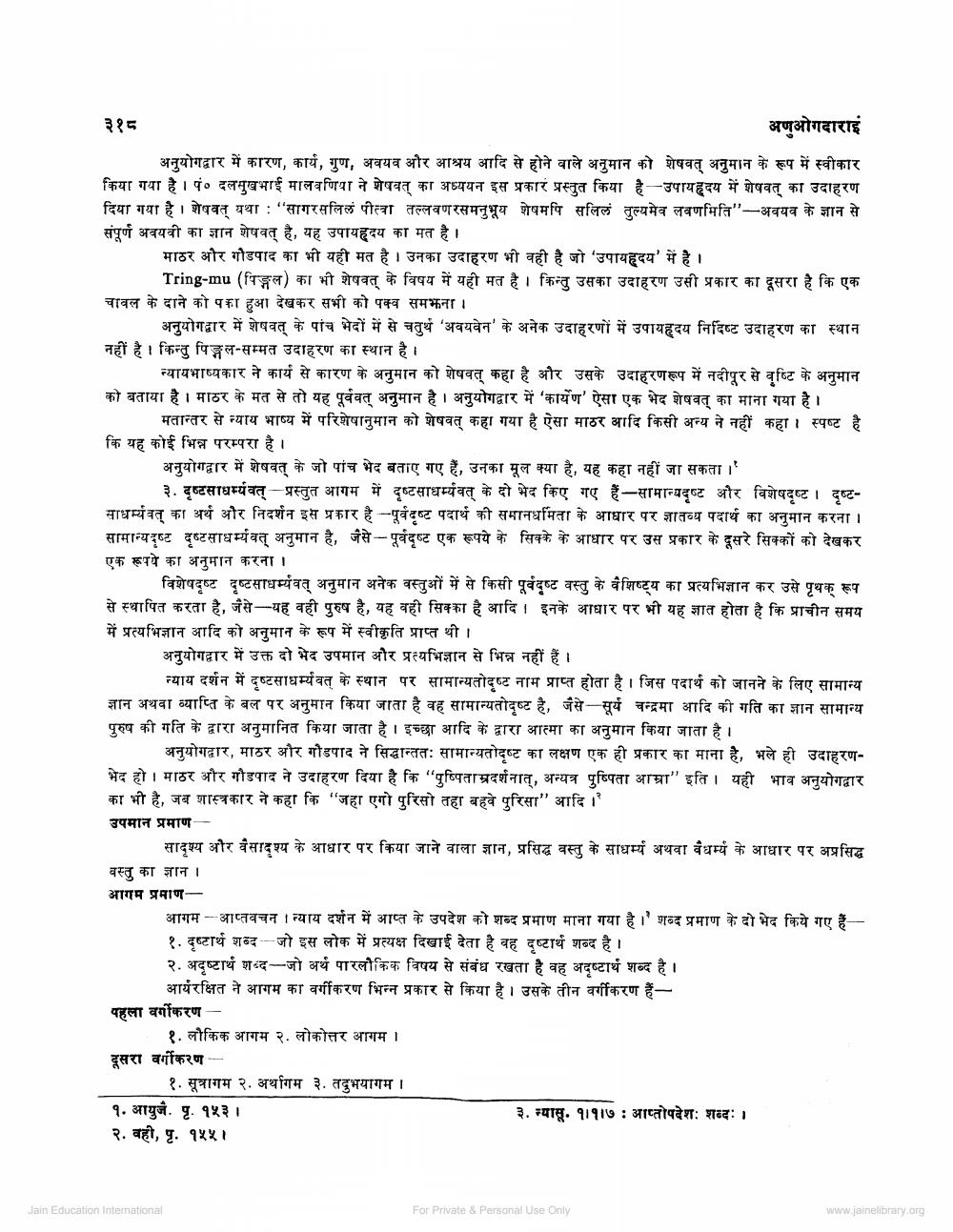________________
३१८
अणुओगदाराई अनुयोगद्वार में कारण, कार्य, गुण, अवयव और आश्रय आदि से होने वाले अनुमान को शेषवत् अनुमान के रूप में स्वीकार किया गया है । पं० दलसुखभाई मालवणिया ने शेषवत् का अध्ययन इस प्रकार प्रस्तुत किया है-उपायहृदय में शेषवत् का उदाहरण दिया गया है। शेषवत् यथा : "सागर सलिलं पीत्वा तल्लवणरसमनुभूय शेषमपि सलिलं तुल्यमेव लवणमिति"-अवयव के ज्ञान से संपूर्ण अवयवी का ज्ञान शेषवत् है, यह उपायहृदय का मत है।
माठर और गौडपाद का भी यही मत है । उनका उदाहरण भी वही है जो 'उपायहृदय' में है।
Tring-mu (पिङ्गल) का भी शेषवत् के विषय में यही मत है। किन्तु उसका उदाहरण उसी प्रकार का दूसरा है कि एक चावल के दाने को पका हुआ देखकर सभी को पक्व समझना ।
___अनुयोगद्वार में शेषवत् के पांच भेदों में से चतुर्थ 'अवयवेन' के अनेक उदाहरणों में उपायहृदय निर्दिष्ट उदाहरण का स्थान नहीं है। किन्तु पिङ्गल-सम्मत उदाहरण का स्थान है।
न्यायभाष्यकार ने कार्य से कारण के अनुमान को शेषवत् कहा है और उसके उदाहरणरूप में नदीपुर से वृष्टि के अनुमान को बताया है। माठर के मत से तो यह पूर्ववत् अनुमान है । अनुयोगद्वार में 'कार्येण' ऐसा एक भेद शेषवत् का माना गया है।
___ मतान्तर से न्याय भाष्य में परिशेषानुमान को शेषवत् कहा गया है ऐसा माठर आदि किसी अन्य ने नहीं कहा। स्पष्ट है कि यह कोई भिन्न परम्परा है।
अनुयोगद्वार में शेषवत् के जो पांच भेद बताए गए हैं, उनका मूल क्या है, यह कहा नहीं जा सकता।'
३. दृष्टसाधर्म्यवत्-प्रस्तुत आगम में दृष्टसाधर्म्यवत् के दो भेद किए गए हैं-सामान्यदृष्ट और विशेषदृष्ट । दृष्टसाधर्म्यवत् का अर्थ और निदर्शन इस प्रकार है-पूर्वदृष्ट पदार्थ की समानधर्मिता के आधार पर ज्ञातव्य पदार्थ का अनुमान करना। सामान्यदृष्ट दृष्टसाधर्म्यवत् अनुमान है, जैसे- पूर्वदृष्ट एक रूपये के सिक्के के आधार पर उस प्रकार के दूसरे सिक्कों को देखकर एक रूपये का अनुमान करना।
विशेषदृष्ट दृष्टसाधर्म्यवत् अनुमान अनेक वस्तुओं में से किसी पूर्वदृष्ट वस्तु के वैशिष्ट्य का प्रत्यभिज्ञान कर उसे पृथक् रूप से स्थापित करता है, जैसे-यह वही पुरुष है, यह वही सिक्का है आदि। इनके आधार पर भी यह ज्ञात होता है कि प्राचीन समय में प्रत्यभिज्ञान आदि को अनुमान के रूप में स्वीकृति प्राप्त थी।
अनुयोगद्वार में उक्त दो भेद उपमान और प्रत्यभिज्ञान से भिन्न नहीं हैं।
न्याय दर्शन में दृष्टसाधर्म्यवत् के स्थान पर सामान्यतोदृष्ट नाम प्राप्त होता है। जिस पदार्थ को जानने के लिए सामान्य ज्ञान अथवा व्याप्ति के बल पर अनुमान किया जाता है वह सामान्यतोदृष्ट है, जैसे सूर्य चन्द्रमा आदि की गति का ज्ञान सामान्य पुरुष की गति के द्वारा अनुमानित किया जाता है । इच्छा आदि के द्वारा आत्मा का अनुमान किया जाता है।
अनुयोगद्वार, माठर और गौडपाद ने सिद्धान्तत: सामान्यतोदृष्ट का लक्षण एक ही प्रकार का माना है, भले ही उदाहरणभेद हो । माठर और गौडपाद ने उदाहरण दिया है कि "पुष्पिताम्रदर्शनात्, अन्यत्र पुष्पिता आम्रा" इति । यही भाव अनुयोगद्वार का भी है, जब शास्त्रकार ने कहा कि "जहा एगो पुरिसो तहा बहवे पुरिसा" आदि ।' उपमान प्रमाण
सादृश्य और वैसाश्य के आधार पर किया जाने वाला ज्ञान, प्रसिद्ध वस्तु के साधर्म्य अथवा वैधर्म्य के आधार पर अप्रसिद्ध वस्तु का ज्ञान । आगम प्रमाण
आगम-आप्तवचन । न्याय दर्शन में आप्त के उपदेश को शब्द प्रमाण माना गया है। शब्द प्रमाण के दो भेद किये गए हैं१. दृष्टार्थ शब्द-जो इस लोक में प्रत्यक्ष दिखाई देता है वह दृष्टार्थ शब्द है। २. अदृष्टार्थ शब्द-जो अर्थ पारलौकिक विषय से संबंध रखता है वह अदृष्टार्थ शब्द है।
आर्यरक्षित ने आगम का वर्गीकरण भिन्न प्रकार से किया है। उसके तीन वर्गीकरण हैंपहला वर्गीकरण
१. लौकिक आगम २. लोकोत्तर आगम । दूसरा वर्गीकरण
१. सूत्रागम २. अर्थागम ३. तदुभयागम । १. आयुज. पृ. १५३ ।
३. न्यासू. १।१७ : आप्तोपदेशः शब्दः । २. वही, पृ. १५५।
Jain Education Intemational
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org