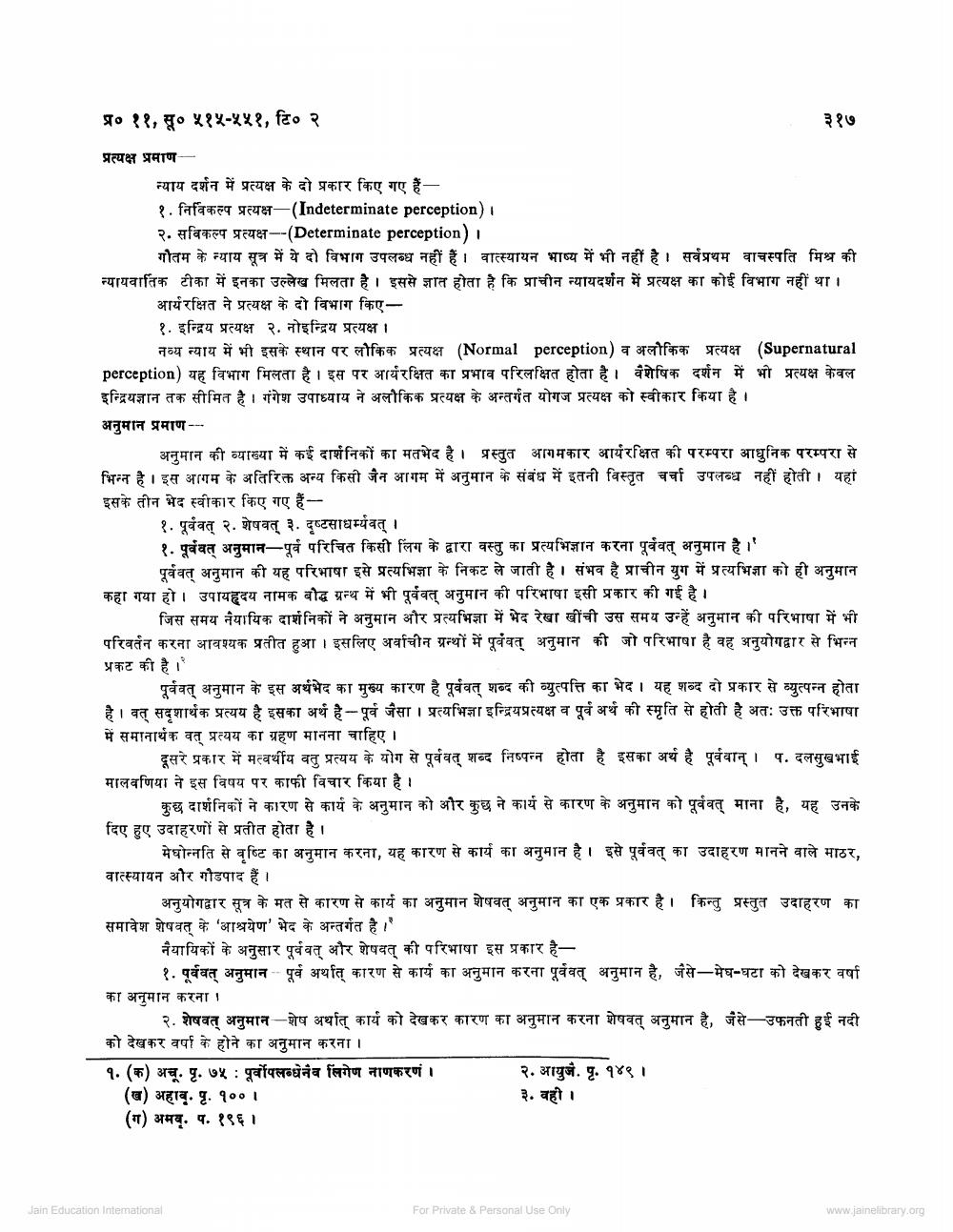________________
प्र० ११, सू० ५१५-५५१, टि० २
३१७
प्रत्यक्ष प्रमाण
न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष के दो प्रकार किए गए हैं१. निर्विकल्प प्रत्यक्ष-(Indeterminate perception)। २. सविकल्प प्रत्यक्ष--(Determinate perception)।
गौतम के न्याय सूत्र में ये दो विभाग उपलब्ध नहीं हैं। वात्स्यायन भाष्य में भी नहीं है। सर्वप्रथम वाचस्पति मिश्र की न्यायवार्तिक टीका में इनका उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन न्यायदर्शन में प्रत्यक्ष का कोई विभाग नहीं था।
आर्य रक्षित ने प्रत्यक्ष के दो विभाग किए१. इन्द्रिय प्रत्यक्ष २. नोइन्द्रिय प्रत्यक्ष ।
नव्य न्याय में भी इसके स्थान पर लौकिक प्रत्यक्ष (Normal perception) व अलौकिक प्रत्यक्ष (Supernatural perception) यह विभाग मिलता है । इस पर आर्यरक्षित का प्रभाव परिलक्षित होता है। वैशेषिक दर्शन में भी प्रत्यक्ष केवल इन्द्रियज्ञान तक सीमित है। गंगेश उपाध्याय ने अलौकिक प्रत्यक्ष के अन्तर्गत योगज प्रत्यक्ष को स्वीकार किया है।
अनुमान प्रमाण--
___अनुमान की व्याख्या में कई दार्शनिकों का मतभेद है। प्रस्तुत आगमकार आर्यरक्षित की परम्परा आधुनिक परम्परा से भिन्न है। इस आगम के अतिरिक्त अन्य किसी जैन आगम में अनुमान के संबंध में इतनी विस्तृत चर्चा उपलब्ध नहीं होती। यहां इसके तीन भेद स्वीकार किए गए हैं
१. पूर्ववत् २. शेषवत् ३. दृष्टसाधर्म्यवत् ।। १. पूर्ववत् अनुमान-पूर्व परिचित किसी लिंग के द्वारा वस्तु का प्रत्यभिज्ञान करना पूर्ववत् अनुमान है।'
पूर्ववत् अनुमान की यह परिभाषा इसे प्रत्यभिज्ञा के निकट ले जाती है। संभव है प्राचीन युग में प्रत्यभिज्ञा को ही अनुमान कहा गया हो। उपायहृदय नामक बौद्ध ग्रन्थ में भी पूर्ववत् अनुमान की परिभाषा इसी प्रकार की गई है।
जिस समय नैयायिक दार्शनिकों ने अनुमान और प्रत्यभिज्ञा में भेद रेखा खींची उस समय उन्हें अनुमान की परिभाषा में भी परिवर्तन करना आवश्यक प्रतीत हुआ । इसलिए अर्वाचीन ग्रन्थों में पूर्ववत् अनुमान की जो परिभाषा है वह अनुयोगद्वार से भिन्न प्रकट की है।
पूर्ववत् अनुमान के इस अर्थभेद का मुख्य कारण है पूर्ववत् शब्द की व्युत्पत्ति का भेद । यह शब्द दो प्रकार से व्युत्पन्न होता है । वत् सदृशार्थक प्रत्यय है इसका अर्थ है-पूर्व जैसा । प्रत्यभिज्ञा इन्द्रियप्रत्यक्ष व पूर्व अर्थ की स्मृति से होती है अतः उक्त परिभाषा में समानार्थक वत् प्रत्यय का ग्रहण मानना चाहिए।
दूसरे प्रकार में मत्वर्थीय वतु प्रत्यय के योग से पूर्ववत् शब्द निष्पन्न होता है इसका अर्थ है पूर्ववान् । प. दलसुखभाई मालवणिया ने इस विषय पर काफी विचार किया है।
कुछ दार्शनिकों ने कारण से कार्य के अनुमान को और कुछ ने कार्य से कारण के अनुमान को पूर्ववत् माना है, यह उनके दिए हुए उदाहरणों से प्रतीत होता है।
मेघोन्नति से वृष्टि का अनुमान करना, यह कारण से कार्य का अनुमान है। इसे पूर्ववत् का उदाहरण मानने वाले माठर, वात्स्यायन और गौडपाद हैं।
अनुयोगद्वार सूत्र के मत से कारण से कार्य का अनुमान शेषवत् अनुमान का एक प्रकार है। किन्तु प्रस्तुत उदाहरण का समावेश शेषवत् के 'आश्रयेण' भेद के अन्तर्गत है।
नैयायिकों के अनुसार पूर्ववत् और शेषवत् की परिभाषा इस प्रकार है
१. पूर्ववत् अनुमान पूर्व अर्थात् कारण से कार्य का अनुमान करना पूर्ववत् अनुमान है, जैसे-मेघ-घटा को देखकर वर्षा का अनुमान करना।
२. शेषवत् अनुमान–शेष अर्थात् कार्य को देखकर कारण का अनुमान करना शेषवत् अनुमान है, जैसे-उफनती हुई नदी को देखकर वर्षा के होने का अनुमान करना । १. (क) अचू. पृ. ७५ : पूर्वोपलब्धेनैव लिगेण नाणकरणं । २. आयुज. पृ. १४९ । (ख) अहाव. पृ. १००।
३. वही। (ग) अमवृ. प. १९६ ।
Jain Education Intemational
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org