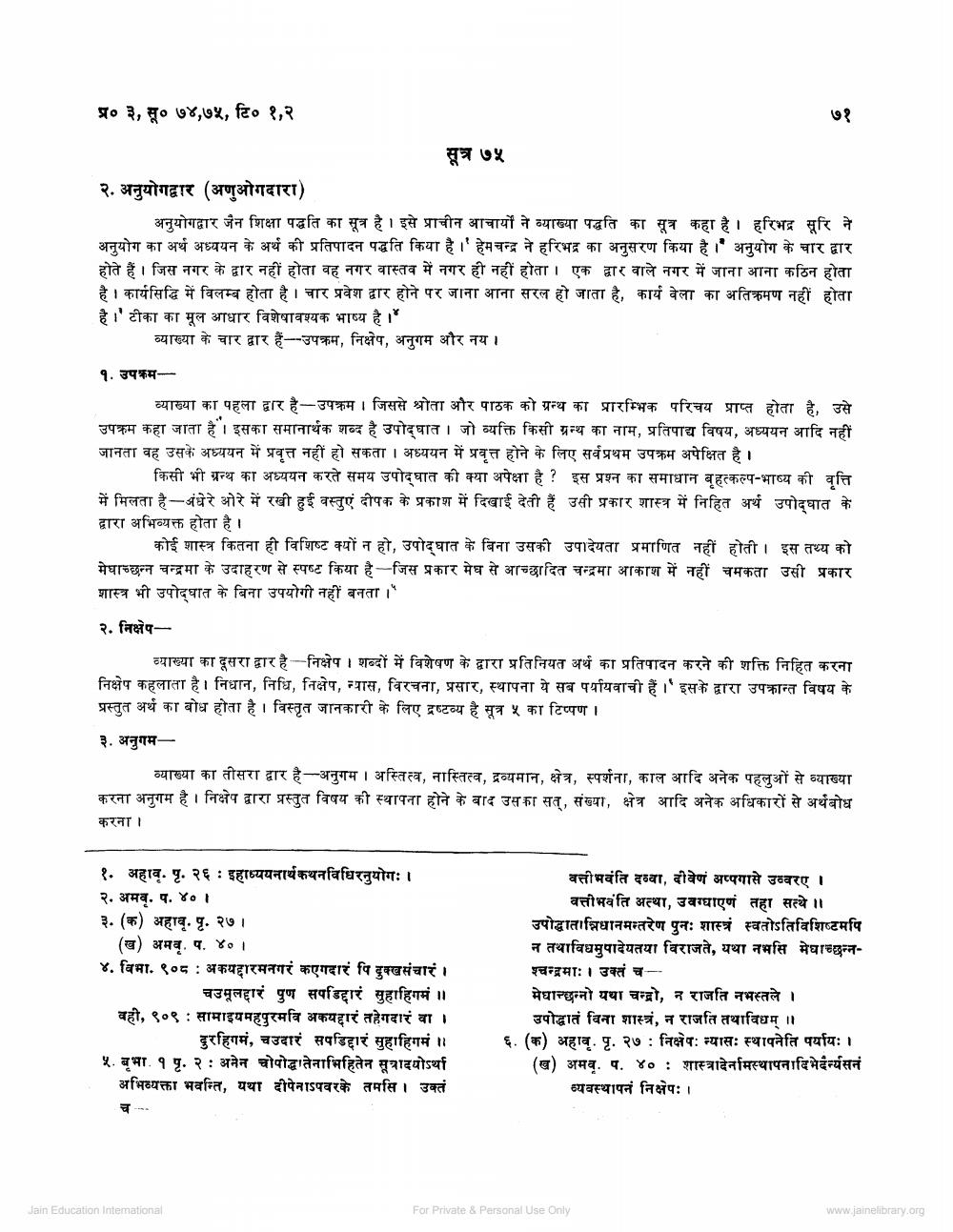________________
प्र०३, सू० ७४,७५, टि० १,२
सूत्र ७५ २. अनुयोगद्वार (अणुओगदारा)
अनुयोगद्वार जैन शिक्षा पद्धति का सूत्र है । इसे प्राचीन आचार्यों ने व्याख्या पद्धति का सूत्र कहा है। हरिभद्र सूरि ने अनुयोग का अर्थ अध्ययन के अर्थ की प्रतिपादन पद्धति किया है। हेमचन्द्र ने हरिभद्र का अनुसरण किया है।' अनुयोग के चार द्वार होते हैं। जिस नगर के द्वार नहीं होता वह नगर वास्तव में नगर ही नहीं होता। एक द्वार वाले नगर में जाना आना कठिन होता है। कार्यसिद्धि में विलम्ब होता है। चार प्रवेश द्वार होने पर जाना आना सरल हो जाता है, कार्य वेला का अतिक्रमण नहीं होता है।' टीका का मूल आधार विशेषावश्यक भाष्य है।'
व्याख्या के चार द्वार हैं-उपक्रम, निक्षेप, अनुगम और नय । १. उपक्रम
व्याख्या का पहला द्वार है-उपक्रम । जिससे श्रोता और पाठक को ग्रन्थ का प्रारम्भिक परिचय प्राप्त होता है, उसे उपक्रम कहा जाता है। इसका समानार्थक शब्द है उपोद्घात । जो व्यक्ति किसी ग्रन्थ का नाम, प्रतिपाद्य विषय, अध्ययन आदि नहीं जानता वह उसके अध्ययन में प्रवृत्त नहीं हो सकता । अध्ययन में प्रवृत्त होने के लिए सर्वप्रथम उपक्रम अपेक्षित है।
किसी भी ग्रन्थ का अध्ययन करते समय उपोद्घात की क्या अपेक्षा है ? इस प्रश्न का समाधान बृहत्कल्प-भाष्य की वृत्ति में मिलता है-अंधेरे ओरे में रखी हुई वस्तुएं दीपक के प्रकाश में दिखाई देती हैं उसी प्रकार शास्त्र में निहित अर्थ उपोद्घात के द्वारा अभिव्यक्त होता है।
कोई शास्त्र कितना ही विशिष्ट क्यों न हो, उपोद्घात के बिना उसकी उपादेयता प्रमाणित नहीं होती। इस तथ्य को मेघाच्छन्न चन्द्रमा के उदाहरण से स्पष्ट किया है जिस प्रकार मेघ से आच्छादित चन्द्रमा आकाश में नहीं चमकता उसी प्रकार शास्त्र भी उपोद्घात के बिना उपयोगी नहीं बनता।"
२. निक्षेप
व्याख्या का दूसरा द्वार है-निक्षेप । शब्दों में विशेषण के द्वारा प्रतिनियत अर्थ का प्रतिपादन करने की शक्ति निहित करना निक्षेप कहलाता है। निधान, निधि, निक्षेप, न्यास, विरचना, प्रसार, स्थापना ये सब पर्यायवाची हैं। इसके द्वारा उपक्रान्त विषय के प्रस्तुत अर्थ का बोध होता है । विस्तृत जानकारी के लिए द्रष्टव्य है सूत्र ५ का टिप्पण । ३. अनुगम
व्याख्या का तीसरा द्वार है-अनुगम । अस्तित्व, नास्तित्व, द्रव्यमान, क्षेत्र, स्पर्शना, काल आदि अनेक पहलुओं से व्याख्या करना अनुगम है। निक्षेप द्वारा प्रस्तुत विषय की स्थापना होने के बाद उसका सत्, संख्या, क्षेत्र आदि अनेक अधिकारों से अर्थबोध करना।
१. अहाव. पृ. २६ : इहाध्ययनार्थकथनविधिरनुयोगः। २. अमव. प.४०। ३. (क) अहावृ. पृ. २७ ।
(ख) अमवृ. प. ४० । ४. विभा. ९०८ : अकयद्दारमनगरं कएगदारं पि दुक्खसंचारं ।
चउमूलद्दारं पुण सपडिदारं सुहाहिगमं ॥ वही, ९०९ : सामाइयमहपुरमवि अकयद्दारं तहेगदारं वा ।
दुरहिगम, चउदारं सपडिद्दारं सुहाहिगमं ॥ ५. बृभा. १ पृ. २ : अनेन चोपोद्धातेनाभिहितेन सूत्रादयोऽर्था
अभिव्यक्ता भवन्ति, यथा दीपेनाऽपवरके तमसि । उक्तं
वत्तीभवंति दम्वा, दीवेणं अप्पगासे उव्वरए ।
वत्तीभवंति अत्था, उवग्धाएणं तहा सत्थे ॥ उपोद्धातान्निधानमन्तरेण पुनः शास्त्रं स्वतोऽतिविशिष्टमपि न तथाविधमुपादेयतया विराजते, यथा नभसि मेघाच्छन्नश्चन्द्रमाः। उक्तं च-- मेघान्छन्नो यथा चन्द्रो, न राजति नभस्तले ।
उपोद्धातं विना शास्त्रं, न राजति तथाविधम् ।। ६. (क) अहावू. पृ. २७ : निक्षेप: भ्यासः स्थापनेति पर्यायः । (ख) अमव. प. ४० : शास्त्रादेमिस्थापनाविभेदैर्व्यसनं
व्यवस्थापन निक्षेपः।
Jain Education Intemational
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org