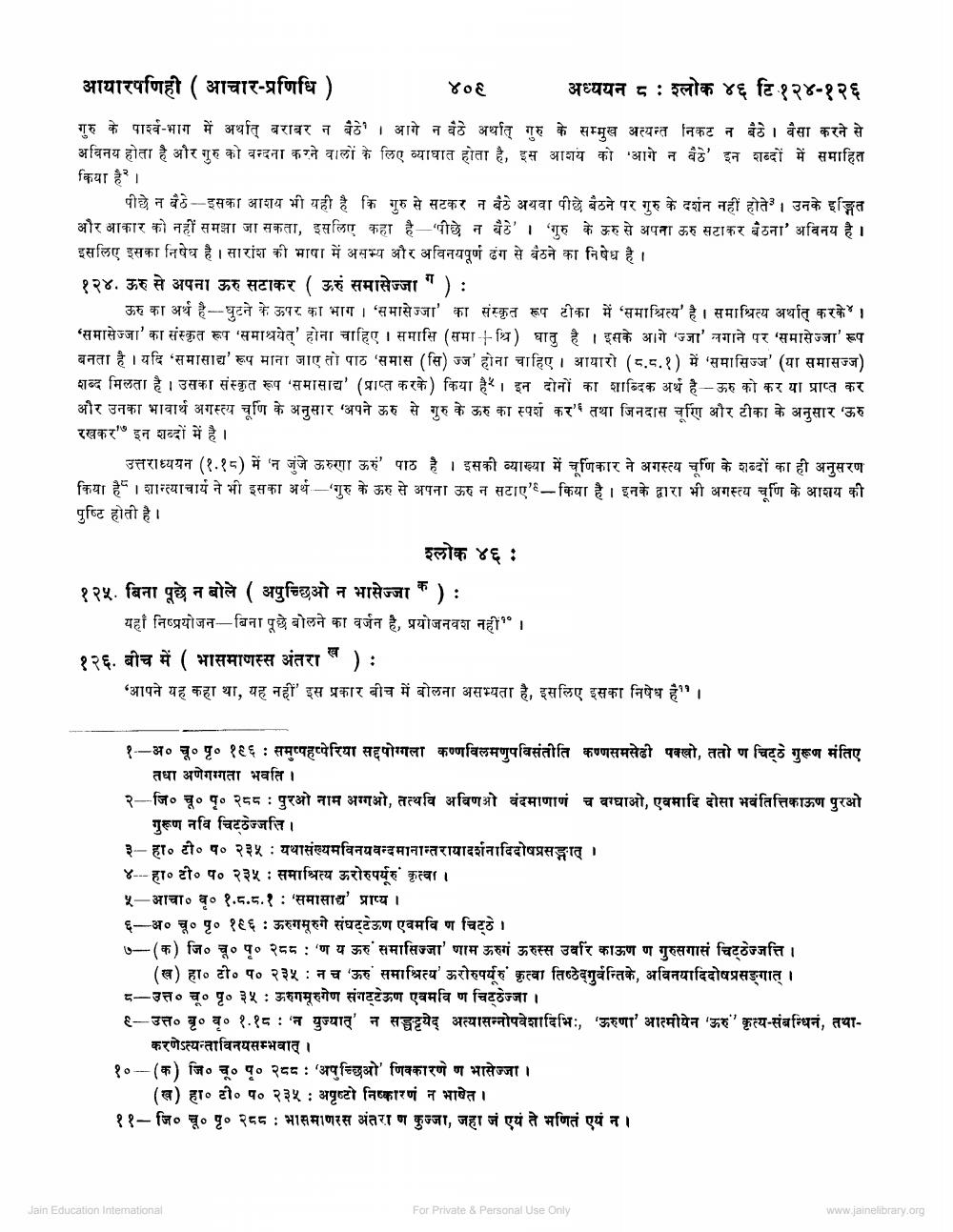________________
४०६
अध्ययन ८ : श्लोक ४६ टि १२४-१२६
आयारपणिही ( आचार-प्रणिधि ) गुरु के पार्श्व-भाग में अर्थात् बराबर न बैठे' । आगे न बैठे अर्थात् गुरु के सम्मुख अत्यन्त निकट न बैठे। वैसा करने से अविनय होता है और गुरु को वन्दना करने वालों के लिए व्याघात होता है, इस आशय को 'आगे न बैठे' इन शब्दों में समाहित किया है।
पीछे न बैठे-इसका आशय भी यही है कि गुरु से सटकर न बैठे अथवा पीछे बैठने पर गुरु के दर्शन नहीं होते। उनके इङ्गित और आकार को नहीं समझा जा सकता, इसलिए कहा है—'पीछे न बैठे' । 'गुरु के ऊरु से अपना ऊरु सटाकर बैठना' अविनय है। इसलिए इसका निषेध है । सारांश की भाषा में असभ्य और अविनयपूर्ण ढंग से बैठने का निषेध है। १२४. ऊरु से अपना ऊरु सटाकर ( ऊरुं समासेज्जा ) :
ऊरु का अर्थ है-घुटने के ऊपर का भाग । 'समासेज्जा' का संस्कृत रूप टीका में 'समाश्रित्य' है। समाश्रित्य अर्थात् करके । 'समासेज्जा' का संस्कृत रूप 'समाश्रयेत्' होना चाहिए । समासि (समा+थि) घातु है । इसके आगे 'ज्जा' लगाने पर 'समासेज्जा' रूप बनता है । यदि 'समासाद्य' रूप माना जाए तो पाठ 'समास (सि) ज्ज' होना चाहिए। आयारो (८.८.१) में 'समासिज्ज' (या समासज्ज) शब्द मिलता है । उसका संस्कृत रूप समासाद्य' (प्राप्त करके) किया है। इन दोनों का शाब्दिक अर्थ है-ऊरु को कर या प्राप्त कर और उनका भावार्थ अगस्त्य चूणि के अनुसार 'अपने ऊरु से गुरु के ऊरु का स्पर्श कर'६ तथा जिनदास चरिण और टीका के अनुसार 'ऊरु रखकर इन शब्दों में है।
उत्तराध्ययन (१.१८) में 'न मुंजे ऊरुणा ऊरुं' पाठ है । इसकी व्याख्या में चूणिकार ने अगस्त्य चूणि के शब्दों का ही अनुसरण किया है । शान्त्याचार्य ने भी इसका अर्थ — 'गुरु के ऊरु से अपना ऊरु न सटाए'-किया है। इनके द्वारा भी अगस्त्य चूणि के आशय की पुष्टि होती है।
श्लोक ४६ : १२५. बिना पूछे न बोले ( अपुच्छिओ न भासेज्जा क ):
यहाँ निष्प्रयोजन—बिना पूछे बोलने का वर्जन है, प्रयोजनवश नहीं । १२६. बीच में ( भासमाणस्स अंतरा ख ) :
'आपने यह कहा था, यह नहीं' इस प्रकार बीच में बोलना असभ्यता है, इसलिए इसका निषेध है।
१-अ० चू० पृ० १६६ : समुप्पहप्पेरिया सद्दपोग्गला कण्णविलमणुपविसंतीति कण्णसमसेढी पक्खो, ततो ण चिठे गुरूण मंतिए
तधा अणेगग्गता भवति । २-जि० चू० पृ० २८८ : पुरओ नाम अग्गओ, तत्थवि अविणओ वंदमाणाणं च वग्घाओ, एवमादि दोसा भवंतित्तिकाऊण पुरओ
गुरूण नवि चिट्ठज्जत्ति। ३-हा० टी०प० २३५ : यथासंख्यमविनयवन्दमानान्तरायादर्शनादिदोषप्रसङ्गात् । ४.--हा० टी० प० २३५ : समाश्रित्य ऊरोरुप'र कृत्वा । ५–आचा. वृ० १.८.८.१ : 'समासाद्य' प्राप्य । ६-अ० चू० पृ० १६६ : ऊरुगमूहगे संघट्टेऊण एवमवि ण चिठे। ७-(क) जि० चू० पृ० २८८ : ‘ण य ऊरुसमासिज्जा' णाम ऊरुगं ऊरुस्स उरि काऊण ण गुरुसगासं चिट्ठज्जत्ति ।
(ख) हा० टी० प० २३५ : न च 'ऊरु समाश्रित्य' ऊरोरुपर्युरुं कृत्वा तिष्ठेद्गुर्वन्तिके, अविनयादिदोषप्रसङ्गात् । ८-उत्त० चू० पृ० ३५ : ऊरुगमूरुगेण संगट्टेऊण एवमवि ण चिट्ठज्जा। ६-उत्त० बृ० वृ० १.१८ : 'न युज्यात्' न सङ्घट्टयेद् अत्यासन्नोपवेशादिभिः, 'ऊरुणा' आत्मीयेन 'ऊरु' कृत्य-संबन्धिनं, तथा
करणेऽत्यन्ताविनयसम्भवात् । १० -(क) जि० चू० पृ० २८८ : 'अपुच्छिओ' णिक्कारणे ण भासेज्जा।
(ख) हा० टी० प० २३५ : अपृष्टो निष्कारणं न भाषेत । ११- जि० चू० पृ० २८८ : भासमाणरस अंतरा ण कुज्जा, जहा जं एयं ते भणितं एयं न।
Jain Education Intemational
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org