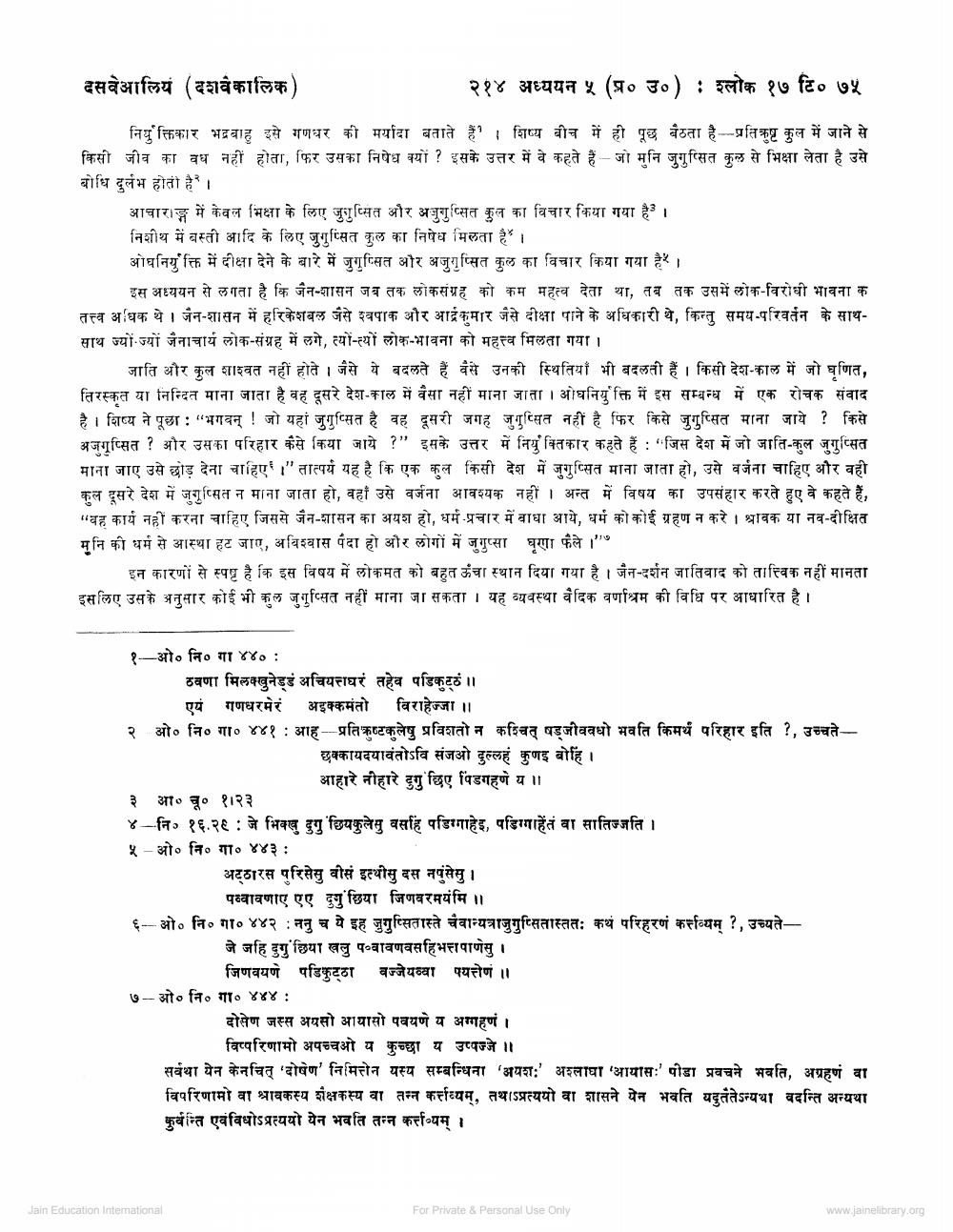________________
दसवेलियं ( दशवेकालिक)
नियुसिकार भद्रवाह इसे गणधर को मर्यादा बताते है
शिष्य बीच में ही पूछ बैठता है-प्रतिकृष्ट कुल में जाने से किसी जीव का वध नहीं होता, फिर उसका निषेध क्यों ? इसके उत्तर में वे कहते हैं- जो मुनि जुगुप्सित कुल से भिक्षा लेता है उसे बोधि दुर्लभ होती है।
२१४ अध्ययन ५ (प्र० उ०) श्लोक १७ टि० ७५
:
आचाराद्ध में केवल भिक्षा के लिए जुगुप्सित और अजुगुप्सित कूल का विचार किया गया है।
निशीथ में बस्ती आदि के लिए जुगुप्सित कुल का निषेध मिलता है ।
ओ नियुक्ति में दीक्षा देने के बारे में जुगुप्सित और अजुगुप्सित कुल का विचार किया गया है।
इस अध्ययन से लगता है कि जैन-शासन जब तक लोकसंग्रह को कम महत्व देता था, तब तक उसमें लोक-विरोधी भावना क तत्व अधिक थे। जैन शासन में हरिकेशनल जैसे दवपाक और आर्द्रकुमार जैसे दीक्षा पाने के अधिकारी थे, किन्तु समय-परिवर्तन के साथसाथ ज्यों-ज्यों जैनाचार्य लोक-संग्रह में लगे, त्यों-त्यों लोक-भावना को महत्त्व मिलता गया ।
1
जाति और कुल शायत नहीं होते। जैसे वे बदलते हैं से उनको स्थितियां भी बदलती है किसी देश काल में जो घृणित, तिरस्कृत या निन्दित माना जाता है वह दूसरे देश काल में वैसा नहीं माना जाता । ओघनियुक्ति में इस सम्बन्ध में एक रोचक संवाद है । शिष्य ने पूछा : “भगवन् ! जो यहां जुगुप्सित है वह दूसरी जगह जुगुप्सित नहीं है फिर किसे जुगुप्सित माना जाये ? किसे अजुगुप्सित ? और उसका परिहार कैसे किया जाये ?" इसके उत्तर में नियुक्तिकार कहते हैं: "जिस देश में जो जाति- कुल जुगुप्सित माना जाए उसे छोड़ देना चाहिए।" तात्पर्य यह है कि एक कुल किसी देश में जुगुप्सित माना जाता हो, उसे वर्जना चाहिए और यही कुल दूसरे देश में जुगुप्सित न माना जाता हो, वहाँ उसे वर्जना आवश्यक नहीं । अन्त में विषय का उपसंहार करते हुए वे कहते हैं, "वह कार्य नहीं करना चाहिए जिससे जैन-शासन का अयश हो, धर्म प्रचार में बाधा आये, धर्म को कोई ग्रहण न करे । श्रावक या नव-दीक्षित मुनि की धर्म से आस्था हट जाए, अविश्वास पैदा हो और लोगों में जुगुप्सा घृणा फैले । ७
इन कारणों से स्पष्ट है कि इस विषय में लोकमत को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। जैन दर्शन जातिवाद को तात्त्विक नहीं मानता इसलिए उसके अनुसार कोई भी कुल जुगुप्सित नहीं माना जा सकता । यह व्यवस्था वैदिक वर्णाश्रम की विधि पर आधारित है ।
१- ओ० नि० गा ४४० :
ठवणा मिलक्युने अनियतधरं सहेब पडिक ।। एवं गणधर मेरं
अहकमतो विराहेजा ||
२ ओ० नि० गा० ४४१ : आह-प्रतिक्रुष्टकुलेषु प्रविशतो न कश्चित् षड्जीववधो भवति किमर्थं परिहार इति ?, उच्चतेछक्कायदयावतोऽवि संजओ दुल्लहं कुणइ बोहि ।
आहारे नीहारे दुगुछिए पिंडगहणे य ॥
३ आ० चू० १।२३
४ - नि० १६.२६ : जे भिक्खु दुगु छियकुलेसु वर्साहं पडिग्गाहेइ, पडिग्गार्हतं वा सातिज्जति ।
५- ओ० नि० गा० ४४३ :
अट्ठारस पुरिसेसु वीसं इत्थीसु दस नपुंसेसु ।
पश्वावणाए एए दुगु छिया जिणवरमयंमि ॥
६-- ओ० नि००४४२ ननु च ये इह जुगुप्सितास्ते चैवान्यगुप्तास्ततः कथं परिहरणं कर्तव्यम् ? उच्यते
जे जहि दुर्गा छिया खलु पश्वावणवसहिभत्तपाणेसु । जिणवयणे पडिकुट्ठा वज्जेयव्वा पयत्तेणं ॥ ७- ओ० नि० गा० ४४४ :
दोसेण जस्स असो आयासो पवयणे य अग्गहणं । विपरिणामो अपञ्चओ य कुच्छा य उप्पज्जे ॥
सर्वथा येन केनचित् 'दोषेण' निमित्तेन यस्य सम्बन्धिना 'अयश:' अश्लाघा 'आयासः' पीडा प्रवचने भवति, अग्रहणं वा विपरिणामो वा श्रावकस्य शैक्षकस्य वा तन्न कर्त्तव्यम्, तथाऽप्रत्ययो वा शासने येन भवति यदुर्ततेऽन्यथा वदन्ति अन्यथा कुर्वन्ति एवंविधोऽप्रत्ययो येन भवति तन्न कर्त्तव्यम् ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org