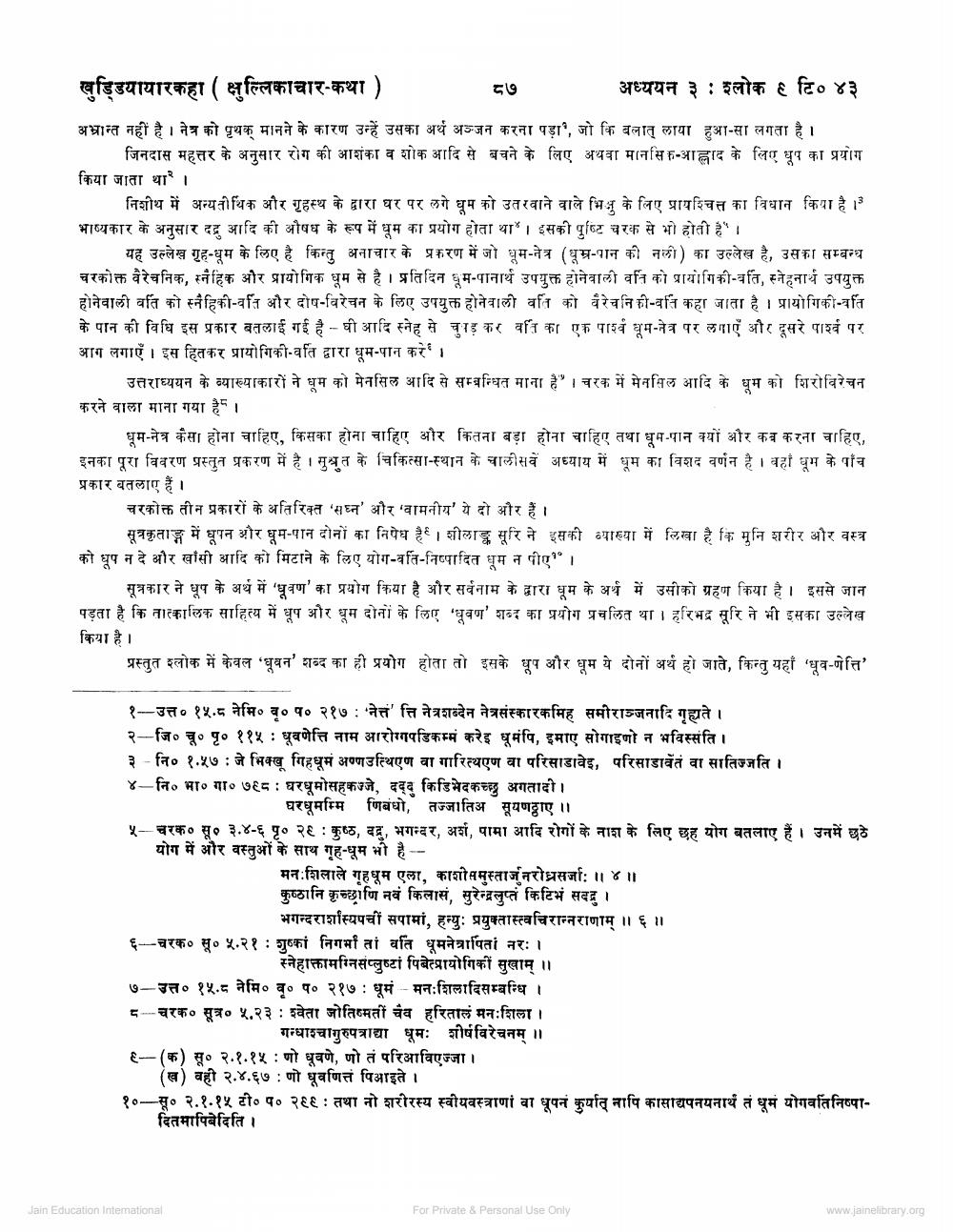________________
खुड्डियायारकहा (क्षुल्लिकाचार-कथा )
८७
अध्ययन ३ : श्लोकह टि०४३ अभ्रान्त नहीं है । नेत्र को पृथक् मानने के कारण उन्हें उसका अर्थ अञ्जन करना पड़ा', जो कि बलात् लाया हुआ-सा लगता है।
जिनदास महत्तर के अनुसार रोग की आशंका व शोक आदि से बचने के लिए अथवा मानसिक-आह्लाद के लिए धूप का प्रयोग किया जाता था।
निशीथ में अन्य तीथिक और गृहस्थ के द्वारा घर पर लगे धूम को उतरवाने वाले भिक्षु के लिए प्रायश्चित्त का विधान किया है।' भाष्यकार के अनुसार दद्रु आदि की औषध के रूप में धूम का प्रयोग होता था। इसकी पुष्टि चरक से भी होती है।
यह उल्लेख गृह-धूम के लिए है किन्तु अनाचार के प्रकरण में जो धूम-नेत्र (धूम्र-पान की नली) का उल्लेख है, उसका सम्बन्ध चरकोक्त वैरेचनिक, स्नैहिक और प्रायोगिक धूम से है । प्रतिदिन धूम-पानार्थ उपयुक्त होनेवाली वर्ति को प्रायोगिकी-वति, स्नेहनार्थ उपयुक्त होनेवाली वर्ति को स्नैहिकी-वति और दोष-विरेचन के लिए उपयुक्त होनेवाली वति को वैरेचनि की-वति कहा जाता है । प्रायोगिकी-वति के पान की विधि इस प्रकार बतलाई गई है - घी आदि स्नेह से चुपड़ कर वति का एक पाश्र्व धूम-नेत्र पर लगाएँ और दूसरे पार्श्व पर आग लगाएँ। इस हितकर प्रायोगिकी-वति द्वारा धूम-पान करें।
___ उत्तराध्ययन के व्याख्याकारों ने धूम को मेनसिल आदि से सम्बन्धित माना हैं" । चरक में मेनसिल आदि के धूम को शिरोविरेचन करने वाला माना गया है।
धूम-नेत्र कैसा होना चाहिए, किसका होना चाहिए और कितना बड़ा होना चाहिए तथा धूम-पान क्यों और कब करना चाहिए, इनका पूरा विवरण प्रस्तुत प्रकरण में है । सुश्रुत के चिकित्सा-स्थान के चालीसवें अध्याय में धूम का विशद वर्णन है। वहाँ धूम के पाँच प्रकार बतलाए हैं।
चरकोक्त तीन प्रकारों के अतिरिक्त सघ्न' और 'वामनीय' ये दो और हैं।
सूत्रकृताङ्ग में धूपन और धूम-पान दोनों का निषेध है । शीलाङ्क सूरि ने इसकी व्याख्या में लिखा है कि मुनि शरीर और वस्त्र को धूप न दे और खाँसी आदि को मिटाने के लिए योग-वति-निष्पादित धूम न पीए ।
सूत्रकार ने धूप के अर्थ में 'धूवण' का प्रयोग किया है और सर्वनाम के द्वारा धूम के अर्थ में उसीको ग्रहण किया है। इससे जान पड़ता है कि तात्कालिक साहित्य में धूप और धूम दोनों के लिए 'धूवण' शब्द का प्रयोग प्रचलित था। हरिभद्र सूरि ने भी इसका उल्लेख किया है।
प्रस्तुत श्लोक में केवल 'धूवन' शब्द का ही प्रयोग होता तो इसके धूप और धूम ये दोनों अर्थ हो जाते, किन्तु यहाँ 'धूव-णेत्ति'
१-उत्त० १५.८ नेमि० वृ० ५० २१७ : नेत्त' त्ति नेत्रशब्देन नेत्रसंस्कारकमिह समीराजनादि गृह्यते । २-जि० चू० पृ० ११५ : धूवणेत्ति नाम आरोग्गपडिकम्म करेइ धूमंपि, इमाए सोगाइणो न भविस्सति । ३ -नि० १.५७ : जे भिक्खू गिहधूम अण्णउत्थिएण वा गारित्थएण वा परिसाडावेइ, परिसाडावेतं वा सातिज्जति । ४-नि० भा० गा० ७६८ : घरधूमोसहकज्जे, ददु किडिभेदकच्छ अगतादी।
घरधूमम्मि णिबंधो, तज्जातिअ सूयणढ़ाए। ५-चरक० सू० ३.४-६ पृ० २६ : कुष्ठ, दद्रु, भगन्दर, अर्श, पामा आदि रोगों के नाश के लिए छह योग बतलाए हैं। उनमें छठे योग में और वस्तुओं के साथ गृह-धूम भी है--
मनःशिलाले गृहधूम एला, काशीसमुस्तार्जुनरोध्रसर्जाः ॥ ४ ॥ कुष्ठानि कृच्छाणि नवं किलासं, सुरेन्द्रलुप्तं किटिभं सदनु ।
भगन्दरास्यिपची सपामां, हन्युः प्रयुक्तास्त्वचिरान्नराणाम् ॥ ६ ॥ ६--चरक० सू०५.२१ : शुष्कां निगरां तां वति धूमनेत्रापितां नरः ।
स्नेहाक्तामग्निसंप्लुष्टां पिबेत्प्रायोगिकी सुखाम् ।। ७-उत्त० १५.८ नेमि० वृ० प० २१७ : धूम-मनःशिलादिसम्बन्धि । --चरक० सूत्र० ५.२३ : श्वेता जोतिष्मती चैव हरितालं मनःशिला ।
गन्धाश्चागुरुपत्राद्या धूमः शीर्ष विरेचनम् ॥ E-(क) सू० २.१.१५ : णो धूवणे, णो तं परिआविएज्जा।
(ख) वही २.४.६७ : णो धूवणित्तं पिआइते।। १०-सू० २.१.१५ टी०५० २६६ : तथा नो शरीरस्य स्वीयवस्त्राणां वा धूपनं कुर्यात् नापि कासाद्यपनयनाथ तं धूम योगवति निष्पा
दितमापिबेदिति।
Jain Education Intemational
For Private & Personal Use Only
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org