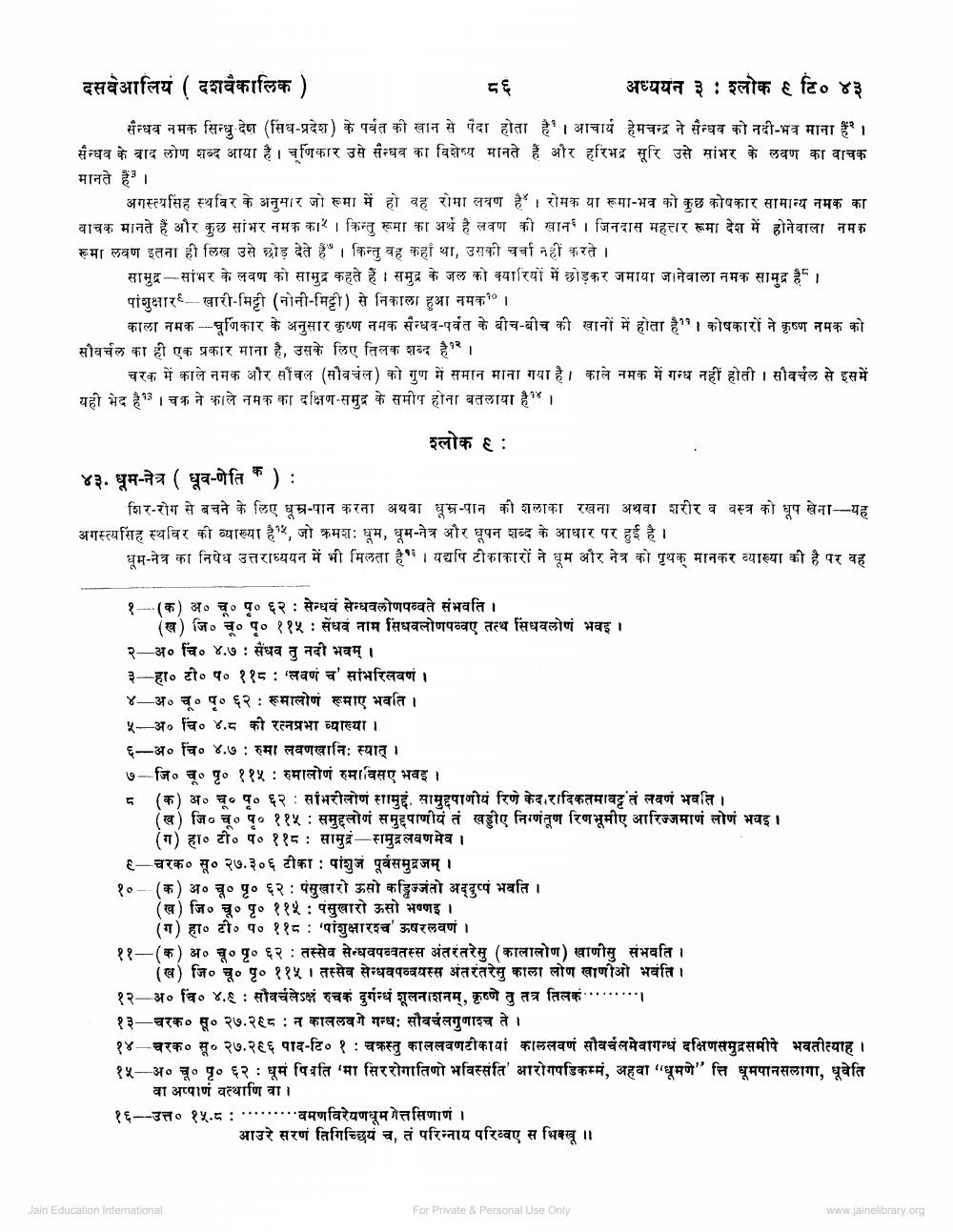________________
दसवेआलियं ( दशवकालिक )
अध्ययन ३ : श्लोक ६ टि० ४३ सैन्धव नमक सिन्धु-देश (सिंध-प्रदेश) के पर्वत की खान से पैदा होता है। आचार्य हेमचन्द्र ने सैन्धव को नदी-भव माना हैं। सैन्धव के बाद लोण शब्द आया है। चणि कार उसे सैन्धव का विशेष्य मानते हैं और हरिभद्र सूरि उसे सांभर के लवण का वाचक मानते हैं।
अगस्त्यसिंह स्थविर के अनुसार जो रूमा में हो वह रोमा लवण है । रोमक या रूमा-भव को कुछ कोषकार सामान्य नमक का वाचक मानते हैं और कुछ सांभर नमक का । किन्तु रूमा का अर्थ है लवण की खान । जिनदास महत्तर रूमा देश में होनेवाला नमक रूमा लवण इतना ही लिख उसे छोड़ देते हैं । किन्तु वह कहाँ था, उसकी चर्चा नहीं करते ।
सामुद्र-सांभर के लवण को सामुद्र कहते हैं । समुद्र के जल को क्यारियों में छोड़कर जमाया जानेवाला नमक सामुद्र है। पांशुक्षार - खारी-मिट्टी (नोनी-मिट्टी) से निकाला हुआ नमक ।
काला नमक --चुणिकार के अनुसार कृष्ण नमक सैन्धव-पर्वत के बीच-बीच की खानों में होता है"। कोषकारों ने कृष्ण नमक को सौवर्चल का ही एक प्रकार माना है, उसके लिए तिलक शब्द है१२ ।
चरक में काले नमक और सौंचल (सौवर्चल) को गुण में समान माना गया है। काले नमक में गन्ध नहीं होती। सौवर्चल से इस में यही भेद है । चक्र ने काले नमक का दक्षिण-समुद्र के समीप होना बतलाया है ।
श्लोकह: ४३. धूम-नेत्र ( धूव-णेति क ) :
शिर-रोग से बचने के लिए धूम्रपान करना अथवा धूम्रपान की शलाका रखना अथवा शरीर व वस्त्र को धूप खेना-यह अगस्त्यसिंह स्थविर की व्याख्या है, जो क्रमश: धूम, धूम-नेत्र और धूपन शब्द के आधार पर हुई है।
धुम-नेत्र का निषेध उत्तराध्ययन में भी मिलता है । यद्यपि टीकाकारों ने धूम और नेत्र को पृथक् मानकर व्याख्या की है पर वह
१--(क) अ० चू० पू०६२: सेन्धवं सेन्धवलोणपन्वते संभवति ।
(ख) जि० चू०प०११५ सेंधवं नाम सिधवलोणपब्वए तत्थ सिंधवलोणं भवइ । २—अ० चि० ४.७ : सैंधव तु नदी भवम् । ३-हा० टी० ५० ११८ : 'लवणं च' सांभरिलवणं । ४–अ० चू० पृ० ६२ : रूमालोणं रूमाए भवति । ५-अ० चि० ४.८ को रत्नप्रभा व्याख्या। ६-अ० चि० ४.७ : रुमा लवणखानि: स्यात् । ७-जि० चू० पृ० ११५ : रुमालोणं रुमाविसए भवइ । ८ (क) अ० ० ० ६२ : सांभरीलोणं सामुई, सामुद्दपाणीयं रिणे केदारादिकतमावट्टतं लवणं भवति ।
(ख) जि० चू० पृ० ११५ : समुद्दलोणं समुद्दपाणीयं तं खड्डीए निग्णंतूण रिणभूमीए आरिज्जमाणं लोणं भवइ ।
(ग) हा० टी० ५० ११८ : सामुद्रं समुद्र लवणमेव । ६–चरक० सू० २७.३०६ टीका : पांशुज पूर्वसमुद्रजम् । १०- (क) अ० चू० पृ० ६२ : पंसुखारो ऊसो कड्डिज्जतो अदुप्पं भवति ।
(ख) जि. चू०पृ०११५ : पंसुखारो ऊसो भण्णइ।
(ग) हा० टी० ५० ११८ : 'पांशुक्षारश्च' ऊषरलवणं । ११–(क) अ० चू० पृ० ६२ : तस्सेव सेन्धवपन्वतस्स अंतरतरेसु (कालालोण) खाणीसु संभवति ।
(ख) जि० चू० पृ० ११५ । तस्सेव सेन्धवपव्वयस्स अंतरंतरेसु काला लोण खाणीओ भवंति । १२–अ० चि० ४.६ : सौवर्चलेऽक्ष रुचकं दुर्गन्धं शूलनाशनम्, कृष्णे तु तत्र तिलक .....। १३—चरक० सू० २७.२६८ : न काललवगे गन्धः सौवर्चलगुणाश्च ते । १४–चरक० सू० २७.२६६ पाद-टि०१ : चक्रस्तु काललवणटीकायां काललवणं सौवर्चलमेवागन्धं दक्षिणसमुद्रसमीपे भवतीत्याह । १५–अ० चू० पृ०६२ : धूमं पिबति 'मा सिररोगातिणो भविस्संति' आरोगपडिकम्म, अहवा "धूमणे" त्ति धूमपानसलागा, धूवेति
वा अप्पाणं वत्थाणि वा। १६--उत्त० १५.८ : .......... वमणविरेयणधूम गेत्तसिणाणं ।
आउरे सरणं तिगिच्छियं च, तं परिन्नाय परिव्वए स भिक्खू ।
अहवालपूनम पास यूमीवर भवानी यह
Jain Education Intemational
For Private & Personal use only
www.jainelibrary.org