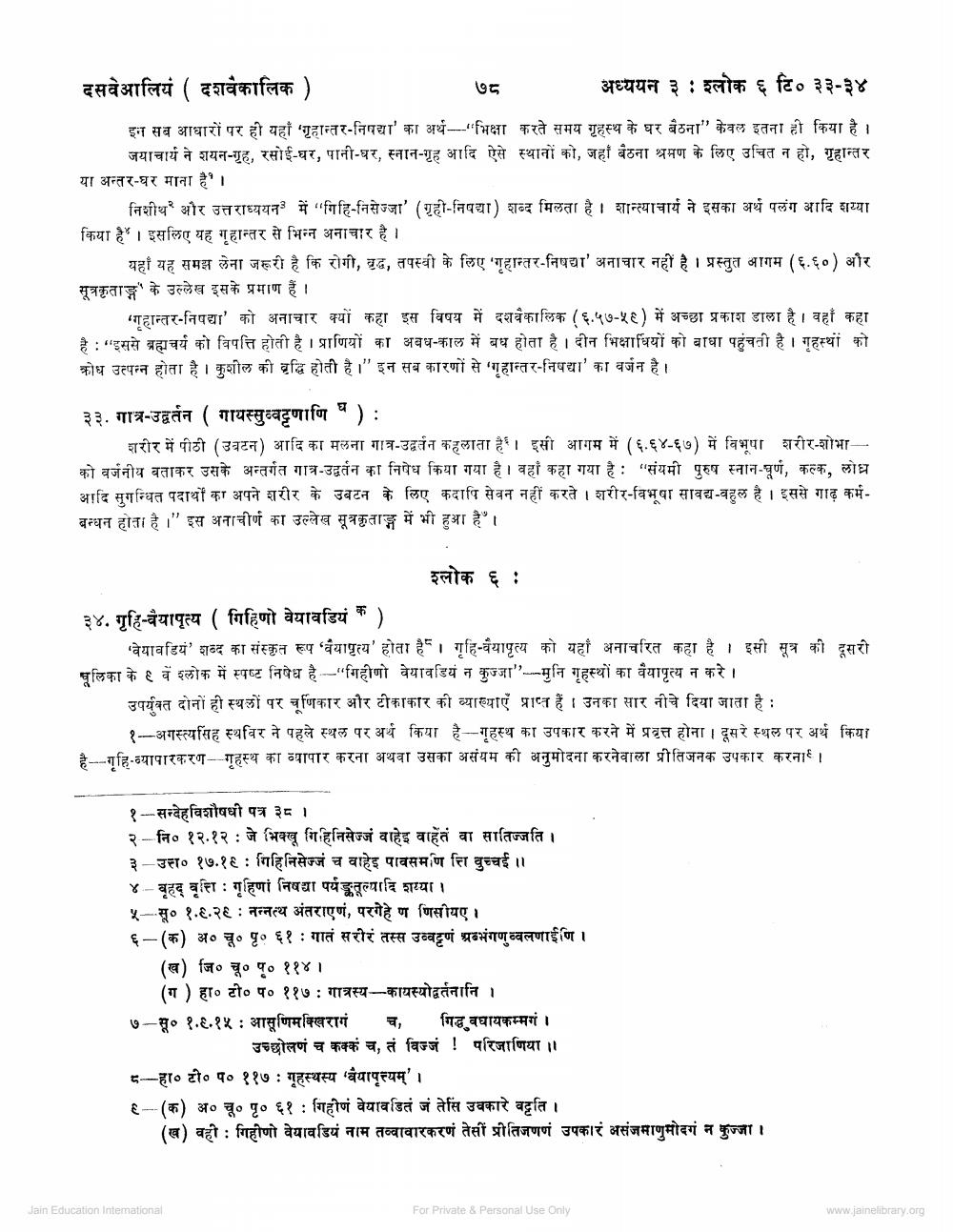________________
दसवेलियं ( दशवैकालिक )
७८
अध्ययन ३ : श्लोक ६ टि० ३३-३४
इन सब आधारों पर ही यहां 'गृहान्तरनिपता' का अर्थ भिक्षा करते समय गृहस्य के पर बैठना केवल इतना ही किया है। जयाचार्य ने शयनगृह, रसोई पर पानी पर स्नानगृह आदि ऐसे स्थानों को, जहाँ बैठना श्रमण के लिए उचित न हो, बृहन्तर या अन्तर-घर माना है' |
निशीथ और उत्तराध्ययन' में "गिहि-निसेज्जा' (गृही- निषद्या) शब्द मिलता है। शान्त्याचार्य ने इसका अर्थ पलंग आदि शय्या किया है। इसलिए यह गृहान्तर से भिन्न अनाचार है ।
उपस्थी के लिए 'गृहान्तर निपया' अनाचार नहीं है। प्रस्तुत आगम (६.६० ) और
यहां यह समझ लेना जरूरी है कि रोगी सूत्रकृताङ्ग" के उल्लेख इसके प्रमाण हैं ।
'गृहान्तर-निया' को अनाचार क्यों कहा इस विषय में दशकालिक (६.५७-५९) में अच्छा प्रकाश डाला है। यहाँ कहा है : "इससे ब्रह्मचर्य को विपत्ति होती है। प्राणियों का अवध-काल में बध होता है। दीन भिक्षाधियों को बाधा पहुंचती है। गृहस्थों को कोष उत्पन्न होता है कुशील की वृद्धि होती है।" इन सब कारणों से 'गृहान्तरनिया का वर्जन है।
३२. गात्र उद्वर्तन ( गायस्वट्टणाणि ध ) :
शरीर में पीठी (उबटन) आदि का मलना गात्र उद्वर्तन कहलाता है। इसी आगम में ( ६.६४-६७ ) में विभूपा शरीर-शोभाको वर्जनीय बताकर उसके अन्तर्गत गात्र उद्वर्तन का निषेध किया गया है । वहाँ कहा गया है : "संयमी पुरुष स्नान चूर्ण, कल्क, लोध्र आदि सुगन्धित पदार्थों का अपने शरीर के उबटन के लिए कदापि सेवन नहीं करते । शरीर-विभूषा सावद्य-बहुल है । इससे गाढ़ कर्मबन्धन होता है।" इस अनाची का उल्लेख षता में भी हुआ है।
श्लोक ६ :
३४. गृहियापृत्य ( गिहिणो वेपावडियं क
)
‘वेयावडियं’ शब्द का संस्कृत रूप ' वैयावृत्य' होता है" । गृहि वैयावृत्य को यहाँ अनाचरित कहा है । इसी सूत्र की दूसरी धूलिका के 8 वें श्लोक में स्पष्ट निषेध है - "गिहीणो वेयावडियं न कुज्जा" मुनि गृहस्थों का व्यापृत्य न करे ।
उपर्युक्त दोनों ही स्थलों पर चूर्णिकार और टीकाकार की व्याख्याएँ प्राप्त हैं। उनका सार नीचे दिया जाता है :
१ - अगस्त्य सिंह स्थविर ने पहले स्थल पर अर्थ किया है- गृहस्थ का उपकार करने में प्रवृत्त होना। दूसरे स्थल पर अर्थ किया - गृहि व्यापारकरण- गृहस्थ का व्यापार करना अथवा उसका असंयम की अनुमोदना करनेवाला प्रीतिजनक उपकार करना ।
१- सन्देहविषयी पत्र ३८
२० १२.१२
जे
वाहेद वाह वा सान्निति ।
३ - उ० १७.१६ : गिहिनिसेज्जं च वाहेइ पावसमणिति वच्चई || ४तिगृहिणां विद्या पर्यादि या।
५०] १.८.२९ नन्नत्य अंतराएवं परगेण भितीय
६ (क) ५० ० ० ६१ गातं सरीरं तस्य उबट्टणं मंगलगाई।
(ख) जि० ० पू० ११४ ॥
fo
(ग) हा० टी० प० ११७ : गात्रस्य - कायस्योद्वर्तनानि ।
७ - सू० १.६.१५ : आसूणिमक्खिरागं
च, fra aarai |
उच्छोलणं च कक्कं च तं विज्जं ! परिजाणिया ||
- हा० टी० ए० ११० गृहस्वस्य वैधास्यम्'
E -- (क) अ० चू० पृ० ६१: गिहीणं वेयावडितं जं तेसि उबकारे वट्टति ।
(ख) यही गिट्टीणो वैवावहियं नाम तव्यावारकरणं तेसी प्रीतिजगणं उपकार अजमाणुमोदन कुज्जा ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org