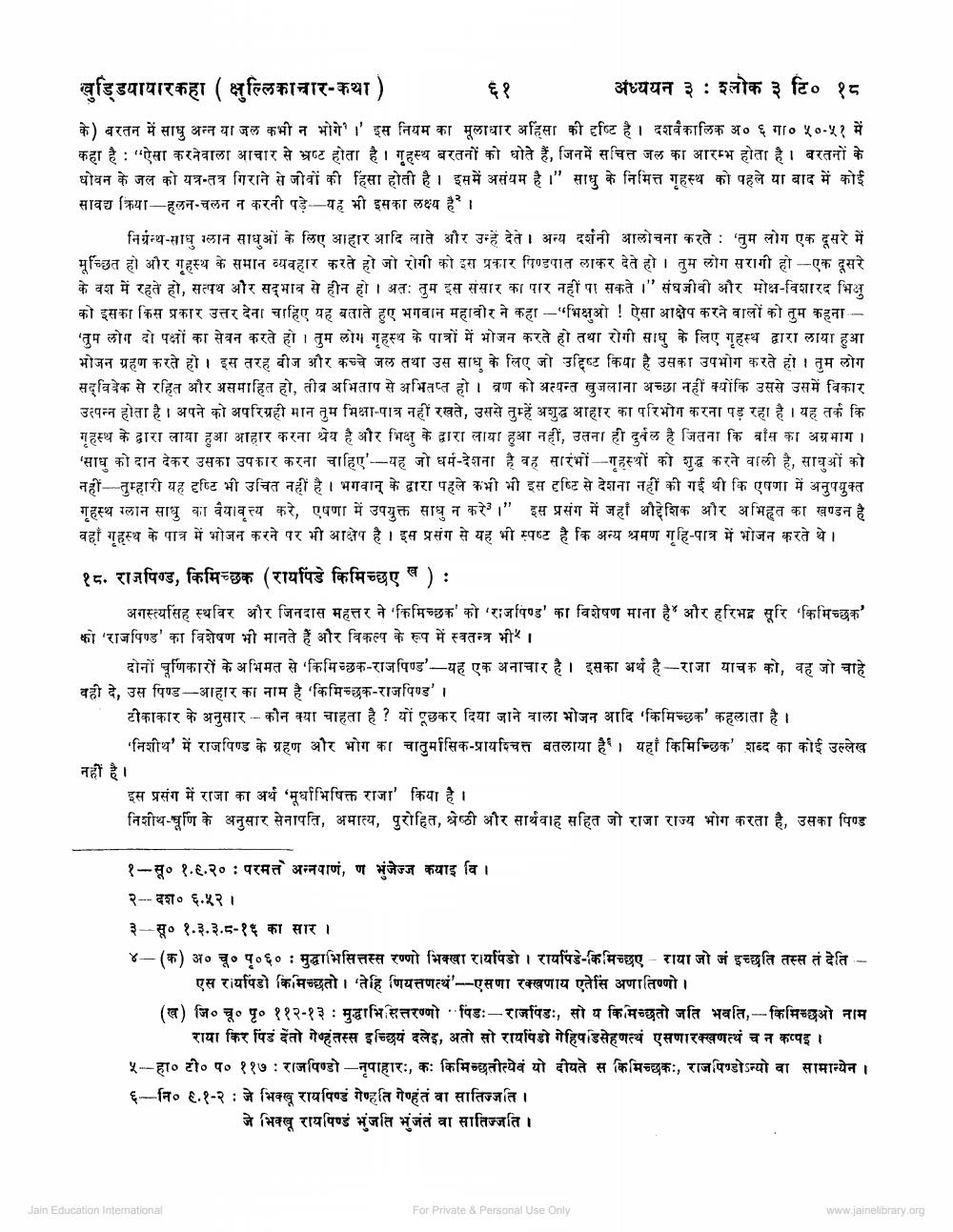________________
६१
खुड्डियायारकहा ( क्षुल्लिकाचार-कथा)
अध्ययन ३ : श्लोक ३ टि० १८ के) बरतन में साधु अन्न या जल कभी न भोगे'।' इस नियम का मूलाधार अहिंसा की दृष्टि है। दशकालिक अ० ६ गा० ५०-५१ में कहा है : “ऐसा करनेवाला आचार से भ्रष्ट होता है । गृहस्थ बरतनों को धोते हैं, जिनमें सचित्त जल का आरम्भ होता है। बरतनों के धोवन के जल को यत्र-तत्र गिराने से जीवों की हिंसा होती है। इसमें असंयम है।" साधु के निमित्त गृहस्थ को पहले या बाद में कोई सावध क्रिया-हलन-चलन न करनी पड़े—यह भी इसका लक्ष्य है ।
निर्ग्रन्थ-साधु ग्लान साधुओं के लिए आहार आदि लाते और उन्हें देते। अन्य दर्शनी आलोचना करते : 'तुम लोग एक दूसरे में मूच्छित हो और गृहस्थ के समान व्यवहार करते हो जो रोगी को इस प्रकार पिण्डपात लाकर देते हो। तुम लोग सरागी हो -एक दूसरे के वश में रहते हो, सत्पथ और सद्भाव से हीन हो । अत: तुम इस संसार का पार नहीं पा सकते ।" संघजीवी और मोक्ष-विशारद भिक्षु को इसका किस प्रकार उत्तर देना चाहिए यह बताते हुए भगवान महावीर ने कहा - "भिक्षुओ ! ऐसा आक्षेप करने वालों को तुम कहना'तुम लोग दो पक्षों का सेवन करते हो । तुम लोग गृहस्थ के पात्रों में भोजन करते हो तथा रोगी साधु के लिए गृहस्थ द्वारा लाया हुआ भोजन ग्रहण करते हो। इस तरह बीज और कच्चे जल तथा उस साधु के लिए जो उद्दिष्ट किया है उसका उपभोग करते हो । तुम लोग सद्विवेक से रहित और असमाहित हो, तीव्र अभिताप से अभितप्त हो। व्रण को अत्यन्त खुजलाना अच्छा नहीं क्योंकि उससे उसमें विकार उत्पन्न होता है। अपने को अपरिग्रही मान तुम भिक्षा-पात्र नहीं रखते, उससे तुम्हें अशुद्ध आहार का परिभोग करना पड़ रहा है । यह तर्क कि गृहस्थ के द्वारा लाया हुआ आहार करना श्रेय है और भिक्षु के द्वारा लाया हुआ नहीं, उतना ही दुर्वल है जितना कि बाँस का अग्रभाग । 'साधु को दान देकर उसका उपकार करना चाहिए'यह जो धर्म-देशना है वह सारंभों--गृहस्थों को शुद्ध करने वाली है, साधुओं को नहीं-तुम्हारी यह दृष्टि भी उचित नहीं है । भगवान् के द्वारा पहले कभी भी इस दृष्टि से देशना नहीं की गई थी कि एषणा में अनुपयुक्त गृहस्थ ग्लान साधु का वैयावृत्त्य करे, एषणा में उपयुक्त साधु न करे।" इस प्रसंग में जहाँ औद्देशिक और अभिहत का खण्डन है वहाँ गृहस्थ के पात्र में भोजन करने पर भी आक्षेप है । इस प्रसंग से यह भी स्पष्ट है कि अन्य श्रमण गृहि-पात्र में भोजन करते थे।
१८. राजपिण्ड, किमिच्छक (रायपिंडे किमिच्छए ख ) :
अगस्त्यसिंह स्थविर और जिनदास महत्तर ने किमिच्छक' को राजपिण्ड' का विशेषण माना है और हरिभद्र सूरि किमिच्छक' को 'राजपिण्ड' का विशेषण भी मानते हैं और विकल्प के रूप में स्वतन्त्र भी।
दोनों चूर्णिकारों के अभिमत से 'किमिच्छक-राजपिण्ड'–यह एक अनाचार है। इसका अर्थ है-राजा याचक को, वह जो चाहे वही दे, उस पिण्ड ---आहार का नाम है 'किमिच्छक-राजपिण्ड' ।
टीकाकार के अनुसार - कौन क्या चाहता है ? यों पूछकर दिया जाने वाला भोजन आदि 'किमिच्छक' कहलाता है।
'निशीथ' में राजपिण्ड के ग्रहण और भोग का चातुर्मासिक-प्रायश्चित्त बतलाया है। यहाँ किमिच्छिक' शब्द का कोई उल्लेख नहीं है।
इस प्रसंग में राजा का अर्थ 'मूर्धाभिषिक्त राजा' किया है। निशीथ-घूणि के अनुसार सेनापति, अमात्य, पुरोहित, श्रेष्ठी और सार्थवाह सहित जो राजा राज्य भोग करता है, उसका पिण्ड
१-सू० १.६.२० : परमत्त अन्नपाणं, ण भुजेज्ज कयाइ वि । २-- दश० ६.५२ । ३-सू० १.३.३.-१६ का सार । ४- (क) अ० चू० पृ०६० : मुद्धाभिसित्तस्स रण्णो भिक्खा रायपिंडो। रायपिंडे-किमिच्छए- राया जो जं इच्छति तस्स तं देति -
____एस रायपिंडो किमिच्छतो। 'तेहि णियत्तणत्थं'--एसणा रक्खणाय एतेसि अणातिण्णो। (ख) जि० चू० पृ० ११२-१३ : मुद्धाभिसित्तरण्णो पिड- राजपिडः, सो य किमिच्छतो जति भवति,-किमिच्छओ नाम
राया किर पिंडं देतो गेण्हतस्स इच्छियं दलेइ, अतो सो रायपिडो गेहिपडिसेहणत्यं एसणारक्खणत्थं च न कप्पइ । ५.--हा० टी० प० ११७ : राजपिण्डो–नपाहारः, कः किमिच्छतीत्येवं यो दीयते स किमिच्छकः, राजपिण्डोऽन्यो वा सामान्येन । ६...--नि० ६.१-२ : जे भिक्खू रायपिण्डं गेहति गेण्हतं वा सातिज्जति ।
जे भिक्खू रायपिण्डं भुंजति भुंजतं वा सातिज्जति ।
Jain Education Intemational
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org