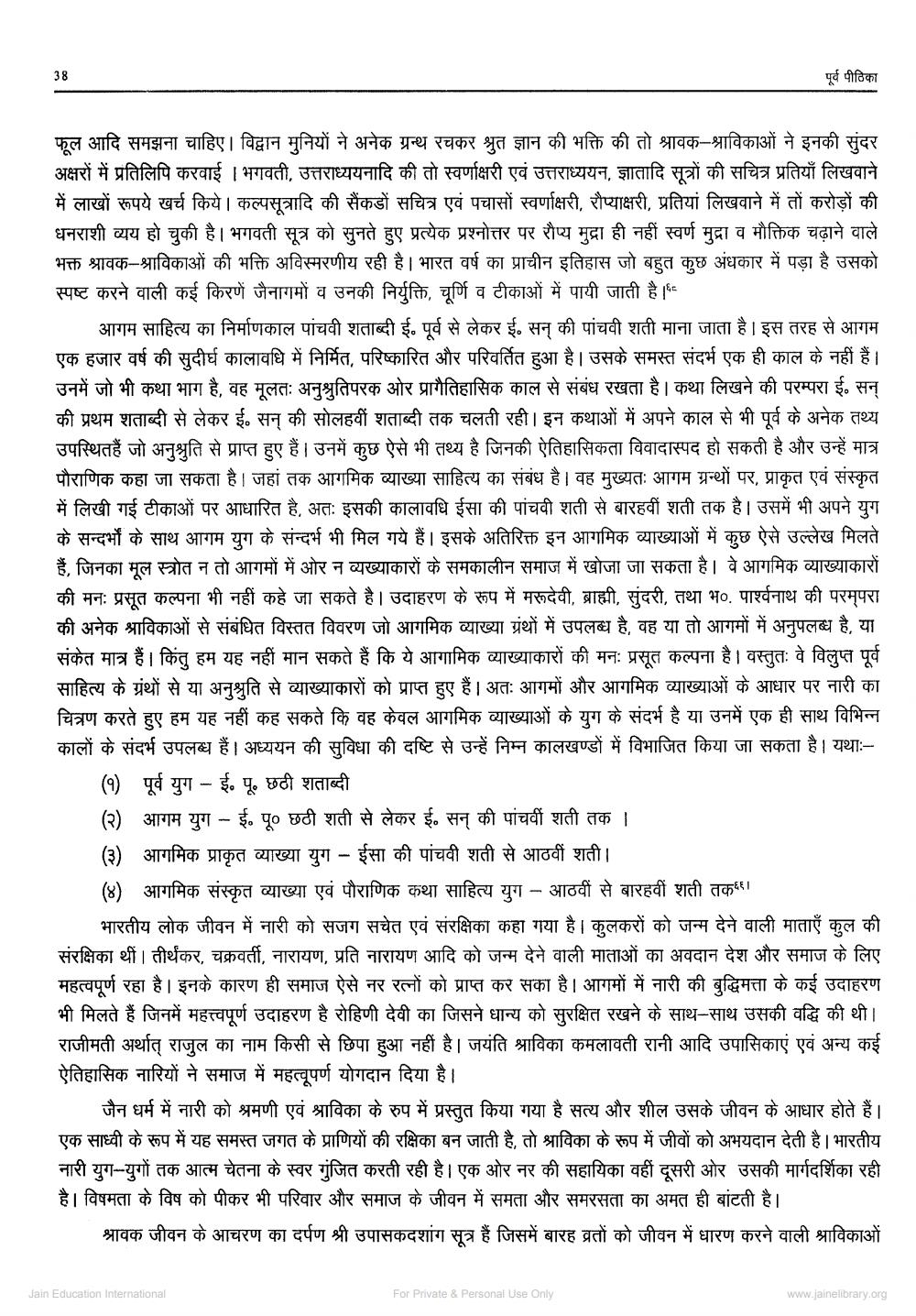________________
पूर्व पीठिका
फूल आदि समझना चाहिए। विद्वान मुनियों ने अनेक ग्रन्थ रचकर श्रुत ज्ञान की भक्ति की तो श्रावक-श्राविकाओं ने इनकी सुंदर अक्षरों में प्रतिलिपि करवाई । भगवती, उत्तराध्ययनादि की तो स्वर्णाक्षरी एवं उत्तराध्ययन, ज्ञातादि सूत्रों की सचित्र प्रतियाँ लिखवाने में लाखों रूपये खर्च किये। कल्पसूत्रादि की सैंकडों सचित्र एवं पचासों स्वर्णाक्षरी, रौप्याक्षरी, प्रतियां लिखवाने में तों करोड़ों की धनराशी व्यय हो चुकी है। भगवती सूत्र को सुनते हुए प्रत्येक प्रश्नोत्तर पर रौप्य मुद्रा ही नहीं स्वर्ण मुद्रा व मौक्तिक चढ़ाने वाले भक्त श्रावक-श्राविकाओं की भक्ति अविस्मरणीय रही है। भारत वर्ष का प्राचीन इतिहास जो बहुत कुछ अंधकार में पड़ा है उसको स्पष्ट करने वाली कई किरणें जैनागमों व उनकी नियुक्ति, चूर्णि व टीकाओं में पायी जाती है।
___ आगम साहित्य का निर्माणकाल पांचवी शताब्दी ई. पूर्व से लेकर ई. सन् की पांचवी शती माना जाता है। इस तरह से आगम एक हजार वर्ष की सुदीर्घ कालावधि में निर्मित, परिष्कारित और परिवर्तित हुआ है। उसके समस्त संदर्भ एक ही काल के नहीं हैं। उनमें जो भी कथा भाग है, वह मूलतः अनुश्रुतिपरक ओर प्रागैतिहासिक काल से संबंध रखता है। कथा लिखने की परम्परा ई. सन् की प्रथम शताब्दी से लेकर ई. सन् की सोलहवीं शताब्दी तक चलती रही। इन कथाओं में अपने काल से भी पूर्व के अनेक तथ्य उपस्थितहैं जो अनुश्रुति से प्राप्त हुए हैं। उनमें कुछ ऐसे भी तथ्य है जिनकी ऐतिहासिकता विवादास्पद हो सकती है और उन्हें मात्र पौराणिक कहा जा सकता है। जहां तक आगमिक व्याख्या साहित्य का संबंध है। वह मुख्यतः आगम ग्रन्थों पर, प्राकृत एवं संस्कृत में लिखी गई टीकाओं पर आधारित है, अतः इसकी कालावधि ईसा की पांचवी शती से बारहवीं शती तक है। उसमें भी अपने युग के सन्दर्भो के साथ आगम युग के संन्दर्भ भी मिल गये हैं। इसके अतिरिक्त इन आगमिक व्याख्याओं में कुछ ऐसे उल्लेख मिलते हैं, जिनका मूल स्त्रोत न तो आगमों में ओर न व्यख्याकारों के समकालीन समाज में खोजा जा सकता है। वे आगमिक व्याख्याकारों की मनः प्रसूत कल्पना भी नहीं कहे जा सकते है। उदाहरण के रूप में मरूदेवी, ब्राह्मी, संदरी, तथा भ०. पार्श्वनाथ की परमपरा की अनेक श्राविकाओं से संबंधित विस्तत विवरण जो आगमिक व्याख्या ग्रंथों में उपलब्ध है, वह या तो आगमों में अनुपलब्ध है, या संकेत मात्र हैं। किंतु हम यह नहीं मान सकते हैं कि ये आगामिक व्याख्याकारों की मनः प्रसूत कल्पना है। वस्तुतः वे विलुप्त पूर्व साहित्य के ग्रंथों से या अनुश्रुति से व्याख्याकारों को प्राप्त हुए हैं। अतः आगमों और आगमिक व्याख्याओं के आधार पर नारी का चित्रण करते हुए हम यह नहीं कह सकते कि वह केवल आगमिक व्याख्याओं के युग के संदर्भ है या उनमें एक ही साथ विभिन्न कालों के संदर्भ उपलब्ध हैं। अध्ययन की सुविधा की दष्टि से उन्हें निम्न कालखण्डों में विभाजित किया जा सकता है। यथा:
(१) पूर्व युग - ई. पू. छठी शताब्दी (२) आगम युग - ई. पू० छठी शती से लेकर ई. सन् की पांचवीं शती तक । (३) आगमिक प्राकृत व्याख्या युग - ईसा की पांचवी शती से आठवीं शती। (४) आगमिक संस्कृत व्याख्या एवं पौराणिक कथा साहित्य युग - आठवीं से बारहवीं शती तक।
भारतीय लोक जीवन में नारी को सजग सचेत एवं संरक्षिका कहा गया है। कुलकरों को जन्म देने वाली माताएँ कुल की संरक्षिका थीं। तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, प्रति नारायण आदि को जन्म देने वाली माताओं का अवदान देश और समाज के लिए महत्वपूर्ण रहा है। इनके कारण ही समाज ऐसे नर रत्नों को प्राप्त कर सका है। आगमों में नारी की बुद्धिमत्ता के कई उदाहरण भी मिलते हैं जिनमें महत्त्वपूर्ण उदाहरण है रोहिणी देवी का जिसने धान्य को सुरक्षित रखने के साथ-साथ उसकी वद्धि की थी। राजीमती अर्थात् राजुल का नाम किसी से छिपा हुआ नहीं है। जयंति श्राविका कमलावती रानी आदि उपासिकाएं एवं अन्य कई ऐतिहासिक नारियों ने समाज में महत्वूपर्ण योगदान दिया है।
जैन धर्म में नारी को श्रमणी एवं श्राविका के रुप में प्रस्तुत किया गया है सत्य और शील उसके जीवन के आधार होते हैं। एक साध्वी के रूप में यह समस्त जगत के प्राणियों की रक्षिका बन जाती है, तो श्राविका के रूप में जीवों को अभयदान देती है। भारतीय नारी युग-युगों तक आत्म चेतना के स्वर गुंजित करती रही है। एक ओर नर की सहायिका वहीं दूसरी ओर उसकी मार्गदर्शिका रही है। विषमता के विष को पीकर भी परिवार और समाज के जीवन में समता और समरसता का अमत ही बांटती है।
श्रावक जीवन के आचरण का दर्पण श्री उपासकदशांग सूत्र हैं जिसमें बारह व्रतों को जीवन में धारण करने वाली श्राविकाओं
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org