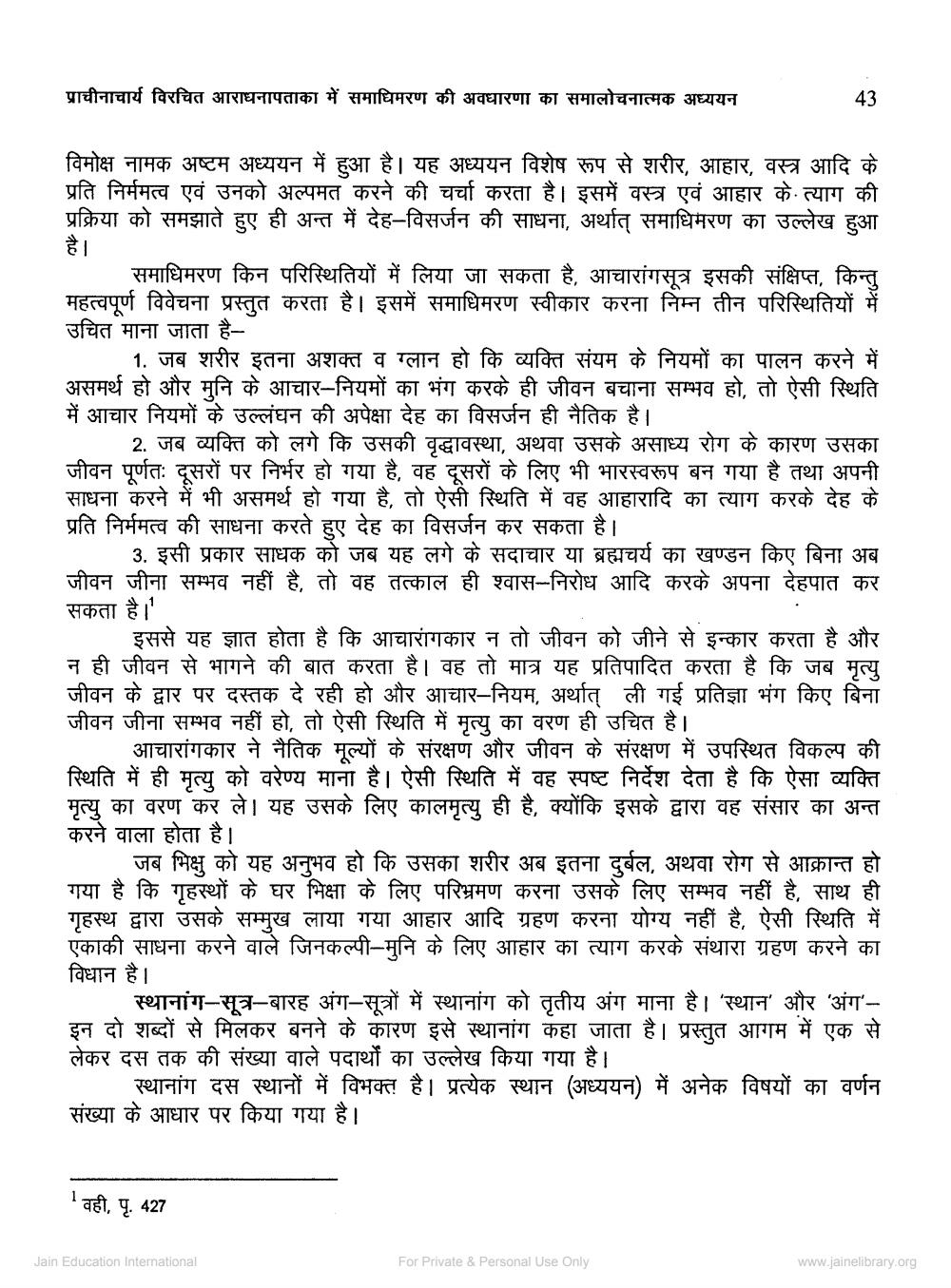________________
प्राचीनाचार्य विरचित आराधनापताका में समाधिमरण की अवधारणा का समालोचनात्मक अध्ययन
43
विमोक्ष नामक अष्टम अध्ययन में हुआ है। यह अध्ययन विशेष रूप से शरीर, आहार, वस्त्र आदि के प्रति निर्ममत्व एवं उनको अल्पमत करने की चर्चा करता है। इसमें वस्त्र एवं आहार के त्याग की प्रक्रिया को समझाते हुए ही अन्त में देह-विसर्जन की साधना, अर्थात् समाधिमरण का उल्लेख हुआ
है।
समाधिमरण किन परिस्थितियों में लिया जा सकता है, आचारांगसूत्र इसकी संक्षिप्त, किन्तु महत्वपूर्ण विवेचना प्रस्तुत करता है। इसमें समाधिमरण स्वीकार करना निम्न तीन परिस्थितियों में उचित माना जाता है
1. जब शरीर इतना अशक्त व ग्लान हो कि व्यक्ति संयम के नियमों का पालन करने में असमर्थ हो और मुनि के आचार-नियमों का भंग करके ही जीवन बचाना सम्भव हो, तो ऐसी स्थिति में आचार नियमों के उल्लंघन की अपेक्षा देह का विसर्जन ही नैतिक है।
2. जब व्यक्ति को लगे कि उसकी वृद्धावस्था, अथवा उसके असाध्य रोग के कारण उसका जीवन पूर्णतः दूसरों पर निर्भर हो गया है, वह दूसरों के लिए भी भारस्वरूप बन गया है तथा अपनी साधना करने में भी असमर्थ हो गया है, तो ऐसी स्थिति में वह आहारादि का त्याग करके देह के प्रति निर्ममत्व की साधना करते हुए देह का विसर्जन कर सकता है।
3. इसी प्रकार साधक को जब यह लगे के सदाचार या ब्रह्मचर्य का खण्डन किए बिना अब जीवन जीना सम्भव नहीं है, तो वह तत्काल ही श्वास-निरोध आदि करके अपना देहपात कर सकता है।
इससे यह ज्ञात होता है कि आचारांगकार न तो जीवन को जीने से इन्कार करता है और न ही जीवन से भागने की बात करता है। वह तो मात्र यह प्रतिपादित करता है कि जब मृत्यु जीवन के द्वार पर दस्तक दे रही हो और आचार-नियम, अर्थात् ली गई प्रतिज्ञा भंग किए बिना जीवन जीना सम्भव नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में मृत्यु का वरण ही उचित है।
आचारांगकार ने नैतिक मूल्यों के संरक्षण और जीवन के संरक्षण में उपस्थित विकल्प की स्थिति में ही मृत्यु को वरेण्य माना है। ऐसी स्थिति में वह स्पष्ट निर्देश देता है कि ऐसा व्यक्ति मृत्यु का वरण कर ले। यह उसके लिए कालमृत्यु ही है, क्योंकि इसके द्वारा वह संसार का अन्त करने वाला होता है।
जब भिक्षु को यह अनुभव हो कि उसका शरीर अब इतना दुर्बल, अथवा रोग से आक्रान्त हो गया है कि गृहस्थों के घर भिक्षा के लिए परिभ्रमण करना उसके लिए सम्भव नहीं है, साथ ही गृहस्थ द्वारा उसके सम्मुख लाया गया आहार आदि ग्रहण करना योग्य नहीं है, ऐसी स्थिति में एकाकी साधना करने वाले जिनकल्पी-मुनि के लिए आहार का त्याग करके संथारा ग्रहण करने का विधान है।
स्थानांग-सूत्र-बारह अंग-सूत्रों में स्थानांग को तृतीय अंग माना है। 'स्थान' और 'अंग'इन दो शब्दों से मिलकर बनने के कारण इसे स्थानांग कहा जाता है। प्रस्तुत आगम में एक से लेकर दस तक की संख्या वाले पदार्थों का उल्लेख किया गया है।
स्थानांग दस स्थानों में विभक्त है। प्रत्येक स्थान (अध्ययन) में अनेक विषयों का वर्णन संख्या के आधार पर किया गया है।
1वही, पृ. 427
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org