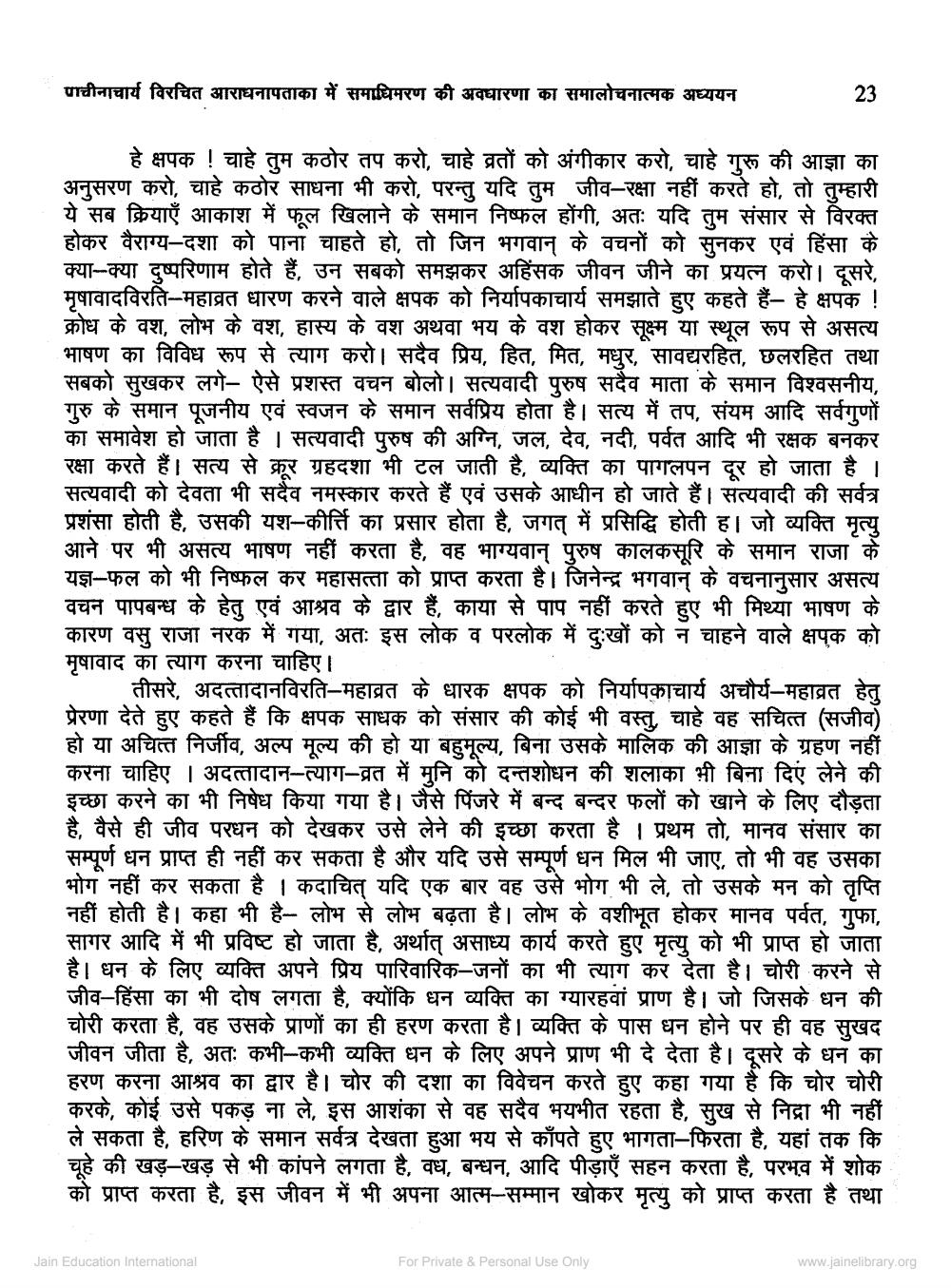________________
प्राचीनाचार्य विरचित आराधनापताका में समाधिमरण की अवधारणा का समालोचनात्मक अध्ययन
हे क्षपक ! चाहे तुम कठोर तप करो, चाहे व्रतों को अंगीकार करो, चाहे गुरु की आज्ञा का अनुसरण करो, चाहे कठोर साधना भी करो, परन्तु यदि तुम जीव-रक्षा नहीं करते हो, तो तुम्हारी ये सब क्रियाएँ आकाश में फूल खिलाने के समान निष्फल होंगी, अतः यदि तुम संसार से विरक्त होकर वैराग्य- दशा को पाना चाहते हो, तो जिन भगवान् के वचनों को सुनकर एवं हिंसा के क्या-क्या दुष्परिणाम होते हैं, उन सबको समझकर अहिंसक जीवन जीने का प्रयत्न करो। दूसरे, मृषावादविरति - महाव्रत धारण करने वाले क्षपक को निर्यापकाचार्य समझाते हुए कहते हैं- हे क्षपक ! क्रोध के वश, लोभ के वश, हास्य के वश अथवा भय के वश होकर सूक्ष्म या स्थूल रूप से असत्य भाषण का विविध रूप से त्याग करो। सदैव प्रिय हित, मित, मधुर, सावद्यरहित, छलरहित तथा सबको सुखकर लगे- ऐसे प्रशस्त वचन बोलो। सत्यवादी पुरुष सदैव माता के समान विश्वसनीय, गुरु के समान पूजनीय एवं स्वजन के समान सर्वप्रिय होता है । सत्य में तप, संयम आदि सर्वगुणों का समावेश हो जाता है । सत्यवादी पुरुष की अग्नि, जल, देव, नदी, पर्वत आदि भी रक्षक बनकर रक्षा करते हैं। सत्य से क्रूर ग्रहदशा भी टल जाती है, व्यक्ति का पागलपन दूर हो जाता है । सत्यवादी को देवता भी सदैव नमस्कार करते हैं एवं उसके आधीन हो जाते हैं। सत्यवादी की सर्वत्र प्रशंसा होती है, उसकी यश-कीर्ति का प्रसार होता है, जगत् में प्रसिद्धि होती ह। जो व्यक्ति मृत्यु आने पर भी असत्य भाषण नहीं करता है, वह भाग्यवान् पुरुष कालकसूरि के समान राजा के यज्ञ - फल को भी निष्फल कर महासत्ता को प्राप्त करता है। जिनेन्द्र भगवान् के वचनानुसार असत्य वचन पापबन्ध के हेतु एवं आश्रव के द्वार हैं, काया से पाप नहीं करते हुए भी मिथ्या भाषण के कारण वसु राजा नरक में गया, अतः इस लोक व परलोक में दुःखों को न चाहने वाले क्षपक को मृषावाद का त्याग करना चाहिए।
23
तीसरे, अदत्तादानविरति - महाव्रत के धारक क्षपक को निर्यापकाचार्य अचौर्य - महाव्रत हेतु प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि क्षपक साधक को संसार की कोई भी वस्तु, चाहे वह सचित्त (सजीव ) हो या अचित्त निर्जीव, अल्प मूल्य की हो या बहुमूल्य, बिना उसके मालिक की आज्ञा के ग्रहण नहीं करना चाहिए । अदत्तादान - त्याग - व्रत में मुनि को दन्तशोधन की शलाका भी बिना दिएं लेने की इच्छा करने का भी निषेध किया गया है। जैसे पिंजरे में बन्द बन्दर फलों को खाने के लिए दौड़ता है, वैसे ही जीव परधन को देखकर उसे लेने की इच्छा करता है । प्रथम तो, मानव संसार का सम्पूर्ण धन प्राप्त ही नहीं कर सकता है और यदि उसे सम्पूर्ण धन मिल भी जाए, तो भी वह उसका भोग नहीं कर सकता है । कदाचित् यदि एक बार वह उसे भोग भी ले, तो उसके मन को तृप्ति नहीं होती है। कहा भी है- लोभ से लोभ बढ़ता है। लोभ के वशीभूत होकर मानव पर्वत, गुफा, सागर आदि में भी प्रविष्ट हो जाता है, अर्थात् असाध्य कार्य करते हुए मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है। धन के लिए व्यक्ति अपने प्रिय पारिवारिक - जनों का भी त्याग कर देता है। चोरी करने से जीव - हिंसा का भी दोष लगता है, क्योंकि धन व्यक्ति का ग्यारहवां प्राण है। जो जिसके धन की चोरी करता है, वह उसके प्राणों का ही हरण करता है। व्यक्ति के पास धन होने पर ही वह सुखद जीवन जीता है, अतः कभी-कभी व्यक्ति धन के लिए अपने प्राण भी दे देता है। दूसरे के धन का हरण करना आश्रव का द्वार है। चोर की दशा का विवेचन करते हुए कहा गया है कि चोर चोरी करके, कोई उसे पकड़ ना ले, इस आशंका से वह सदैव भयभीत रहता है, सुख से निद्रा भी नहीं ले सकता है, हरिण के समान सर्वत्र देखता हुआ भय से काँपते हुए भागता फिरता है, यहां तक कि चूहे की खड़खड़ से भी कांपने लगता है, वध, बन्धन, आदि पीड़ाएँ सहन करता है, परभव में शोक को प्राप्त करता है, इस जीवन में भी अपना आत्म-सम्मान खोकर मृत्यु को प्राप्त करता है तथा
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org