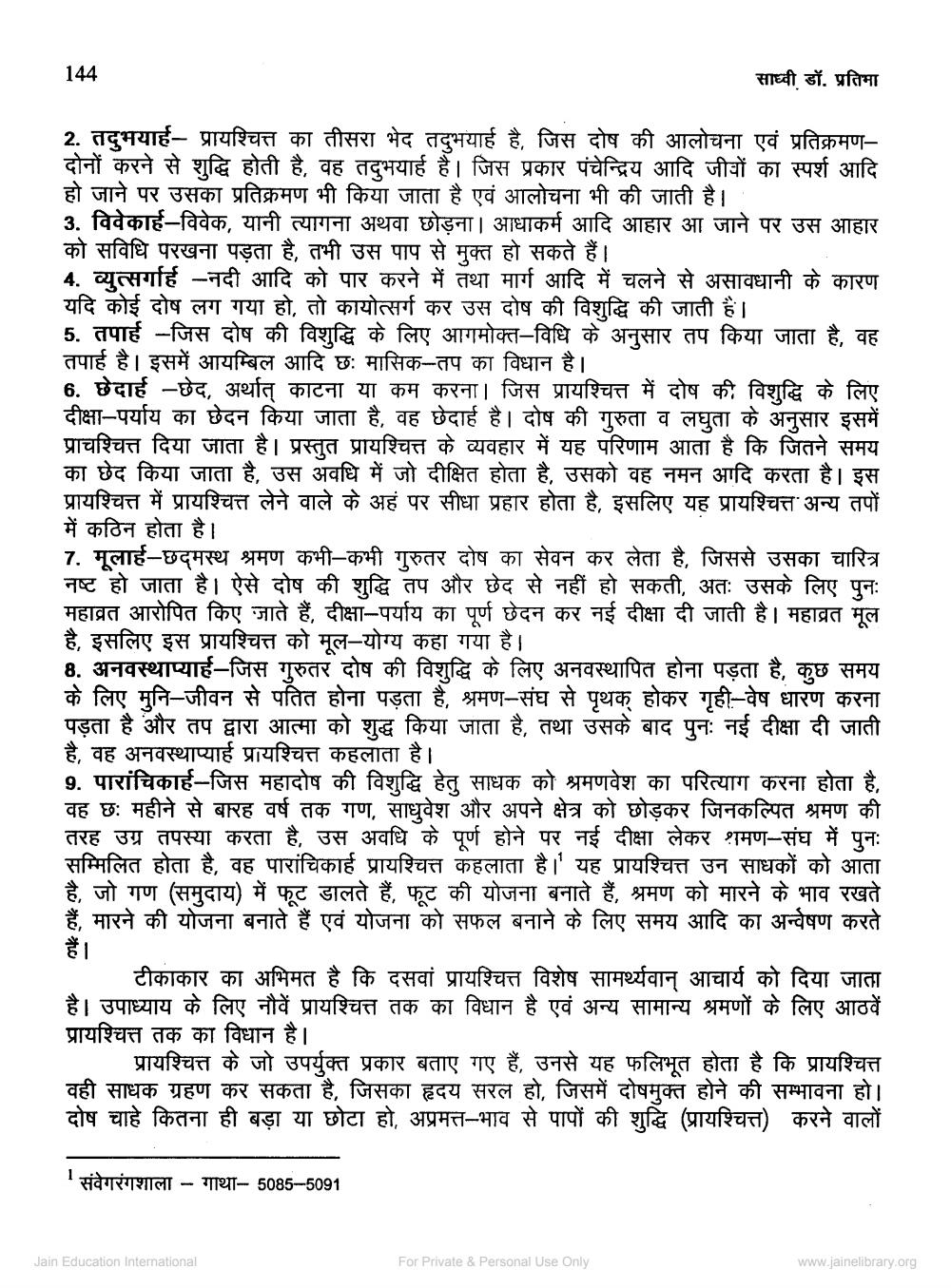________________
144
साध्वी डॉ. प्रतिभा
र इसमें
2. तदुभयाह- प्रायश्चित्त का तीसरा भेद तदुभयाह है, जिस दोष की आलोचना एवं प्रतिक्रमणदोनों करने से शुद्धि होती है, वह तदुभयाह है। जिस प्रकार पंचेन्द्रिय आदि जीवों का स्पर्श आदि हो जाने पर उसका प्रतिक्रमण भी किया जाता है एवं आलोचना भी की जाती है। 3. विवेकाह-विवेक, यानी त्यागना अथवा छोड़ना। आधाकर्म आदि आहार आ जाने पर उस आहार को सविधि परखना पड़ता है, तभी उस पाप से मुक्त हो सकते हैं। 4. व्युत्सर्गार्ह -नदी आदि को पार करने में तथा मार्ग आदि में चलने से असावधानी के कारण यदि कोई दोष लग गया हो, तो कायोत्सर्ग कर उस दोष की विशुद्धि की जाती है। 5. तपार्ह -जिस दोष की विशुद्धि के लिए आगमोक्त-विधि के अनुसार तप किया जाता है, वह तपार्ह है। इसमें आयम्बिल आदि छ: मासिक-तप का विधान है। 6. छेदाह -छेद, अर्थात् काटना या कम करना। जिस प्रायश्चित्त में दोष की विशुद्धि के लिए दीक्षा-पर्याय का छेदन किया जाता है, वह छेदाह है। दोष की गरुता व लघता के अ प्राचश्चित्त दिया जाता है। प्रस्तुत प्रायश्चित्त के व्यवहार में यह परिणाम आता है कि जितने समय का छेद किया जाता है, उस अवधि में जो दीक्षित होता है, उसको वह नमन आदि करता है। इस प्रायश्चित्त में प्रायश्चित्त लेने वाले के अहं पर सीधा प्रहार होता है, इसलिए यह प्रायश्चित्त अन्य तपों में कठिन होता है। 7. मूलार्ह-छद्मस्थ श्रमण कभी-कभी गुरुतर दोष का सेवन कर लेता है, जिससे उसका चारित्र
| ऐसे दोष की शुद्धि तप और छेद से नहीं हो सकती, अतः उसके लिए पुनः महाव्रत आरोपित किए जाते हैं, दीक्षा-पर्याय का पूर्ण छेदन कर नई दीक्षा दी जाती है। महाव्रत मूल है, इसलिए इस प्रायश्चित्त को मूल-योग्य कहा गया है। 8. अनवस्थाप्यारी-जिस गुरुतर दोष की विशुद्धि के लिए अनवस्थापित होना पड़ता है, कुछ समय के लिए मुनि-जीवन से पतित होना पड़ता है, श्रमण-संघ से पृथक् होकर गृही-वेष धारण करना पड़ता है और तप द्वारा आत्मा को शुद्ध किया जाता है, तथा उसके बाद पुनः नई दीक्षा दी जाती है, वह अनवस्थाप्याई प्रायश्चित्त कहलाता है। 9. पारांचिकार्ह-जिस महादोष की विशुद्धि हेतु साधक को श्रमणवेश का परित्याग करना होता है, वह छ: महीने से बारह वर्ष तक गण, साधुवेश और अपने क्षेत्र को छोड़कर जिनकल्पित श्रमण की तरह उग्र तपस्या करता है, उस अवधि के पूर्ण होने पर नई दीक्षा लेकर शमण-संघ में पुनः सम्मिलित होता है, वह पारांचिकार्ह प्रायश्चित्त कहलाता है। यह प्रायश्चित्त उन साधकों को आता है, जो गण (समुदाय) में फूट डालते हैं, फूट की योजना बनाते हैं, श्रमण को मारने के भाव रखते हैं, मारने की योजना बनाते हैं एवं योजना को सफल बनाने के लिए समय आदि का अन्वेषण करते
टीकाकार का अभिमत है कि दसवां प्रायश्चित्त विशेष सामर्थ्यवान् आचार्य को दिया जाता है। उपाध्याय के लिए नौवें प्रायश्चित्त तक का विधान है एवं अन्य सामान्य श्रमणों के लिए आठवें प्रायश्चित्त तक का विधान है।
प्रायश्चित्त के जो उपर्युक्त प्रकार बताए गए हैं, उनसे यह फलिभूत होता है कि प्रायश्चित्त वही साधक ग्रहण कर सकता है, जिसका हृदय सरल हो, जिसमें दोषमुक्त होने की सम्भावना हो। दोष चाहे कितना ही बड़ा या छोटा हो, अप्रमत्त-भाव से पापों की शुद्धि (प्रायश्चित्त) करने वालों
संवेगरंगशाला - गाथा-5085-5091
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org