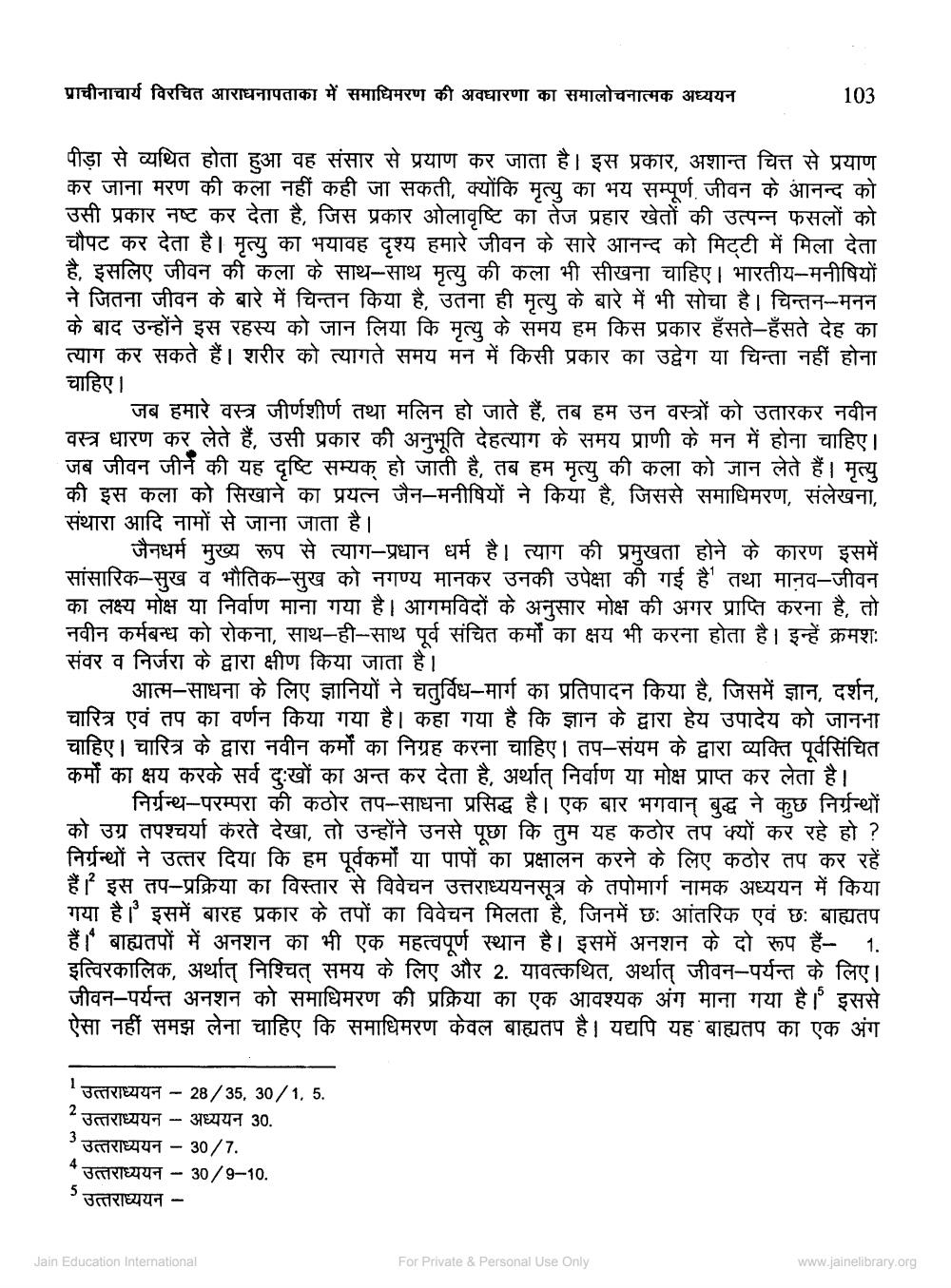________________
प्राचीनाचार्य विरचित आराधनापताका में समाधिमरण की अवधारणा का समालोचनात्मक अध्ययन
103
पीड़ा से व्यथित होता हुआ वह संसार से प्रयाण कर जाता है। इस प्रकार, अशान्त चित्त से प्रयाण कर जाना मरण की कला नहीं कही जा सकती, क्योंकि मृत्यु का भय सम्पूर्ण जीवन के आनन्द को उसी प्रकार नष्ट कर देता है, जिस प्रकार ओलावृष्टि का तेज प्रहार खेतों की उत्पन्न फसलों को चौपट कर देता है। मृत्यु का भयावह दृश्य हमारे जीवन के सारे आनन्द को मिट्टी में मिला देता है, इसलिए जीवन की कला के साथ-साथ मृत्यु की कला भी सीखना चाहिए। भारतीय-मनीषियों ने जितना जीवन के बारे में चिन्तन किया है, उतना ही मृत्यु के बारे में भी सोचा है। चिन्तन-मनन के बाद उन्होंने इस रहस्य को जान लिया कि मृत्यु के समय हम किस प्रकार हँसते-हँसते देह का त्याग कर सकते हैं। शरीर को त्यागते समय मन में किसी प्रकार का उद्वेग या चिन्ता नहीं होना चाहिए।
जब हमारे वस्त्र जीर्णशीर्ण तथा मलिन हो जाते हैं, तब हम उन वस्त्रों को उतारकर नवीन वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार की अनुभूति देहत्याग के समय प्राणी के मन में होना चाहिए। जब जीवन जीने की यह दृष्टि सम्यक हो जाती है, तब हम मृत्यु की कला को जान लेते हैं। मृत्यु की इस कला को सिखाने का प्रयत्न जैन-मनीषियों ने किया है, जिससे समाधिमरण, संलेखना, संथारा आदि नामों से जाना जाता है।
जैनधर्म मुख्य रूप से त्याग-प्रधान धर्म है। त्याग की प्रमुखता होने के कारण इसमें सांसारिक-सुख व भौतिक-सुख को नगण्य मानकर उनकी उपेक्षा की गई है तथा मानव-जीवन का लक्ष्य मोक्ष या निर्वाण माना गया है। आगमविदों के अनुसार मोक्ष की अगर प्राप्ति करना है, तो नवीन कर्मबन्ध को रोकना, साथ-ही-साथ पूर्व संचित कर्मों का क्षय भी करना होता है। इन्हें क्रमशः संवर व निर्जरा के द्वारा क्षीण किया जाता है।
आत्म-साधना के लिए ज्ञानियों ने चतुर्विध-मार्ग का प्रतिपादन किया है, जिसमें ज्ञान, दर्शन, चारित्र एवं तप का वर्णन किया गया है। कहा गया है कि ज्ञान के द्वारा हेय उपादेय को जानना चाहिए। चारित्र के द्वारा नवीन कर्मों का निग्रह करना चाहिए। तप-संयम के द्वारा व्यक्ति पूर्वसिंचित कर्मों का क्षय करके सर्व दुःखों का अन्त कर देता है, अर्थात् निर्वाण या मोक्ष प्राप्त कर लेता है।
निर्ग्रन्थ-परम्परा की कठोर तप-साधना प्रसिद्ध है। एक बार भगवान् बुद्ध ने कुछ निर्ग्रन्थों को उग्र तपश्चर्या करते देखा, तो उन्होंने उनसे पूछा कि तुम यह कठोर तप क्यों कर रहे हो ? निर्ग्रन्थों ने उत्तर दिया कि हम पूर्वकर्मों या पापों का प्रक्षालन करने के लिए कठोर तप कर रहें हैं। इस तप-प्रक्रिया का विस्तार से विवेचन उत्तराध्ययनसूत्र के तपोमार्ग नामक अध्ययन में किया गया है। इसमें बारह प्रकार के तपों का विवेचन मिलता है, जिनमें छ: आंतरिक एवं छ: बाह्यतप हैं। बाह्यतपों में अनशन का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें अनशन के दो रूप हैं- 1. इत्विरकालिक, अर्थात् निश्चित् समय के लिए और 2. यावत्कथित, अर्थात् जीवन-पर्यन्त के लिए। जीवन-पर्यन्त अनशन को समाधिमरण की प्रक्रिया का एक आवश्यक अंग माना गया है। इससे ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि समाधिमरण केवल बाह्यतप है। यद्यपि यह बाह्यतप का एक अंग
'उत्तराध्ययन - 28/35, 30/1, 5. उत्तराध्ययन - अध्ययन 30. उत्तराध्ययन - 30/7.
उत्तराध्ययन - 30/9-10. 5 उत्तराध्ययन -
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org