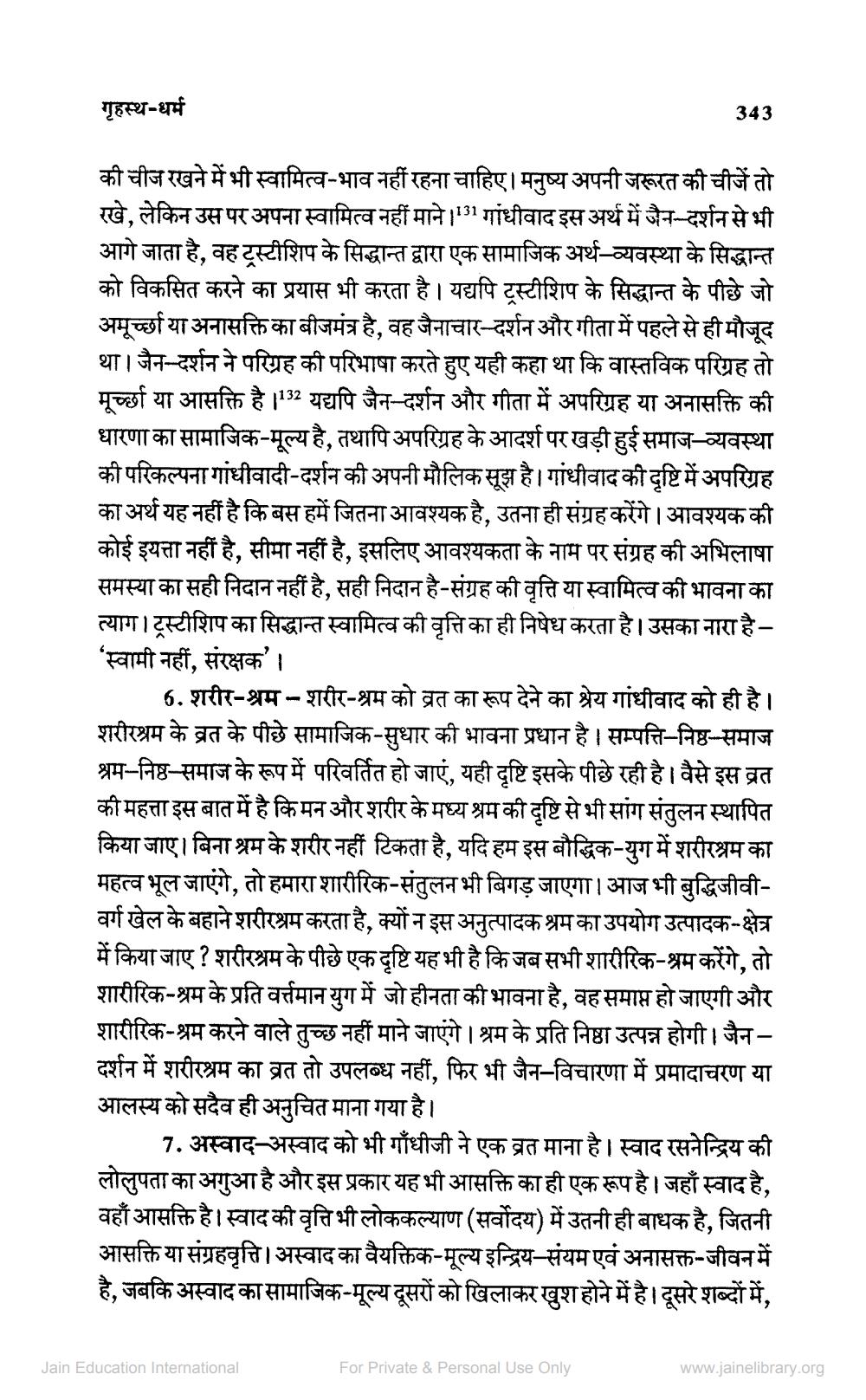________________
गृहस्थ-धर्म
की चीज रखने में भी स्वामित्व-भाव नहीं रहना चाहिए। मनुष्य अपनी जरूरत की चीजें तो रखे, लेकिन उस पर अपना स्वामित्व नहीं माने। 131 गांधीवाद इस अर्थ में जैन-दर्शन से भी आगे जाता है, वह ट्रस्टीशिप के सिद्धान्त द्वारा एक सामाजिक अर्थ-व्यवस्था के सिद्धान्त को विकसित करने का प्रयास भी करता है । यद्यपि ट्रस्टीशिप के सिद्धान्त के पीछे जो अमूर्च्छा या अनासक्ति का बीजमंत्र है, वह जैनाचार - दर्शन और गीता में पहले से ही मौजूद था। जैन दर्शन ने परिग्रह की परिभाषा करते हुए यही कहा था कि वास्तविक परिग्रह तो मूर्च्छा या आसक्ति है । 132 यद्यपि जैन - दर्शन और गीता में अपरिग्रह या अनासक्ति की धारणा का सामाजिक मूल्य है, तथापि अपरिग्रह के आदर्श पर खड़ी हुई समाज - व्यवस्था की परिकल्पना गांधीवादी दर्शन की अपनी मौलिक सूझ है। गांधीवाद की दृष्टि में अपरिग्रह
अर्थ यह नहीं है कि बस हमें जितना आवश्यक है, उतना ही संग्रह करेंगे। आवश्यक की कोई इत्ता नहीं है, सीमा नहीं है, इसलिए आवश्यकता के नाम पर संग्रह की अभिलाषा समस्या का सही निदान नहीं है, सही निदान है - संग्रह की वृत्ति या स्वामित्व की भावना का त्याग | ट्रस्टीशिप का सिद्धान्त स्वामित्व की वृत्ति का ही निषेध करता है। उसका नारा है'स्वामी नहीं, संरक्षक' ।
-
-
उ-समाज
6. शरीर - श्रम - शरीर श्रम को व्रत का रूप देने का श्रेय गांधीवाद को ही है । शरीरश्रम के व्रत के पीछे सामाजिक सुधार की भावना प्रधान है। सम्पत्ति-निष्ठ-स श्रम-निष्ठ8-समाज के रूप में परिवर्तित हो जाएं, यही दृष्टि इसके पीछे रही है। वैसे इस व्रत की महत्ता इस बात में है कि मन और शरीर के मध्य श्रम की दृष्टि से भी सांग संतुलन स्थापित किया जाए। बिना श्रम के शरीर नहीं टिकता है, यदि हम इस बौद्धिक- युग में शरीरश्रम का महत्व भूल जाएंगे, तो हमारा शारीरिक संतुलन भी बिगड़ जाएगा। आज भी बुद्धिजीवीवर्ग खेल के बहाने शरीरश्रम करता है, क्यों न इस अनुत्पादक श्रम का उपयोग उत्पादक- - क्षेत्र में किया जाए ? शरीरश्रम के पीछे एक दृष्टि यह भी है कि जब सभी शारीरिक श्रम करेंगे, तो शारीरिक श्रम के प्रति वर्त्तमान युग में जो हीनता की भावना है, वह समाप्त हो जाएगी और शारीरिक श्रम करने वाले तुच्छ नहीं माने जाएंगे। श्रम के प्रति निष्ठा उत्पन्न होगी। जैन - दर्शन में शरीरश्रम का व्रत तो उपलब्ध नहीं, फिर भी जैन- विचारणा में प्रमादाचरण या आलस्य को सदैव ही अनुचित माना गया है।
-
7. अस्वाद - अस्वाद को भी गाँधीजी ने एक व्रत माना है । स्वाद रसनेन्द्रिय की लोलुपताका अगुआ है और इस प्रकार यह भी आसक्ति का ही एक रूप है। जहाँ स्वाद है, वहाँ आसक्ति है। स्वाद की वृत्ति भी लोककल्याण (सर्वोदय) में उतनी ही बाधक है, जितनी आसक्ति या संग्रहवृत्ति । अस्वाद का वैयक्तिक- मूल्य इन्द्रिय-संयम एवं अनासक्त - जीवन में है, जबकि अस्वाद का सामाजिक मूल्य दूसरों को खिलाकर खुश होने में है। दूसरे शब्दों में,
Jain Education International
-
343
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org