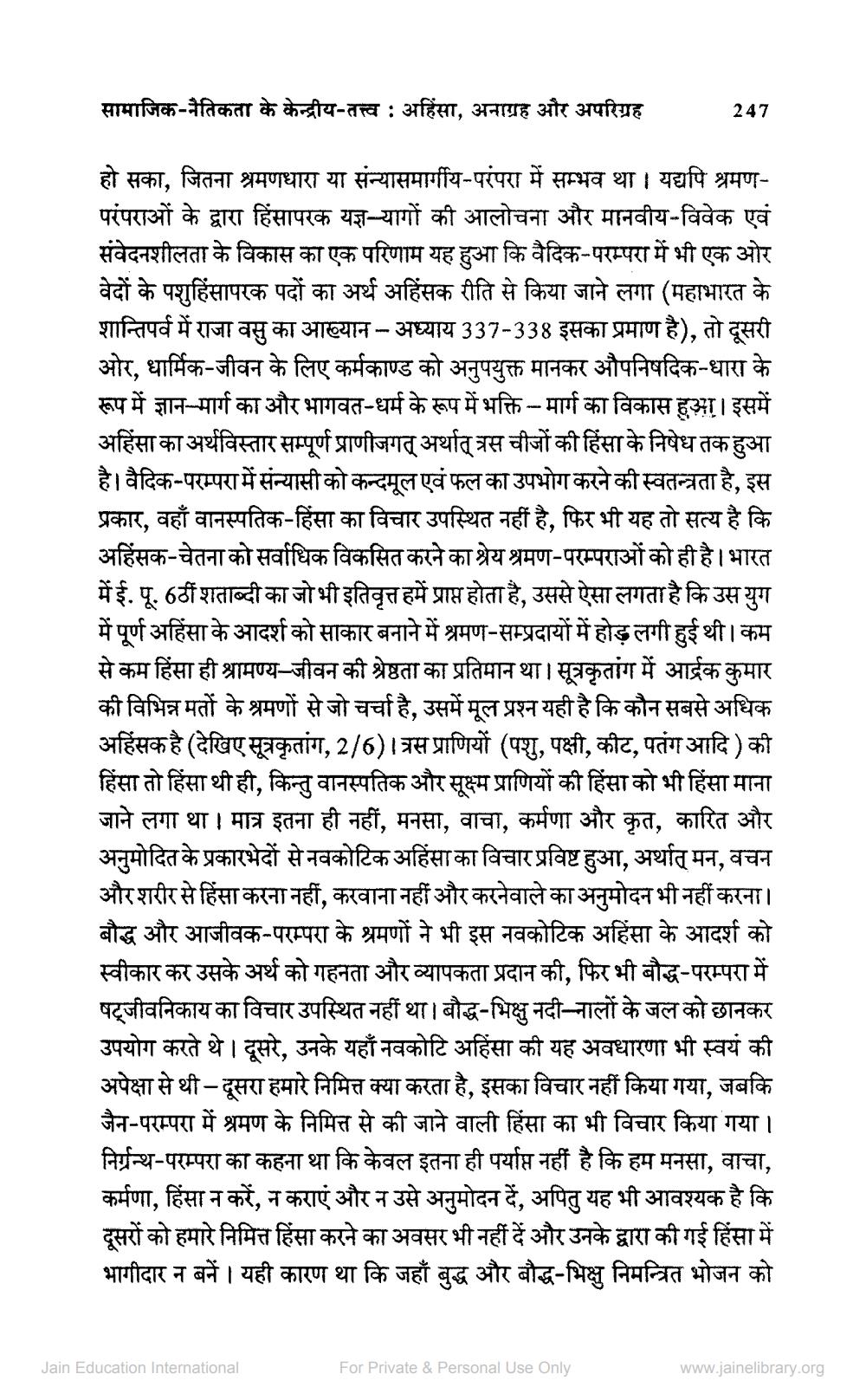________________
सामाजिक-नैतिकता के केन्द्रीय-तत्त्व : अहिंसा, अनाग्रह और अपरिग्रह
247
हो सका, जितना श्रमणधारा या संन्यासमार्गीय-परंपरा में सम्भव था। यद्यपि श्रमणपरंपराओं के द्वारा हिंसापरक यज्ञ-यागों की आलोचना और मानवीय-विवेक एवं संवेदनशीलता के विकास का एक परिणाम यह हुआ कि वैदिक-परम्परा में भी एक ओर वेदों के पशुहिंसापरक पदों का अर्थ अहिंसक रीति से किया जाने लगा (महाभारत के शान्तिपर्व में राजा वसु का आख्यान- अध्याय 337-338 इसका प्रमाण है), तो दूसरी ओर, धार्मिक-जीवन के लिए कर्मकाण्ड को अनुपयुक्त मानकर औपनिषदिक-धारा के रूप में ज्ञान मार्ग का और भागवत-धर्म के रूप में भक्ति - मार्ग का विकास हुआ। इसमें अहिंसा का अर्थविस्तार सम्पूर्ण प्राणीजगत् अर्थात् त्रस चीजों की हिंसा के निषेध तक हुआ है। वैदिक-परम्परा में संन्यासी को कन्दमूल एवं फल का उपभोग करने की स्वतन्त्रता है, इस प्रकार, वहाँ वानस्पतिक-हिंसा का विचार उपस्थित नहीं है, फिर भी यह तो सत्य है कि अहिंसक-चेतना को सर्वाधिक विकसित करने का श्रेय श्रमण-परम्पराओं को ही है। भारत में ई. पू. 6ठीं शताब्दी का जो भी इतिवृत्त हमें प्राप्त होता है, उससे ऐसा लगता है कि उस युग में पूर्ण अहिंसा के आदर्श को साकार बनाने में श्रमण-सम्प्रदायों में होड़ लगी हुई थी। कम से कम हिंसा ही श्रामण्य-जीवन की श्रेष्ठता का प्रतिमान था। सूत्रकृतांग में आर्द्रक कुमार की विभिन्न मतों के श्रमणों से जो चर्चा है, उसमें मूल प्रश्न यही है कि कौन सबसे अधिक अहिंसक है (देखिए सूत्रकृतांग, 2/6) त्रस प्राणियों (पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि) की हिंसा तो हिंसा थी ही, किन्तु वानस्पतिक और सूक्ष्म प्राणियों की हिंसा को भी हिंसा माना जाने लगा था। मात्र इतना ही नहीं, मनसा, वाचा, कर्मणा और कृत, कारित और अनुमोदित के प्रकारभेदों से नवकोटिक अहिंसा का विचार प्रविष्ट हुआ, अर्थात् मन, वचन
और शरीर से हिंसा करना नहीं, करवाना नहीं और करनेवाले का अनुमोदन भी नहीं करना। बौद्ध और आजीवक-परम्परा के श्रमणों ने भी इस नवकोटिक अहिंसा के आदर्श को स्वीकार कर उसके अर्थ को गहनता और व्यापकता प्रदान की, फिर भी बौद्ध-परम्परा में षट्जीवनिकाय का विचार उपस्थित नहीं था। बौद्ध-भिक्षु नदी-नालों के जल को छानकर उपयोग करते थे। दूसरे, उनके यहाँ नवकोटि अहिंसा की यह अवधारणा भी स्वयं की अपेक्षा से थी- दूसरा हमारे निमित्त क्या करता है, इसका विचार नहीं किया गया, जबकि जैन-परम्परा में श्रमण के निमित्त से की जाने वाली हिंसा का भी विचार किया गया। निर्ग्रन्थ-परम्परा का कहना था कि केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है कि हम मनसा, वाचा, कर्मणा, हिंसा न करें, न कराएं और न उसे अनुमोदन दें, अपितु यह भी आवश्यक है कि दूसरों को हमारे निमित्त हिंसा करने का अवसर भी नहीं दें और उनके द्वारा की गई हिंसा में भागीदार न बनें । यही कारण था कि जहाँ बुद्ध और बौद्ध-भिक्षु निमन्त्रित भोजन को
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org