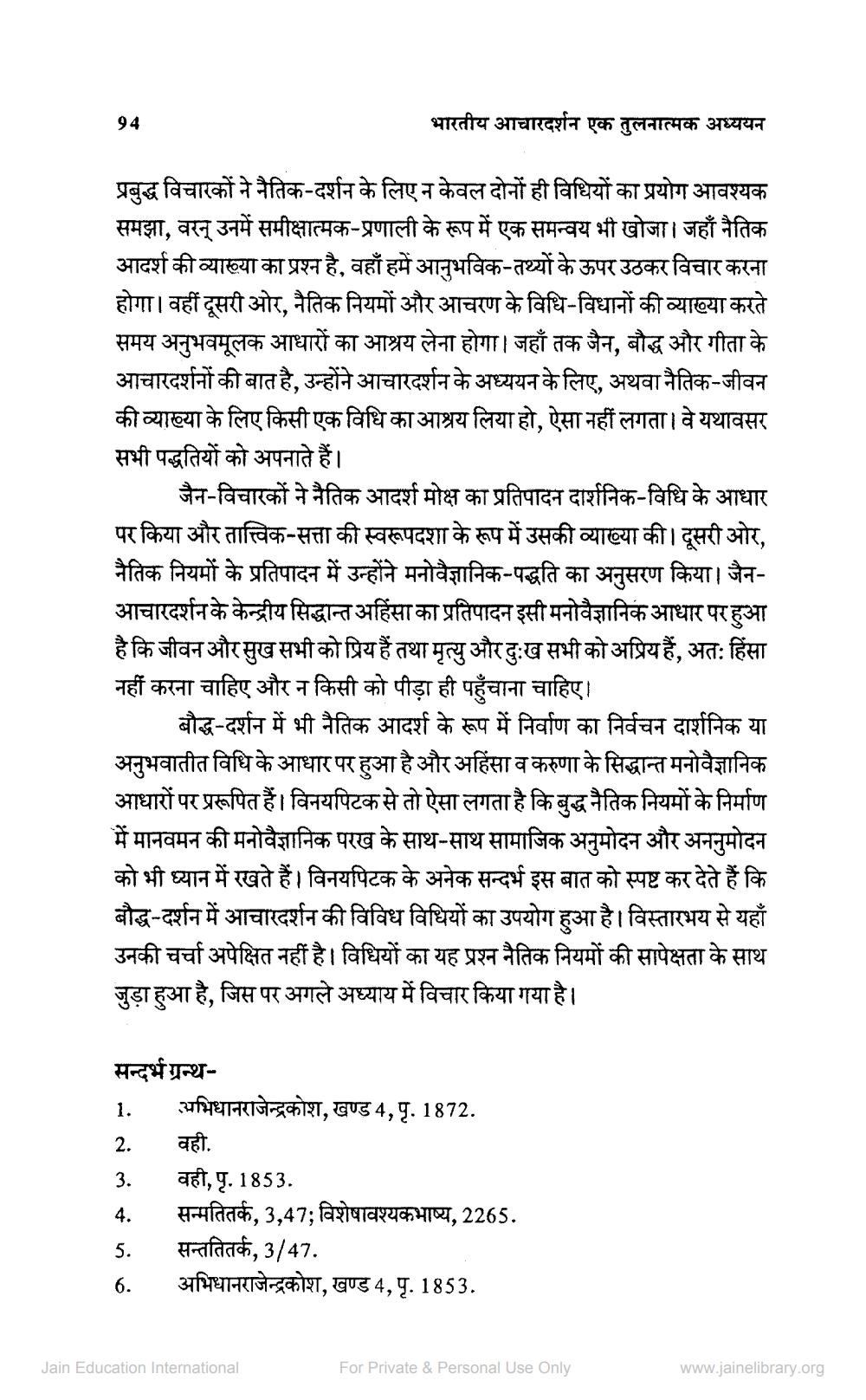________________
94
भारतीय आचारदर्शन एक तुलनात्मक अध्ययन
प्रबुद्ध विचारकों ने नैतिक-दर्शन के लिए न केवल दोनों ही विधियों का प्रयोग आवश्यक समझा, वरन् उनमें समीक्षात्मक-प्रणाली के रूप में एक समन्वय भी खोजा। जहाँ नैतिक आदर्श की व्याख्या का प्रश्न है, वहाँ हमें आनुभविक-तथ्यों के ऊपर उठकर विचार करना होगा। वहीं दूसरी ओर, नैतिक नियमों और आचरण के विधि-विधानों की व्याख्या करते समय अनुभवमूलक आधारों का आश्रय लेना होगा। जहाँ तक जैन, बौद्ध और गीता के आचारदर्शनों की बात है, उन्होंने आचारदर्शन के अध्ययन के लिए, अथवा नैतिक-जीवन की व्याख्या के लिए किसी एक विधि का आश्रय लिया हो, ऐसा नहीं लगता। वे यथावसर सभी पद्धतियों को अपनाते हैं।
जैन-विचारकों ने नैतिक आदर्श मोक्ष का प्रतिपादन दार्शनिक-विधि के आधार पर किया और तात्त्विक-सत्ता की स्वरूपदशा के रूप में उसकी व्याख्या की। दूसरी ओर, नैतिक नियमों के प्रतिपादन में उन्होंने मनोवैज्ञानिक-पद्धति का अनुसरण किया। जैनआचारदर्शन के केन्द्रीय सिद्धान्त अहिंसा का प्रतिपादन इसी मनोवैज्ञानिक आधार पर हुआ है कि जीवन और सुख सभी को प्रिय हैं तथा मृत्यु और दुःख सभी को अप्रिय हैं, अत: हिंसा नहीं करना चाहिए और न किसी को पीड़ा ही पहुँचाना चाहिए।
बौद्ध-दर्शन में भी नैतिक आदर्श के रूप में निर्वाण का निर्वचन दार्शनिक या अनुभवातीत विधि के आधार पर हुआ है और अहिंसा व करुणा के सिद्धान्त मनोवैज्ञानिक आधारों पर प्ररूपित हैं। विनयपिटक से तो ऐसा लगता है कि बुद्ध नैतिक नियमों के निर्माण में मानवमन की मनोवैज्ञानिक परख के साथ-साथ सामाजिक अनुमोदन और अननुमोदन को भी ध्यान में रखते हैं। विनयपिटक के अनेक सन्दर्भ इस बात को स्पष्ट कर देते हैं कि बौद्ध-दर्शन में आचारदर्शन की विविध विधियों का उपयोग हुआ है। विस्तारभय से यहाँ उनकी चर्चा अपेक्षित नहीं है। विधियों का यह प्रश्न नैतिक नियमों की सापेक्षता के साथ जुड़ा हुआ है, जिस पर अगले अध्याय में विचार किया गया है।
सन्दर्भ ग्रन्थ1. अभिधानराजेन्द्रकोश,खण्ड 4, पृ. 1872. 2. वही. 3. वही, पृ. 1853.
सन्मतितर्क, 3,47; विशेषावश्यकभाष्य, 2265. 5. सन्ततितर्क, 3/47. 6. अभिधानराजेन्द्रकोश, खण्ड 4, पृ. 1853.
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org