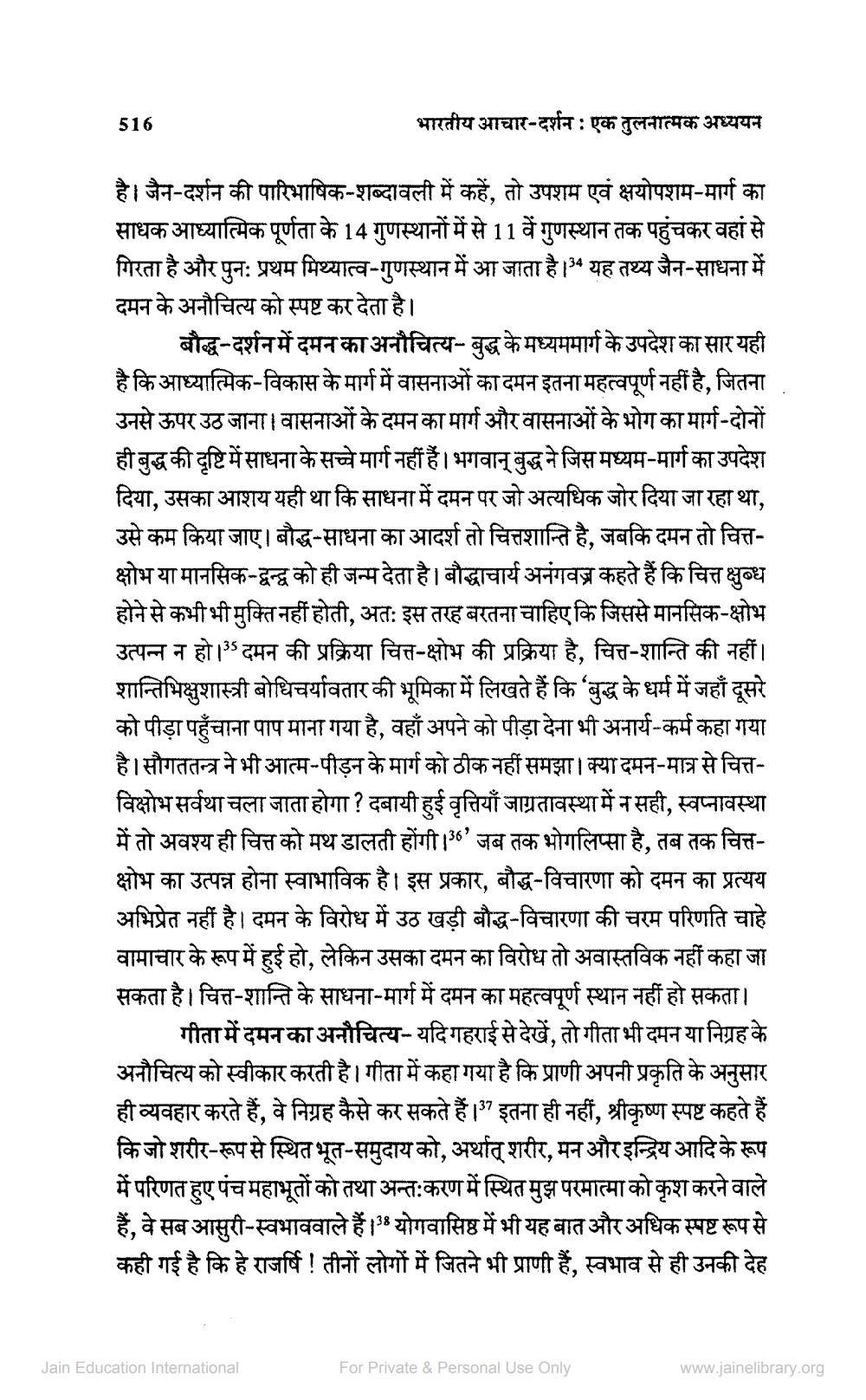________________
516
भारतीय आचार-दर्शन : एक तुलनात्मक अध्ययन
है। जैन-दर्शन की पारिभाषिक-शब्दावली में कहें, तो उपशम एवं क्षयोपशम-मार्ग का साधक आध्यात्मिक पूर्णता के 14 गुणस्थानों में से 11 वें गुणस्थान तक पहुंचकर वहां से गिरता है और पुन: प्रथम मिथ्यात्व-गुणस्थान में आ जाता है। यह तथ्य जैन-साधना में दमन के अनौचित्य को स्पष्ट कर देता है।
बौद्ध-दर्शन में दमनकाअनौचित्य- बुद्ध के मध्यममार्ग के उपदेश का सार यही है कि आध्यात्मिक-विकास के मार्ग में वासनाओं कादमन इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना उनसे ऊपर उठ जाना। वासनाओं के दमन का मार्ग और वासनाओं के भोग का मार्ग-दोनों ही बुद्ध की दृष्टि में साधना के सच्चे मार्ग नहीं हैं। भगवान् बुद्ध ने जिस मध्यम-मार्ग का उपदेश दिया, उसका आशय यही था कि साधना में दमन पर जो अत्यधिक जोर दिया जा रहा था. उसे कम किया जाए। बौद्ध-साधना का आदर्श तो चित्तशान्ति है, जबकि दमन तो चित्तक्षोभ या मानसिक-द्वन्द्व को ही जन्म देता है। बौद्धाचार्य अनंगवज्र कहते हैं कि चित्त क्षुब्ध होने से कभी भी मुक्ति नहीं होती, अत: इस तरह बरतना चाहिए कि जिससे मानसिक-क्षोभ उत्पन्न न हो। दमन की प्रक्रिया चित्त-क्षोभ की प्रक्रिया है, चित्त-शान्ति की नहीं। शान्तिभिक्षुशास्त्री बोधिचर्यावतार की भूमिका में लिखते हैं कि बुद्ध के धर्म में जहाँ दूसरे को पीड़ा पहुँचाना पाप माना गया है, वहाँ अपने को पीड़ा देना भी अनार्य-कर्म कहा गया है।सौगततन्त्र ने भी आत्म-पीड़न के मार्ग को ठीक नहीं समझा। क्या दमन-मात्र से चित्तविक्षोभसर्वथा चला जाता होगा? दबायी हुई वृत्तियाँ जाग्रतावस्था में न सही, स्वप्नावस्था में तो अवश्य ही चित्त को मथ डालती होंगी।' जब तक भोगलिप्सा है, तब तक चित्तक्षोभ का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। इस प्रकार, बौद्ध-विचारणा को दमन का प्रत्यय अभिप्रेत नहीं है। दमन के विरोध में उठ खड़ी बौद्ध-विचारणा की चरम परिणति चाहे वामाचार के रूप में हुई हो, लेकिन उसका दमन का विरोध तो अवास्तविक नहीं कहा जा सकता है। चित्त-शान्ति के साधना-मार्ग में दमन का महत्वपूर्ण स्थान नहीं हो सकता।
गीतामें दमनकाअनौचित्य- यदि गहराई से देखें, तो गीता भी दमन या निग्रह के अनौचित्य को स्वीकार करती है। गीता में कहा गया है कि प्राणी अपनी प्रकृति के अनुसार ही व्यवहार करते हैं, वे निग्रह कैसे कर सकते हैं। इतना ही नहीं, श्रीकृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जो शरीर-रूप से स्थित भूत-समुदाय को, अर्थात् शरीर, मन और इन्द्रिय आदि के रूप में परिणत हुए पंचमहाभूतों को तथा अन्त:करण में स्थित मुझ परमात्मा को कृश करने वाले हैं, वे सब आसुरी-स्वभाववाले हैं। योगवासिष्ठ में भी यह बात और अधिक स्पष्ट रूप से कही गई है कि हे राजर्षि ! तीनों लोगों में जितने भी प्राणी हैं, स्वभाव से ही उनकी देह
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org