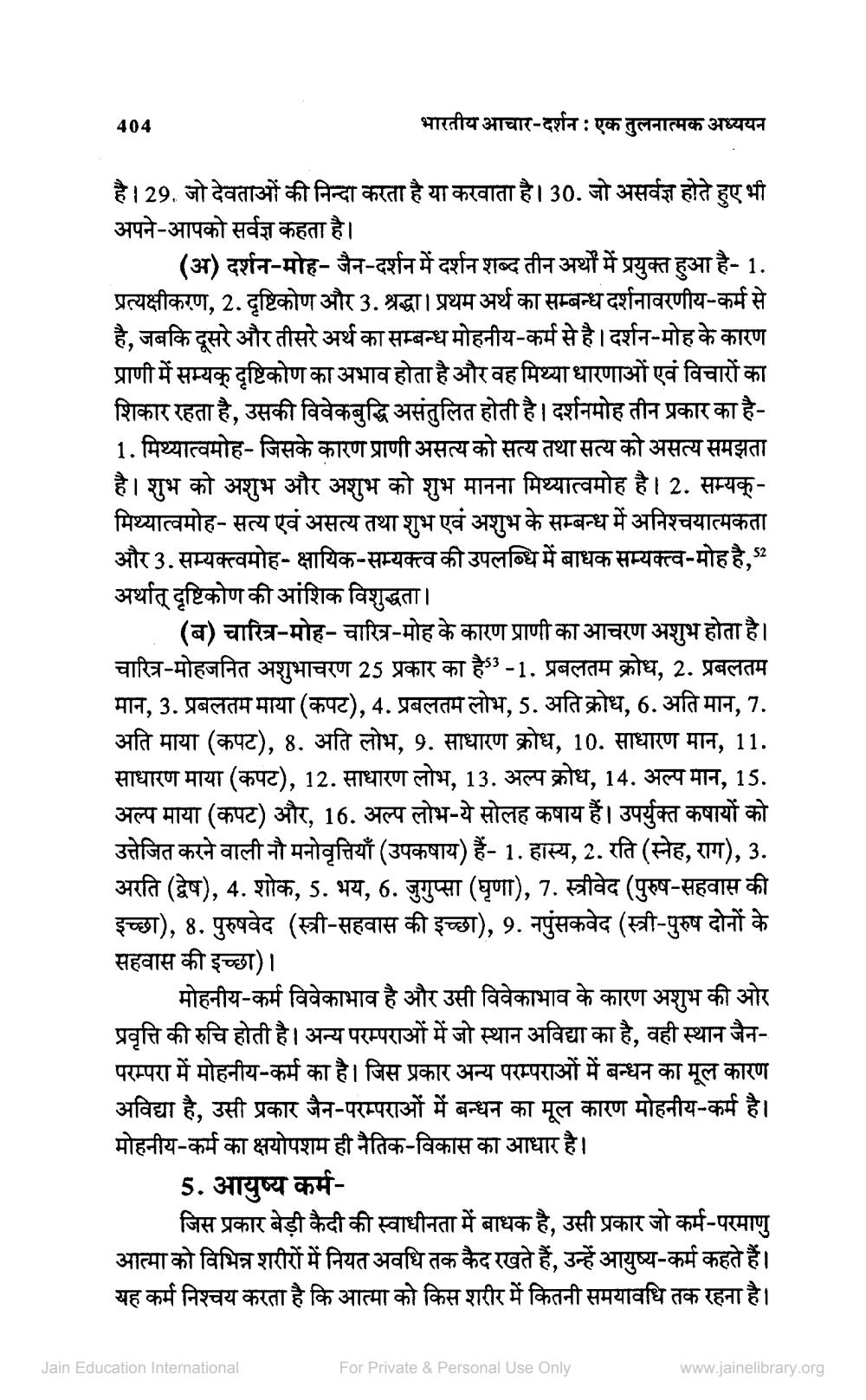________________
404
भारतीय आचार-दर्शन : एक तुलनात्मक अध्ययन
है। 29. जो देवताओं की निन्दा करता है या करवाता है। 30. जो असर्वज्ञ होते हुए भी अपने-आपको सर्वज्ञ कहता है।
(अ) दर्शन-मोह- जैन-दर्शन में दर्शन शब्द तीन अर्थों में प्रयुक्त हुआ है- 1. प्रत्यक्षीकरण, 2. दृष्टिकोण और 3. श्रद्धा। प्रथम अर्थ का सम्बन्ध दर्शनावरणीय-कर्म से है, जबकि दूसरे और तीसरे अर्थ का सम्बन्ध मोहनीय-कर्म से है। दर्शन-मोह के कारण प्राणी में सम्यक् दृष्टिकोण का अभाव होता है और वह मिथ्या धारणाओं एवं विचारों का शिकार रहता है, उसकी विवेकबुद्धि असंतुलित होती है। दर्शनमोह तीन प्रकार का है1. मिथ्यात्वमोह-जिसके कारण प्राणी असत्य को सत्य तथा सत्य को असत्य समझता है। शुभ को अशुभ और अशुभ को शुभ मानना मिथ्यात्वमोह है। 2. सम्यक्मिथ्यात्वमोह- सत्य एवं असत्य तथा शुभ एवं अशुभ के सम्बन्ध में अनिश्चयात्मकता
और 3. सम्यक्त्वमोह- क्षायिक-सम्यक्त्व की उपलब्धि में बाधक सम्यक्त्व-मोह है," अर्थात् दृष्टिकोण की आंशिक विशुद्धता।
(ब) चारित्र-मोह- चारित्र-मोह के कारण प्राणी का आचरण अशुभ होता है। चारित्र-मोहजनित अशुभाचरण 25 प्रकार का है -1. प्रबलतम क्रोध, 2. प्रबलतम मान, 3. प्रबलतम माया (कपट), 4. प्रबलतम लोभ, 5. अति क्रोध, 6. अति मान, 7. अति माया (कपट), 8. अति लोभ, 9. साधारण क्रोध, 10. साधारण मान, 11. साधारण माया (कपट), 12. साधारण लोभ, 13. अल्प क्रोध, 14. अल्प मान, 15. अल्प माया (कपट) और, 16. अल्प लोभ-ये सोलह कषाय हैं। उपर्युक्त कषायों को उत्तेजित करने वाली नौ मनोवृत्तियाँ (उपकषाय) हैं- 1. हास्य, 2.रति (स्नेह, राग), 3. अरति (द्वेष), 4. शोक, 5. भय, 6. जुगुप्सा (घृणा), 7. स्त्रीवेद (पुरुष-सहवास की इच्छा), 8. पुरुषवेद (स्त्री-सहवास की इच्छा), 9. नपुंसकवेद (स्त्री-पुरुष दोनों के सहवास की इच्छा)।
मोहनीय-कर्म विवेकाभाव है और उसी विवेकाभाव के कारण अशुभ की ओर प्रवृत्ति की रुचि होती है। अन्य परम्पराओं में जो स्थान अविद्या का है, वही स्थान जैनपरम्परा में मोहनीय-कर्म का है। जिस प्रकार अन्य परम्पराओं में बन्धन का मूल कारण अविद्या है, उसी प्रकार जैन-परम्पराओं में बन्धन का मूल कारण मोहनीय-कर्म है। मोहनीय-कर्म का क्षयोपशम ही नैतिक-विकास का आधार है।
5. आयुष्य कर्म
जिस प्रकार बेड़ी कैदी की स्वाधीनता में बाधक है, उसी प्रकार जो कर्म-परमाणु आत्मा को विभिन्न शरीरों में नियत अवधि तक कैद रखते हैं, उन्हें आयुष्य-कर्म कहते हैं। यह कर्म निश्चय करता है कि आत्मा को किस शरीर में कितनी समयावधि तक रहना है।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org