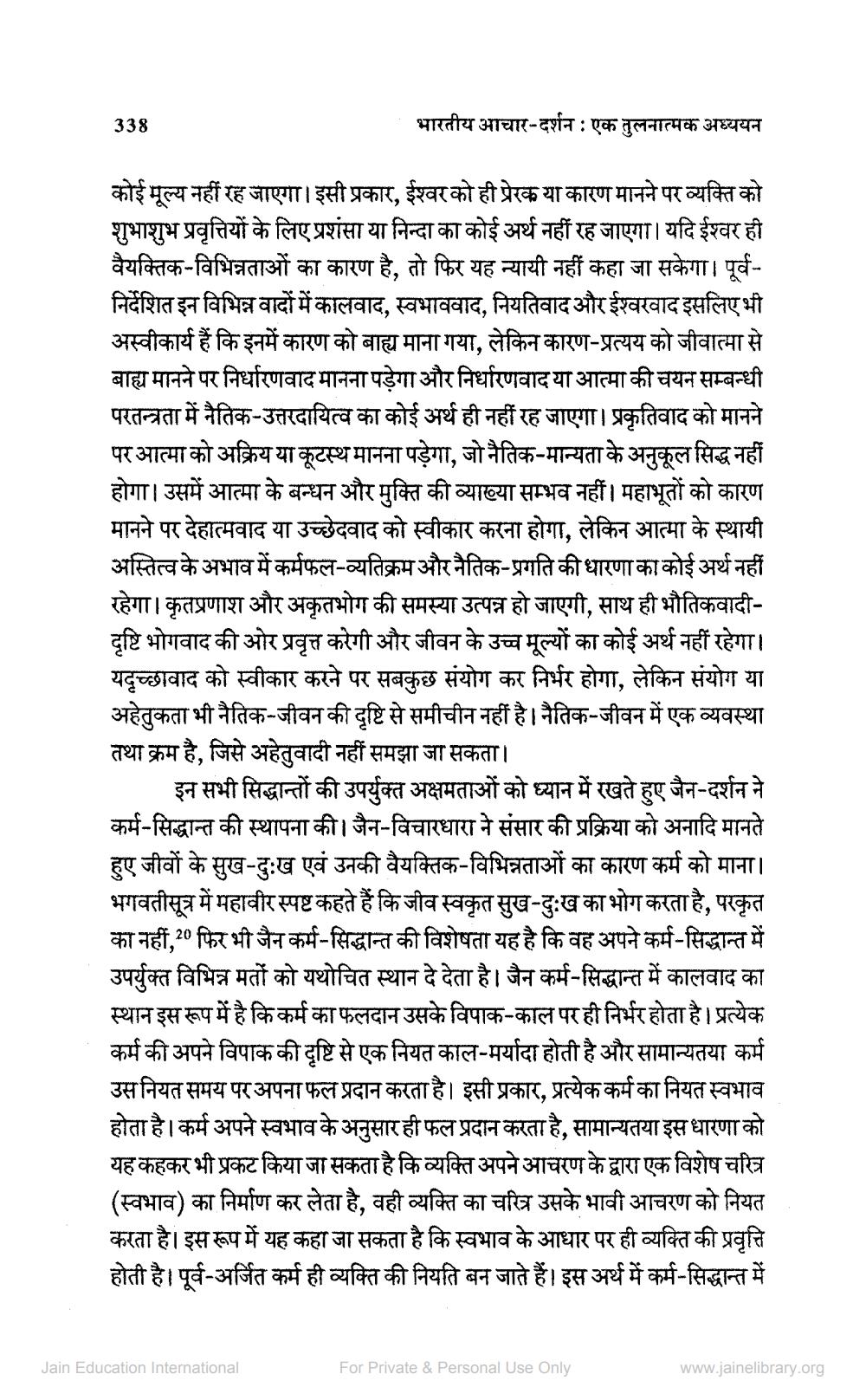________________
338
भारतीय आचार-दर्शन : एक तुलनात्मक अध्ययन
कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। इसी प्रकार, ईश्वरको ही प्रेरक या कारण मानने पर व्यक्ति को शुभाशुभ प्रवृत्तियों के लिए प्रशंसा या निन्दा का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। यदि ईश्वर ही वैयक्तिक-विभिन्नताओं का कारण है, तो फिर यह न्यायी नहीं कहा जा सकेगा। पूर्वनिर्देशित इन विभिन्न वादों में कालवाद, स्वभाववाद, नियतिवाद और ईश्वरवाद इसलिए भी अस्वीकार्य हैं कि इनमें कारण को बाह्य माना गया, लेकिन कारण-प्रत्यय को जीवात्मा से बाह्य मानने पर निर्धारणवादमानना पड़ेगा और निर्धारणवादया आत्मा की चयन सम्बन्धी परतन्त्रता में नैतिक-उत्तरदायित्व का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। प्रकृतिवाद को मानने पर आत्माको अक्रिय या कूटस्थमानना पड़ेगा, जो नैतिक-मान्यता के अनुकूल सिद्ध नहीं होगा। उसमें आत्मा के बन्धन और मुक्ति की व्याख्या सम्भव नहीं। महाभूतों को कारण मानने पर देहात्मवाद या उच्छेदवाद को स्वीकार करना होगा, लेकिन आत्मा के स्थायी अस्तित्व के अभाव में कर्मफल-व्यतिक्रम और नैतिक-प्रगति की धारणा का कोई अर्थ नहीं रहेगा। कृतप्रणाश और अकृतभोग की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, साथ ही भौतिकवादीदृष्टि भोगवाद की ओर प्रवृत्त करेगी और जीवन के उच्च मूल्यों का कोई अर्थ नहीं रहेगा। यदृच्छावाद को स्वीकार करने पर सबकुछ संयोग कर निर्भर होगा, लेकिन संयोग या
अहेतुकता भी नैतिक-जीवन की दृष्टि से समीचीन नहीं है। नैतिक-जीवन में एक व्यवस्था तथा क्रम है, जिसे अहेतुवादी नहीं समझा जा सकता।
इन सभी सिद्धान्तों की उपर्युक्त अक्षमताओं को ध्यान में रखते हुए जैन-दर्शन ने कर्म-सिद्धान्त की स्थापना की। जैन-विचारधारा ने संसार की प्रक्रिया को अनादि मानते हुए जीवों के सुख-दुःख एवं उनकी वैयक्तिक-विभिन्नताओं का कारण कर्म को माना। भगवतीसूत्र में महावीर स्पष्ट कहते हैं कि जीवस्वकृत सुख-दुःख का भोग करता है, परकृत का नहीं,20 फिर भी जैन कर्म-सिद्धान्त की विशेषता यह है कि वह अपने कर्म-सिद्धान्त में उपर्युक्त विभिन्न मतों को यथोचित स्थान दे देता है। जैन कर्म-सिद्धान्त में कालवाद का स्थान इस रूप में है कि कर्म का फलदान उसके विपाक-काल पर ही निर्भर होता है। प्रत्येक कर्म की अपने विपाक की दृष्टि से एक नियत काल-मर्यादा होती है और सामान्यतया कर्म उसनियत समय पर अपना फल प्रदान करता है। इसी प्रकार, प्रत्येककर्म का नियत स्वभाव होता है। कर्म अपने स्वभाव के अनुसार ही फल प्रदान करता है, सामान्यतया इस धारणा को यह कहकर भी प्रकट किया जा सकता है कि व्यक्ति अपने आचरण के द्वारा एक विशेष चरित्र (स्वभाव) का निर्माण कर लेता है, वही व्यक्ति का चरित्र उसके भावी आचरण को नियत करता है। इस रूप में यह कहा जा सकता है कि स्वभाव के आधार पर ही व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है। पूर्व-अर्जित कर्म ही व्यक्ति की नियति बन जाते हैं। इस अर्थ में कर्म-सिद्धान्त में
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org