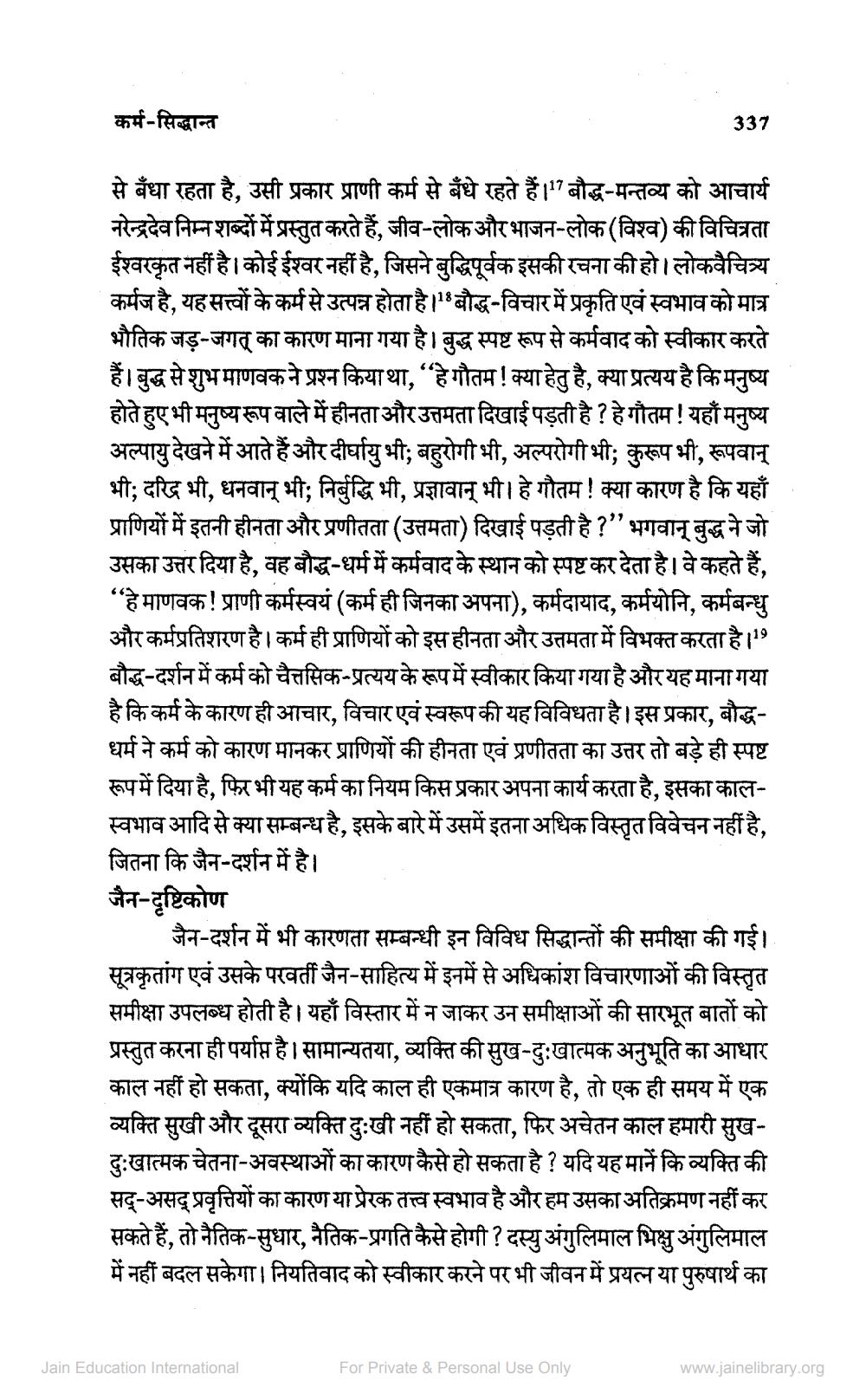________________
कर्म-सिद्धान्त
337
से बँधा रहता है, उसी प्रकार प्राणी कर्म से बँधे रहते हैं।" बौद्ध-मन्तव्य को आचार्य नरेन्द्रदेव निम्न शब्दों में प्रस्तुत करते हैं, जीव-लोक और भाजन-लोक (विश्व) की विचित्रता ईश्वरकृत नहीं है। कोई ईश्वर नहीं है, जिसने बुद्धिपूर्वक इसकी रचना की हो। लोकवैचित्र्य कर्मज है, यह सत्त्वों के कर्म से उत्पन्न होता है। बौद्ध-विचार में प्रकृति एवं स्वभावको मात्र भौतिक जड़-जगत् का कारण माना गया है। बुद्ध स्पष्ट रूप से कर्मवाद को स्वीकार करते हैं। बुद्ध से शुभमाणवक ने प्रश्न किया था, “हे गौतम! क्याहेतु है, क्या प्रत्यय है कि मनुष्य होते हुए भी मनुष्यरूप वाले में हीनताऔर उत्तमता दिखाई पड़ती है ? हे गौतम ! यहाँ मनुष्य अल्पायु देखने में आते हैं और दीर्घायु भी; बहुरोगीभी, अल्परोगीभी; कुरूप भी, रूपवान् भी; दरिद्र भी, धनवान् भी; निर्बुद्धि भी, प्रज्ञावान् भी। हे गौतम! क्या कारण है कि यहाँ प्राणियों में इतनी हीनता और प्रणीतता (उत्तमता) दिखाई पड़ती है ?" भगवान् बुद्ध ने जो उसका उत्तर दिया है, वह बौद्ध-धर्म में कर्मवाद के स्थान को स्पष्ट कर देता है। वे कहते हैं, "हे माणवक! प्राणी कर्मस्वयं (कर्म ही जिनका अपना), कर्मदायाद, कर्मयोनि, कर्मबन्धु और कर्मप्रतिशरण है। कर्म ही प्राणियों को इस हीनता और उत्तमता में विभक्त करता है।" बौद्ध-दर्शन में कर्म को चैत्तसिक-प्रत्यय के रूप में स्वीकार किया गया है और यह माना गया है कि कर्म के कारण ही आचार, विचार एवं स्वरूप की यह विविधता है। इस प्रकार, बौद्धधर्म ने कर्म को कारण मानकर प्राणियों की हीनता एवं प्रणीतता का उत्तर तो बड़े ही स्पष्ट रूप में दिया है, फिर भी यह कर्म का नियम किस प्रकार अपना कार्य करता है, इसका कालस्वभाव आदि से क्या सम्बन्ध है, इसके बारे में उसमें इतना अधिक विस्तृत विवेचन नहीं है, जितना कि जैन-दर्शन में है। जैन-दृष्टिकोण
जैन-दर्शन में भी कारणता सम्बन्धी इन विविध सिद्धान्तों की समीक्षा की गई। सूत्रकृतांग एवं उसके परवर्ती जैन-साहित्य में इनमें से अधिकांश विचारणाओं की विस्तृत समीक्षा उपलब्ध होती है। यहाँ विस्तार में न जाकर उन समीक्षाओं की सारभूत बातों को प्रस्तुत करना ही पर्याप्त है। सामान्यतया, व्यक्ति की सुख-दुःखात्मक अनुभूति का आधार काल नहीं हो सकता, क्योंकि यदि काल ही एकमात्र कारण है, तो एक ही समय में एक व्यक्ति सुखी और दूसरा व्यक्ति दुःखी नहीं हो सकता, फिर अचेतन काल हमारी सुखदुःखात्मक चेतना-अवस्थाओं का कारण कैसे हो सकता है ? यदि यह मानें कि व्यक्ति की सद्-असद्प्रवृत्तियों का कारण या प्रेरक तत्त्व स्वभाव है और हम उसका अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं, तो नैतिक-सुधार, नैतिक-प्रगति कैसे होगी? दस्यु अंगुलिमाल भिक्षु अंगुलिमाल में नहीं बदल सकेगा। नियतिवाद को स्वीकार करने पर भी जीवन में प्रयत्न या पुरुषार्थ का
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org