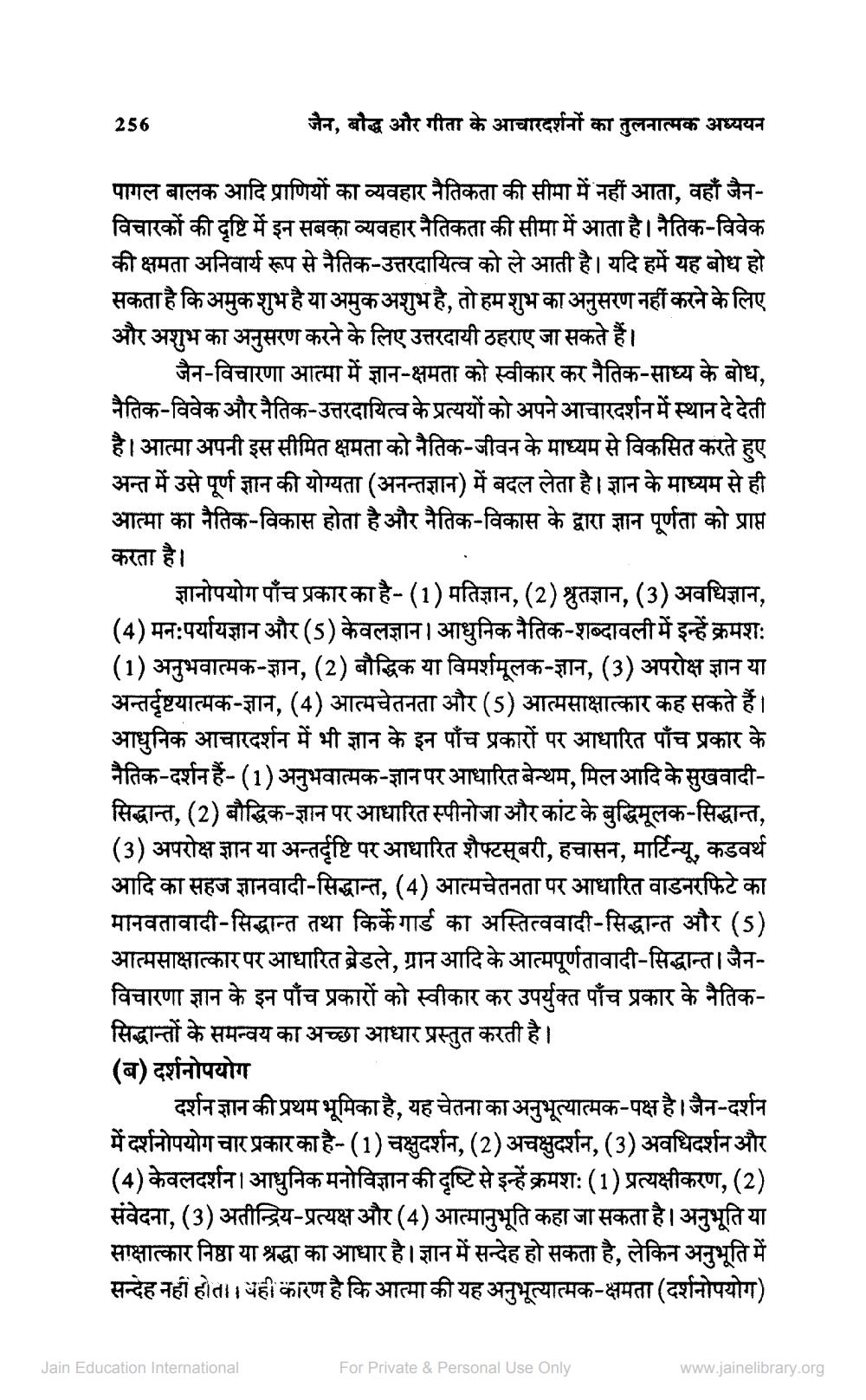________________
जैन, बौद्ध और गीता के आचारदर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन
पागल बालक आदि प्राणियों का व्यवहार नैतिकता की सीमा में नहीं आता, वहाँ जैनविचारकों की दृष्टि में इन सबका व्यवहार नैतिकता की सीमा में आता है। नैतिक-विवेक
क्षमता अनिवार्य रूप से नैतिक- उत्तरदायित्व को ले आती है। यदि हमें यह बोध हो सकता है कि अमुक शुभ है या अमुक अशुभ है, तो हम शुभ का अनुसरण नहीं करने के लिए और अशुभ का अनुसरण करने के लिए उत्तरदायी ठहराए जा सकते हैं।
जैन- विचारणा आत्मा में ज्ञान - क्षमता को स्वीकार कर नैतिक-साध्य के बोध, नैतिक- विवेक और नैतिक- उत्तरदायित्व के प्रत्ययों को अपने आचारदर्शन में स्थान दे देती है। आत्मा अपनी इस सीमित क्षमता को नैतिक जीवन के माध्यम से विकसित करते हुए अन्त में उसे पूर्ण ज्ञान की योग्यता (अनन्तज्ञान) में बदल लेता है। ज्ञान के माध्यम से ही आत्मा का नैतिक विकास होता है और नैतिक विकास के द्वारा ज्ञान पूर्णता को प्राप्त करता है।
256
-
ज्ञानोपयोग पाँच प्रकार का है - ( 1 ) मतिज्ञान, ( 2 ) श्रुतज्ञान, (3) अवधिज्ञान, (4) मन: पर्यायज्ञान और (5) केवलज्ञान। आधुनिक नैतिक-शब्दावली में इन्हें क्रमश: (1) अनुभवात्मक ज्ञान, (2) बौद्धिक या विमर्शमूलक ज्ञान, (3) अपरोक्ष ज्ञान या अन्तर्दृष्टयात्मक - ज्ञान, (4) आत्मचेतनता और (5) आत्मसाक्षात्कार कह सकते हैं। आधुनिक आचारदर्शन में भी ज्ञान के इन पाँच प्रकारों पर आधारित पाँच प्रकार के नैतिक-दर्शन हैं- (1) अनुभवात्मक-ज्ञान पर आधारित बेन्थम, मिल आदि के सुखवादीसिद्धान्त, (2) बौद्धिक - ज्ञान पर आधारित स्पीनोजा और कांट के बुद्धिमूलक सिद्धान्त, (3) अपरोक्ष ज्ञान या अन्तर्दृष्टि पर आधारित शैफ्टस्बरी, हचासन, मार्टिन्यू, कडवर्थ आदि का सहज ज्ञानवादी - सिद्धान्त, (4) आत्मचेतनता पर आधारित वाडनरफिटे का मानवतावादी - सिद्धान्त तथा किर्केगार्ड का अस्तित्ववादी सिद्धान्त और (5) आत्मसाक्षात्कार पर आधारित ब्रेडले, ग्रान आदि के आत्मपूर्णतावादी सिद्धान्त । जैनविचारणा ज्ञान के इन पाँच प्रकारों को स्वीकार कर उपर्युक्त पाँच प्रकार के नैतिकसिद्धान्तों के समन्वय का अच्छा आधार प्रस्तुत करती है।
(ब) दर्शनोपयोग
-
दर्शन ज्ञान की प्रथम भूमिका है, यह चेतना का अनुभूत्यात्मक पक्ष है। जैन-दर्शन में दर्शनोपयोग चार प्रकार का है- (1) चक्षुदर्शन, (2) अचक्षुदर्शन, (3) अवधिदर्शन और (4) केवलदर्शन । आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि से इन्हें क्रमश: (1) प्रत्यक्षीकरण, (2) संवेदना, (3) अतीन्द्रिय- प्रत्यक्ष और (4) आत्मानुभूति कहा जा सकता है। अनुभूति या साक्षात्कार निष्ठा या श्रद्धा का आधार है। ज्ञान में सन्देह हो सकता है, लेकिन अनुभूति में सन्देह नहीं होता। यही कारण है कि आत्मा की यह अनुभूत्यात्मक क्षमता (दर्शनोपयोग)
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org