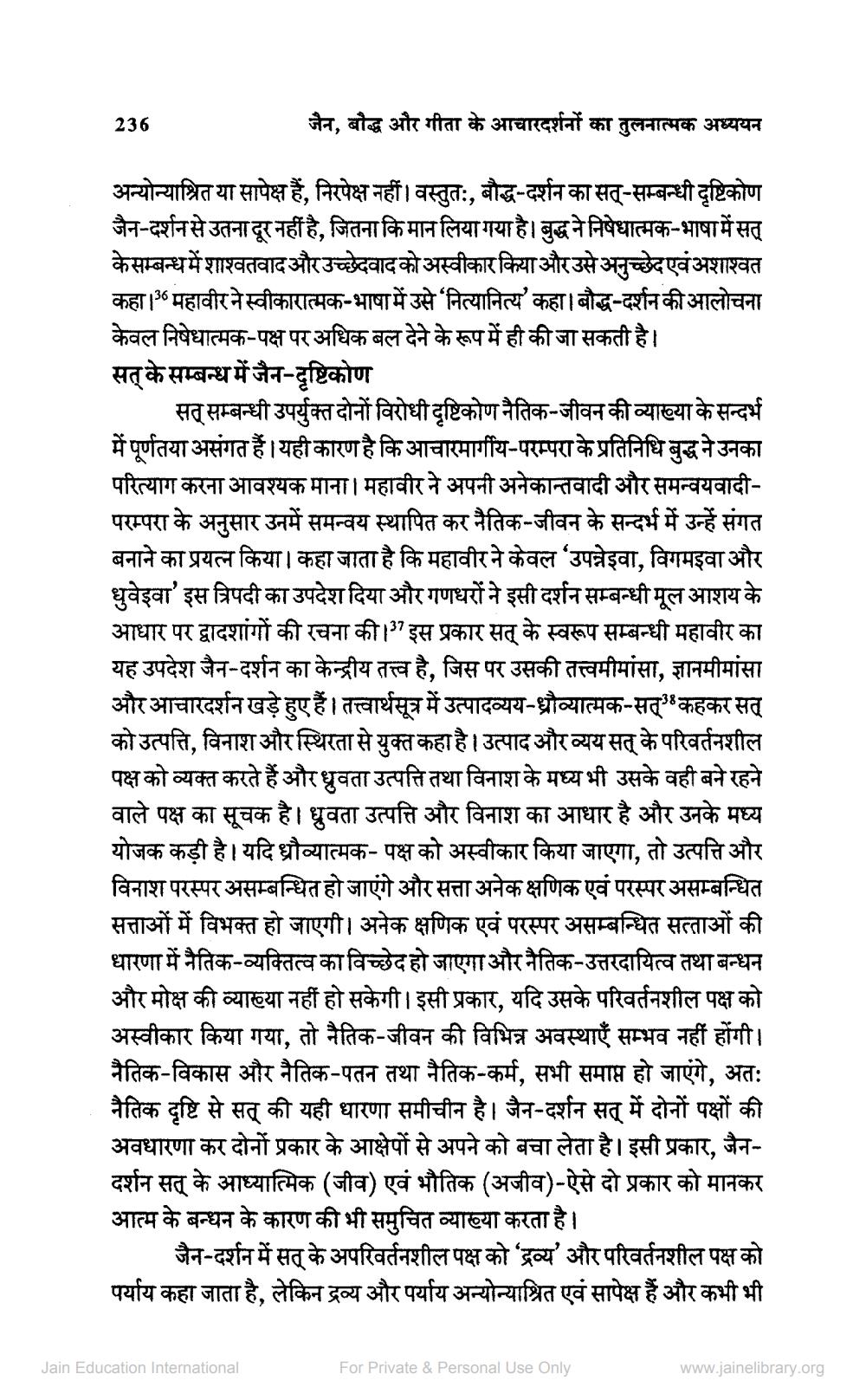________________
जैन, बौद्ध और गीता के आचारदर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन
अन्योन्याश्रित या सापेक्ष हैं, निरपेक्ष नहीं । वस्तुतः, बौद्ध दर्शन का सत्-सम्बन्धी दृष्टिकोण जैन-दर्शन से उतना दूर नहीं है, जितना कि मान लिया गया है। बुद्ध ने निषेधात्मक-भाषा में सत् के सम्बन्ध में शाश्वतवाद और उच्छेदवाद को अस्वीकार किया और उसे अनुच्छेद एवं अशाश्वत कहा | 36 महावीर ने स्वीकारात्मक - भाषा में उसे 'नित्यानित्य' कहा। बौद्ध दर्शन की आलोचना केवल निषेधात्मक पक्ष पर अधिक बल देने के रूप में ही की जा सकती है।
-
236
सत् के सम्बन्ध में जैन- दृष्टिकोण
सत् सम्बन्धी उपर्युक्त दोनों विरोधी दृष्टिकोण नैतिक जीवन की व्याख्या के सन्दर्भ में पूर्णतया असंगत हैं । यही कारण है कि आचारमार्गीय परम्परा के प्रतिनिधि बुद्ध ने उनका परित्याग करना आवश्यक माना । महावीर ने अपनी अनेकान्तवादी और समन्वयवादीपरम्परा के अनुसार उनमें समन्वय स्थापित कर नैतिक जीवन के सन्दर्भ में उन्हें संगत बनाने का प्रयत्न किया। कहा जाता है कि महावीर ने केवल 'उपन्नेइवा, विगमइवा और धुवेइवा' इस त्रिपदी का उपदेश दिया और गणधरों ने इसी दर्शन सम्बन्धी मूल आशय के आधार पर द्वादशांगों की रचना की । " इस प्रकार सत् के स्वरूप सम्बन्धी महावीर का यह उपदेश जैन-दर्शन का केन्द्रीय तत्त्व है, जिस पर उसकी तत्त्वमीमांसा, ज्ञानमीमांसा और आचारदर्शन खड़े हुए हैं। तत्त्वार्थसूत्र में उत्पादव्यय- ध्रौव्यात्मक - सत्" कहकर सत् को उत्पत्ति, विनाश और स्थिरता से युक्त कहा है। उत्पाद और व्यय सत् के परिवर्तनशील पक्ष को व्यक्त करते हैं और ध्रुवता उत्पत्ति तथा विनाश के मध्य भी उसके वही बने रहने वाले पक्ष का सूचक है। ध्रुवता उत्पत्ति और विनाश का आधार है और उनके मध्य योजक कड़ी है । यदि ध्रौव्यात्मक - पक्ष को अस्वीकार किया जाएगा, तो उत्पत्ति और विनाश परस्पर असम्बन्धित हो जाएंगे और सत्ता अनेक क्षणिक एवं परस्पर असम्बन्धित सत्ताओं में विभक्त हो जाएगी। अनेक क्षणिक एवं परस्पर असम्बन्धित सत्ताओं की धारणा में नैतिक व्यक्तित्व का विच्छेद हो जाएगा और नैतिक- उत्तरदायित्व तथा बन्धन और मोक्ष की व्याख्या नहीं हो सकेगी। इसी प्रकार, यदि उसके परिवर्तनशील पक्ष को अस्वीकार किया गया, तो नैतिक जीवन की विभिन्न अवस्थाएँ सम्भव नहीं होंगी। नैतिक-विकास और नैतिक पतन तथा नैतिक-कर्म, सभी समाप्त हो जाएंगे, अतः नैतिक दृष्टि से सत् की यही धारणा समीचीन है। जैन दर्शन सत् में दोनों पक्षों की अवधारणा कर दोनों प्रकार के आक्षेपों से अपने को बचा लेता है। इसी प्रकार, जैनदर्शन सत् के आध्यात्मिक (जीव) एवं भौतिक (अजीव) - ऐसे दो प्रकार को मानकर धन के कारण की भी समुचित व्याख्या करता है।
जैन- दर्शन में सत् के अपरिवर्तनशील पक्ष को 'द्रव्य' और परिवर्तनशील पक्ष को पर्याय कहा जाता है, लेकिन द्रव्य और पर्याय अन्योन्याश्रित एवं सापेक्ष हैं और कभी भी
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org