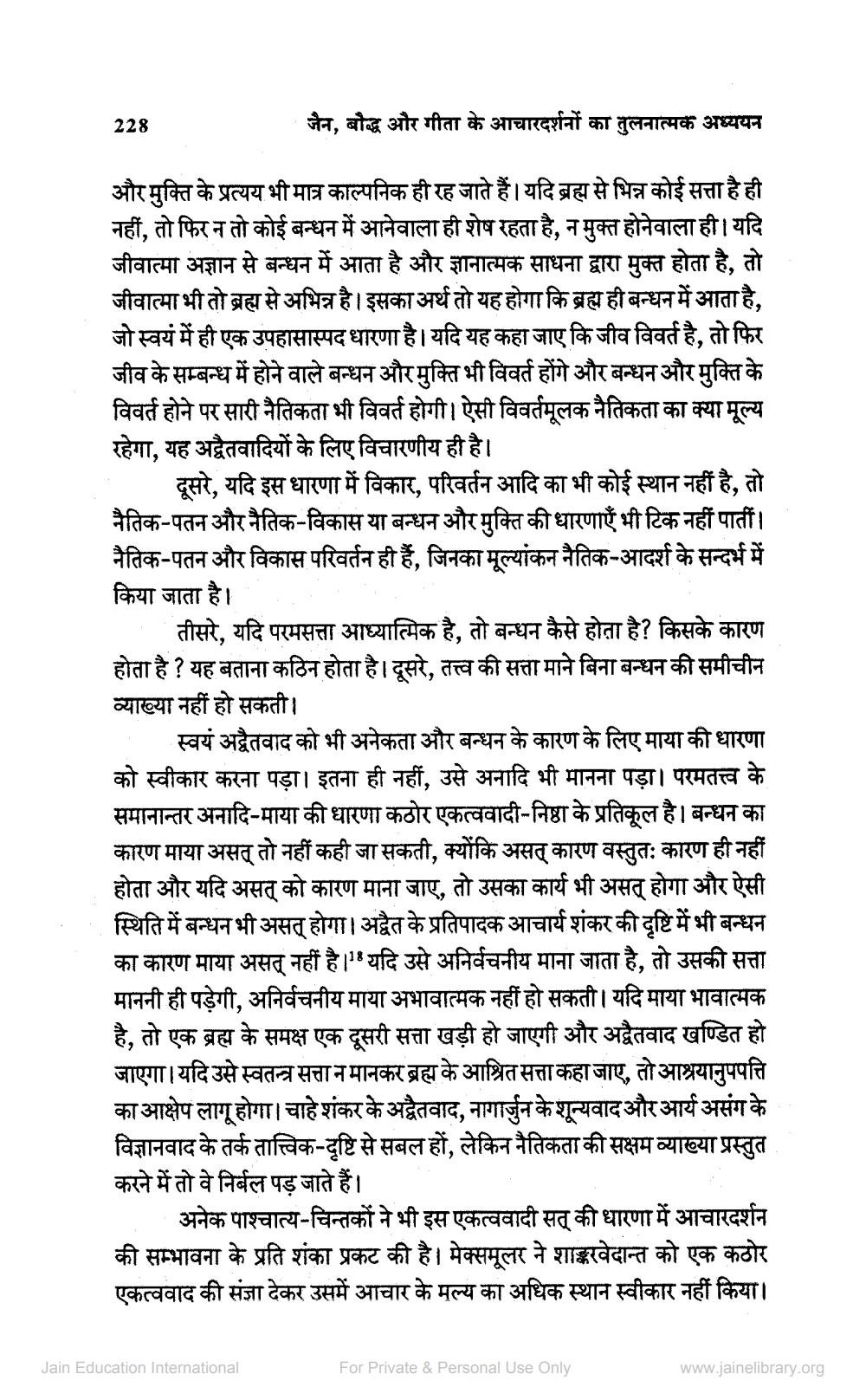________________
जैन, बौद्ध और गीता के आचारदर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन
और मुक्ति के प्रत्यय भी मात्र काल्पनिक ही रह जाते हैं । यदि ब्रह्म से भिन्न कोई सत्ता है ही नहीं, तो फिर न तो कोई बन्धन में आनेवाला ही शेष रहता है, न मुक्त होनेवाला ही। यदि जीवात्मा अज्ञान से बन्धन में आता है और ज्ञानात्मक साधना द्वारा मुक्त होता है, तो जीवात्मा भी तो ब्रह्म से अभिन्न है। इसका अर्थ तो यह होगा कि ब्रह्म ही बन्धन में आता है, जो स्वयं में ही एक उपहासास्पद धारणा है। यदि यह कहा जाए कि जीव विवर्त है, तो फिर
aa सम्बन्ध में होने वाले बन्धन और मुक्ति भी विवर्त होंगे और बन्धन और मुक्ति के विवर्त होने पर सारी नैतिकता भी विवर्त होगी। ऐसी विवर्तमूलक नैतिकता का क्या मूल्य रहेगा, यह अद्वैतवादियों के लिए विचारणीय ही है ।
228
दूसरे, यदि इस धारणा में विकार, परिवर्तन आदि का भी कोई स्थान नहीं है, तो नैतिक पतन और नैतिक-विकास या बन्धन और मुक्ति की धारणाएँ भी टिक नहीं पातीं। नैतिक-पतन और विकास परिवर्तन ही हैं, जिनका मूल्यांकन नैतिक आदर्श के सन्दर्भ में किया जाता है।
तीसरे, यदि परमसत्ता आध्यात्मिक है, तो बन्धन कैसे होता है ? किसके कारण होता है ? यह बताना कठिन होता है। दूसरे तत्त्व की सत्ता माने बिना बन्धन की समीचीन व्याख्या नहीं हो सकती।
स्वयं अद्वैतवाद को भी अनेकता और बन्धन के कारण के लिए माया की धारणा को स्वीकार करना पड़ा। इतना ही नहीं, उसे अनादि भी मानना पड़ा । परमतत्त्व के समानान्तर अनादि- माया की धारणा कठोर एकत्ववादी- निष्ठा के प्रतिकूल है । बन्धन का कारण माया असत् तो नहीं कही जा सकती, क्योंकि असत् कारण वस्तुतः कारण ही नहीं होता और यदि असत् को कारण माना जाए, तो उसका कार्य भी असत् होगा और ऐसी स्थिति में बन्धन भी असत् होगा। अद्वैत के प्रतिपादक आचार्य शंकर की दृष्टि में भी बन्धन का कारण माया असत् नहीं है।" यदि उसे अनिर्वचनीय माना जाता है, तो उसकी सत्ता माननी ही पड़ेगी, अनिर्वचनीय माया अभावात्मक नहीं हो सकती । यदि माया भावात्मक है, तो एक ब्रह्म के समक्ष एक दूसरी सत्ता खड़ी हो जाएगी और अद्वैतवाद खण्डित हो जाएगा। यदि उसे स्वतन्त्र सत्ता न मानकर ब्रह्म के आश्रित सत्ता कहा जाए, तो आश्रयानुपपत्ति का आक्षेप लागू होगा। चाहे शंकर के अद्वैतवाद, नागार्जुन के शून्यवाद और आर्य असंग के विज्ञानवाद के तर्क तात्त्विक दृष्टि से सबल हों, लेकिन नैतिकता की सक्षम व्याख्या प्रस्तुत करने में तो वे निर्बल पड़ जाते हैं।
-
अनेक पाश्चात्य-चिन्तकों ने भी इस एकत्ववादी सत् की धारणा में आचारदर्शन की सम्भावना के प्रति शंका प्रकट की है। मेक्समूलर ने शाङ्करवेदान्त को एक कठोर एकत्ववाद की संज्ञा देकर उसमें आचार के मल्य का अधिक स्थान स्वीकार नहीं किया ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org