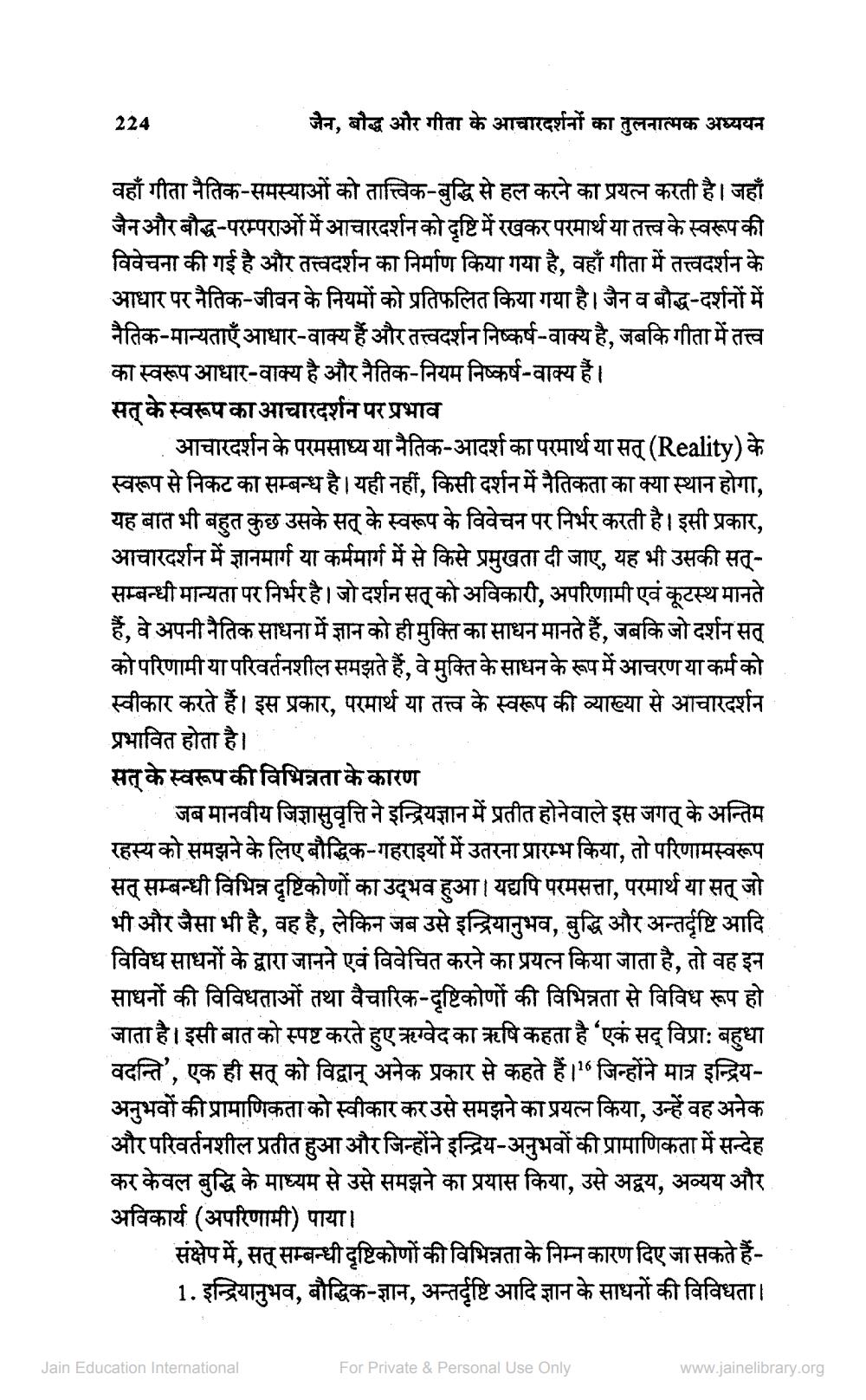________________
जैन, बौद्ध और गीता के आचारदर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन
वहाँ गीता नैतिक-समस्याओं को तात्त्विक-बुद्धि से हल करने का प्रयत्न करती है। जहाँ जैन और बौद्ध - परम्पराओं में आचारदर्शन को दृष्टि में रखकर परमार्थ या तत्त्व के स्वरूप की विवेचना की गई है और तत्त्वदर्शन का निर्माण किया गया है, वहाँ गीता में तत्त्वदर्शन के आधार पर नैतिक जीवन के नियमों को प्रतिफलित किया गया है। जैन व बौद्ध दर्शनों में नैतिक-मान्यताएँ आधार - वाक्य हैं और तत्त्वदर्शन निष्कर्ष - वाक्य है, जबकि गीता में तत्त्व का स्वरूप आधार - वाक्य है और नैतिक नियम निष्कर्ष - वाक्य हैं।
224
सत् के स्वरूप का आचारदर्शन पर प्रभाव
आचारदर्शन के परमसाध्य या नैतिक आदर्श का परमार्थ या सत् (Reality) के स्वरूप से निकट का सम्बन्ध है। यही नहीं, किसी दर्शन में नैतिकता का क्या स्थान होगा, यह बात भी बहुत कुछ उसके सत् के स्वरूप के विवेचन पर निर्भर करती है। इसी प्रकार, आचारदर्शन में ज्ञानमार्ग या कर्ममार्ग में से किसे प्रमुखता दी जाए, यह भी उसकी सत् - सम्बन्धी मान्यता पर निर्भर है। जो दर्शन सत् को अविकारी, अपरिणामी एवं कूटस्थ मानते हैं, वे अपनी नैतिक साधना में ज्ञान को ही मुक्ति का साधन मानते हैं, जबकि जो दर्शन सत् को परिणामी या परिवर्तनशील समझते हैं, वे मुक्ति के साधन के रूप में आचरण या कर्म को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार, परमार्थ या तत्त्व के स्वरूप की व्याख्या से आचारदर्शन प्रभावित होता है।
सत् के स्वरूप की विभिन्नता के कारण
जब मानवीय जिज्ञासुवृत्ति ने इन्द्रियज्ञान में प्रतीत होनेवाले इस जगत् के अन्तिम रहस्य को समझने के लिए बौद्धिक गहराइयों में उतरना प्रारम्भ किया, तो परिणामस्वरूप सत् सम्बन्धी विभिन्न दृष्टिकोणों का उद्भव हुआ। यद्यपि परमसत्ता, परमार्थ या सत् जो भी और जैसा भी है, वह है, लेकिन जब उसे इन्द्रियानुभव, बुद्धि और अन्तर्दृष्टि आदि विविध साधनों के द्वारा जानने एवं विवेचित करने का प्रयत्न किया जाता है, तो वह इन साधनों की विविधताओं तथा वैचारिक दृष्टिकोणों की विभिन्नता से विविध रूप हो जाता है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए ऋग्वेद का ऋषि कहता है 'एकं सद् विप्राः बहुधा वदन्ति', एक ही सत् को विद्वान् अनेक प्रकार से कहते हैं । " जिन्होंने मात्र इन्द्रियअनुभवों की प्रामाणिकता को स्वीकार कर उसे समझने का प्रयत्न किया, उन्हें वह अनेक और परिवर्तनशील प्रतीत हुआ और जिन्होंने इन्द्रिय- अनुभवों की प्रामाणिकता में सन्देह कर केवल बुद्धि के माध्यम से उसे समझने का प्रयास किया, उसे अद्वय, अव्यय और अविकार्य (अपरिणामी ) पाया।
-
संक्षेप में, सत् सम्बन्धी दृष्टिकोणों की विभिन्नता के निम्न कारण दिए जा सकते हैं1. इन्द्रियानुभव, बौद्धिक- ज्ञान, अन्तर्दृष्टि आदि ज्ञान के साधनों की विविधता ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org