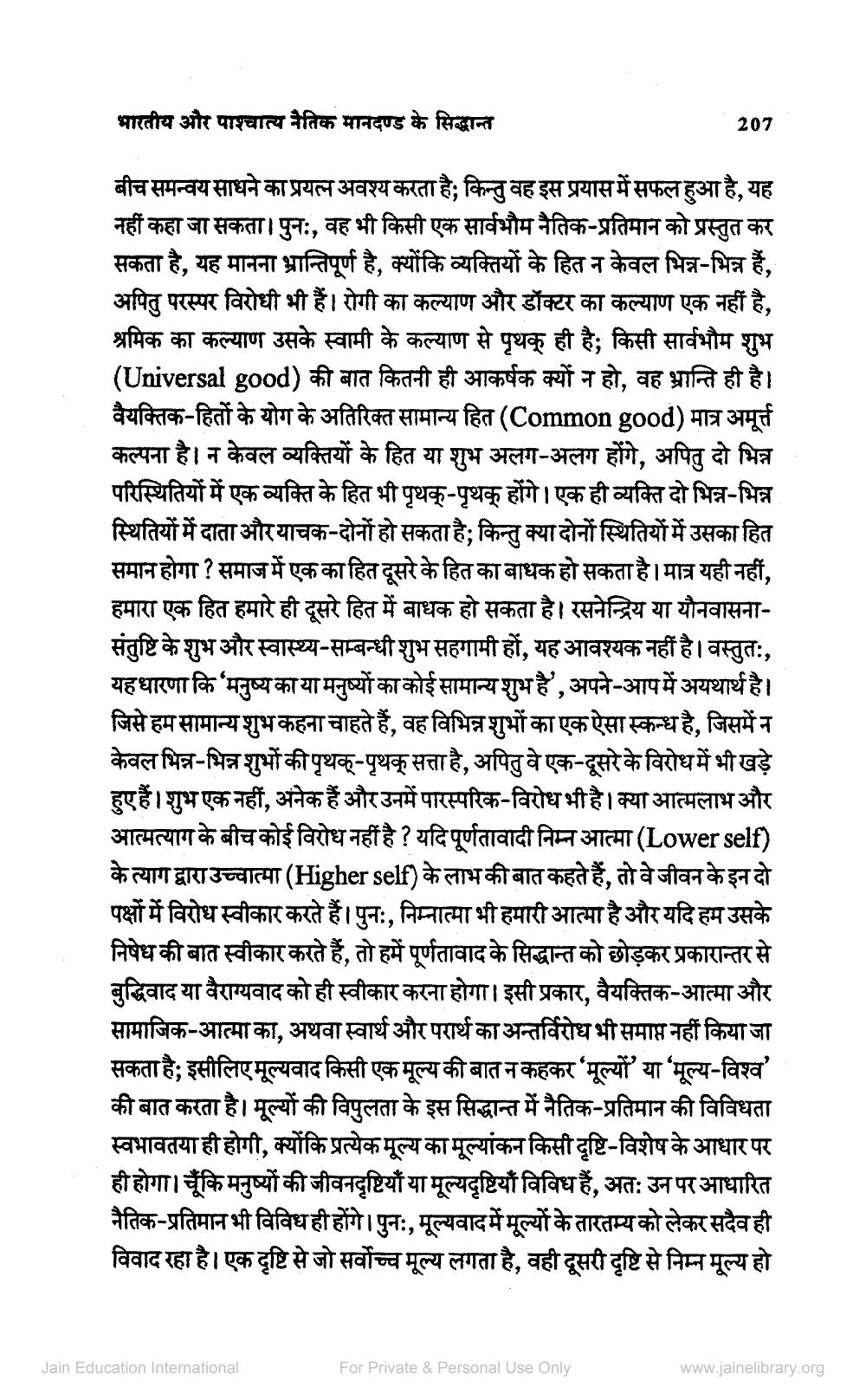________________
भारतीय और पाश्चात्य नैतिक मानदण्ड के सिद्धान्त
बीच समन्वय साधने का प्रयत्न अवश्य करता है; किन्तु वह इस प्रयास में सफल हुआ है, यह नहीं कहा जा सकता । पुनः, वह भी किसी एक सार्वभौम नैतिक- प्रतिमान को प्रस्तुत कर सकता है, यह मानना भ्रान्तिपूर्ण है, क्योंकि व्यक्तियों के हित न केवल भिन्न-भिन्न हैं, अपितु परस्पर विरोधी भी हैं। रोगी का कल्याण और डॉक्टर का कल्याण एक नहीं है, श्रमिक का कल्याण उसके स्वामी के कल्याण से पृथक् ही है; किसी सार्वभौम शुभ (Universal good) की बात कितनी ही आकर्षक क्यों न हो, वह भ्रान्ति ही है । वैयक्तिक हितों के योग के अतिरिक्त सामान्य हित (Common good) मात्र अमूर्त कल्पना है। न केवल व्यक्तियों के हित या शुभ अलग-अलग होंगे, अपितु दो भिन्न परिस्थितियों में एक व्यक्ति के हित भी पृथक्-पृथक् होंगे। एक ही व्यक्ति दो भिन्न-भिन्न स्थितियों में दाता और याचक- दोनों हो सकता है; किन्तु क्या दोनों स्थितियों में उसका हित समान होगा ? समाज में एक का हित दूसरे के हित का बाधक हो सकता है। मात्र यही नहीं, हमारा एक हित हमारे ही दूसरे हित में बाधक हो सकता है। रसनेन्द्रिय या यौनवासनासंतुष्टि के शुभ और स्वास्थ्य सम्बन्धी शुभ सहगामी हों, यह आवश्यक नहीं है। वस्तुतः, यह धारणा कि 'मनुष्य का या मनुष्यों का कोई सामान्य शुभ है', अपने-आप में अयथार्थ है । जिसे हम सामान्य शुभ कहना चाहते हैं, वह विभिन्न शुभों का एक ऐसा स्कन्ध है, जिसमें न केवल भिन्न-भिन्न शुभों की पृथक्-पृथक् सत्ता है, अपितु वे एक-दूसरे के विरोध में भी खड़े हुए हैं। शुभ एक नहीं, अनेक हैं और उनमें पारस्परिक-विरोध भी है। क्या आत्मलाभ और आत्मत्याग के बीच कोई विरोध नहीं है ? यदि पूर्णतावादी निम्न आत्मा (Lower self) के त्याग द्वारा उच्चात्मा (Higher self) के लाभ की बात कहते हैं, तो वे जीवन के इन दो पक्षों में विरोध स्वीकार करते हैं। पुनः, निम्नात्मा भी हमारी आत्मा है और यदि हम उसके निषेध की बात स्वीकार करते हैं, तो हमें पूर्णतावाद के सिद्धान्त को छोड़कर प्रकारान्तर से बुद्धिवाद या वैराग्यवाद को ही स्वीकार करना होगा। इसी प्रकार, वैयक्तिक - आत्मा और सामाजिक- आत्मा का अथवा स्वार्थ और परार्थ का अन्तर्विरोध भी समाप्त नहीं किया जा सकता है; इसीलिए मूल्यवाद किसी एक मूल्य की बात न कहकर 'मूल्यों' या 'मूल्य - विश्व' की बात करता है। मूल्यों की विपुलता के इस सिद्धान्त में नैतिक- प्रतिमान की विविधता स्वभावतया ही होगी, क्योंकि प्रत्येक मूल्य का मूल्यांकन किसी दृष्टि-विशेष के आधार पर
होगा। चूँकि मनुष्यों की जीवनदृष्टियाँ या मूल्यदृष्टियाँ विविध हैं, अतः उन पर आधारित नैतिक- प्रतिमान भी विविध ही होंगे। पुनः, मूल्यवाद में मूल्यों के तारतम्य को लेकर सदैव ही विवाद रहा है। एक दृष्टि से जो सर्वोच्च मूल्य लगता है, वही दूसरी दृष्टि से निम्न मूल्य हो
Jain Education International
-
For Private & Personal Use Only
207
www.jainelibrary.org