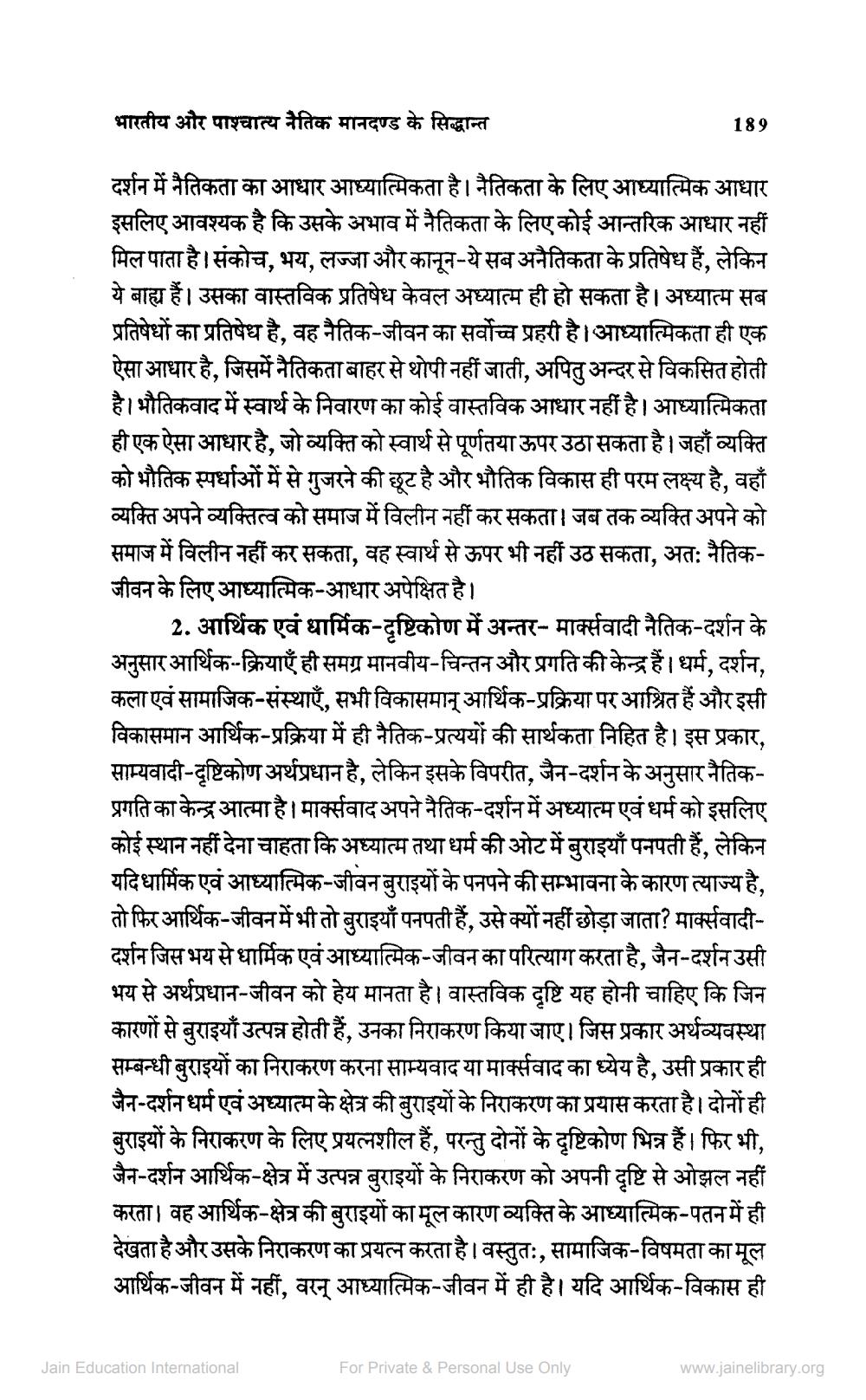________________
भारतीय और पाश्चात्य नैतिक मानदण्ड के सिद्धान्त
दर्शन में नैतिकता का आधार आध्यात्मिकता है। नैतिकता के लिए आध्यात्मिक आधार इसलिए आवश्यक है कि उसके अभाव में नैतिकता के लिए कोई आन्तरिक आधार नहीं मिल पाता है। संकोच, भय, लज्जा और कानून- ये सब अनैतिकता के प्रतिषेध हैं, लेकिन
बाह्य हैं। उसका वास्तविक प्रतिषेध केवल अध्यात्म ही हो सकता है। अध्यात्म सब प्रतिषेधों का प्रतिषेध है, वह नैतिक जीवन का सर्वोच्च प्रहरी है। आध्यात्मिकता ही एक ऐसा आधार है, जिसमें नैतिकता बाहर से थोपी नहीं जाती, अपितु अन्दर से विकसित होती है। भौतिकवाद में स्वार्थ के निवारण का कोई वास्तविक आधार नहीं है । आध्यात्मिकता
एक ऐसा आधार है, जो व्यक्ति को स्वार्थ से पूर्णतया ऊपर उठा सकता है। जहाँ व्यक्ति को भौतिक स्पर्धाओं में से गुजरने की छूट है और भौतिक विकास ही परम लक्ष्य है, वहाँ व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को समाज में विलीन नहीं कर सकता। जब तक व्यक्ति अपने को समाज में विलीन नहीं कर सकता, वह स्वार्थ से ऊपर भी नहीं उठ सकता, अत: नैतिकजीवन के लिए आध्यात्मिक आधार अपेक्षित है ।
-
2. आर्थिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण में अन्तर - मार्क्सवादी नैतिक-दर्शन के अनुसार आर्थिक--क्रियाएँ ही समग्र मानवीय चिन्तन और प्रगति की केन्द्र हैं । धर्म, दर्शन, कला एवं सामाजिक संस्थाएँ, सभी विकासमान् आर्थिक- प्रक्रिया पर आश्रित हैं और इसी विकासमान आर्थिक प्रक्रिया में ही नैतिक-प्रत्ययों की सार्थकता निहित है। इस प्रकार, साम्यवादी दृष्टिकोण अर्थप्रधान है, लेकिन इसके विपरीत, जैन दर्शन के अनुसार नैतिकप्रगति का केन्द्र आत्मा है। मार्क्सवाद अपने नैतिक-दर्शन में अध्यात्म एवं धर्म को इसलिए कोई स्थान नहीं देना चाहता कि अध्यात्म तथा धर्म की ओट में बुराइयाँ पनपती हैं, लेकिन यदिधार्मिक एवं आध्यात्मिक जीवन बुराइयों के पनपने की सम्भावना के कारण त्याज्य है, तो फिर आर्थिक जीवन में भी तो बुराइयाँ पनपती हैं, उसे क्यों नहीं छोड़ा जाता ? मार्क्सवादीदर्शन जिस भय से धार्मिक एवं आध्यात्मिक जीवन का परित्याग करता है, जैन- दर्शन उसी भय से अर्थप्रधान-जीवन को हेय मानता है। वास्तविक दृष्टि यह होनी चाहिए कि जिन कारणों से बुराइयाँ उत्पन्न होती हैं, उनका निराकरण किया जाए। जिस प्रकार अर्थव्यवस्था सम्बन्धी बुराइयों का निराकरण करना साम्यवाद या मार्क्सवाद का ध्येय है, उसी प्रकार ही जैन - दर्शन धर्म एवं अध्यात्म के क्षेत्र की बुराइयों के निराकरण का प्रयास करता है। दोनों ही बुराइयों के निराकरण के लिए प्रयत्नशील हैं, परन्तु दोनों के दृष्टिकोण भिन्न हैं। फिर भी, जैन-दर्शन आर्थिक-क्षेत्र में उत्पन्न बुराइयों के निराकरण को अपनी दृष्टि से ओझल नहीं करता। वह आर्थिक क्षेत्र की बुराइयों का मूल कारण व्यक्ति के आध्यात्मिक-पतन में ही देखता है और उसके निराकरण का प्रयत्न करता है। वस्तुतः, सामाजिक विषमता का मूल आर्थिक जीवन में नहीं, वरन् आध्यात्मिक जीवन में ही है । यदि आर्थिक विकास ही
Jain Education International
-
189
-
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org