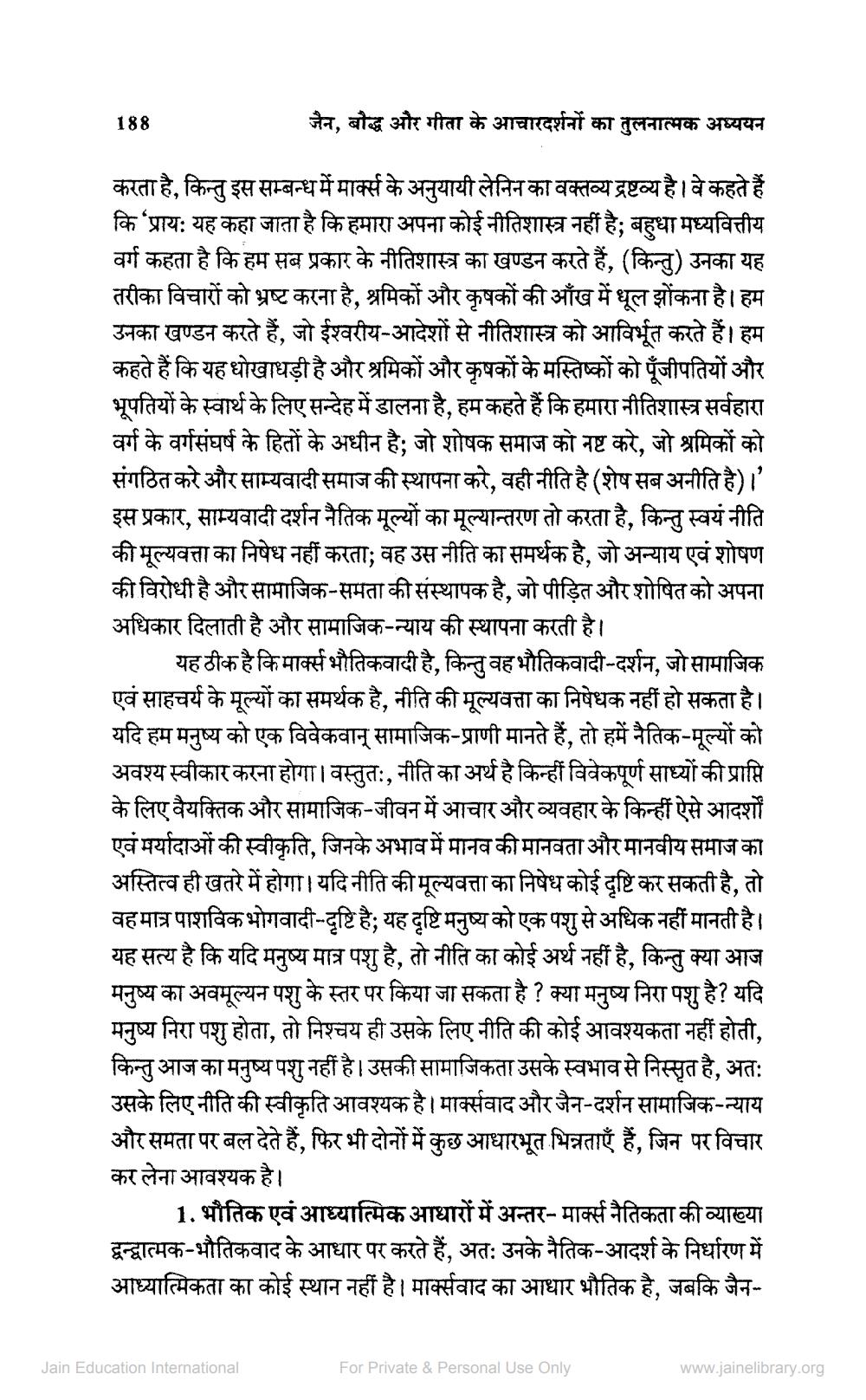________________
जैन, बौद्ध और गीता के आचारदर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन
करता है, किन्तु इस सम्बन्ध में मार्क्स के अनुयायी लेनिन का वक्तव्य द्रष्टव्य है। वे कहते हैं कि 'प्राय: यह कहा जाता है कि हमारा अपना कोई नीतिशास्त्र नहीं है; बहुधा मध्यवित्तीय वर्ग कहता है कि हम सब प्रकार के नीतिशास्त्र का खण्डन करते हैं, (किन्तु) उनका यह तरीका विचारों को भ्रष्ट करना है, श्रमिकों और कृषकों की आँख में धूल झोंकना है। हम उनका खण्डन करते हैं, जो ईश्वरीय-आदेशों से नीतिशास्त्र को आविर्भूत करते हैं। हम कहते हैं कि यह धोखाधड़ी है और श्रमिकों और कृषकों के मस्तिष्कों को पूँजीपतियों और भूपतियों के स्वार्थ के लिए सन्देह में डालना है, हम कहते हैं कि हमारा नीतिशास्त्र सर्वहारा वर्ग के वर्गसंघर्ष के हितों के अधीन है; जो शोषक समाज को नष्ट करे, जो श्रमिकों को संगठित करे और साम्यवादी समाज की स्थापना करे, वही नीति है ( शेष सब अनीति है ) । ' इस प्रकार, साम्यवादी दर्शन नैतिक मूल्यों का मूल्यान्तरण तो करता है, किन्तु स्वयं नीति की मूल्यवत्ता का निषेध नहीं करता; वह उस नीति का समर्थक है, जो अन्याय एवं शोषण की विरोधी है और सामाजिक समता की संस्थापक है, जो पीड़ित और शोषित को अपना अधिकार दिलाती है और सामाजिक न्याय की स्थापना करती है ।
188
-
यह ठीक है कि मार्क्स भौतिकवादी है, किन्तु वह भौतिकवादी दर्शन, जो सामाजिक एवं साहचर्य के मूल्यों का समर्थक है, नीति की मूल्यवत्ता का निषेधक नहीं हो सकता है। यदि हम मनुष्य को एक विवेकवान् सामाजिक प्राणी मानते हैं, तो हमें नैतिक मूल्यों को अवश्य स्वीकार करना होगा । वस्तुतः, नीति का अर्थ है किन्हीं विवेकपूर्ण साध्यों की प्राप्ति के लिए वैयक्तिक और सामाजिक-जीवन में आचार और व्यवहार के किन्हीं ऐसे आदर्शों एवं मर्यादाओं की स्वीकृति, जिनके अभाव में मानव की मानवता और मानवीय समाज का अस्तित्व ही खतरे में होगा। यदि नीति की मूल्यवत्ता का निषेध कोई दृष्टि कर सकती है, तो वह मात्र पाशविक भोगवादी दृष्टि है; यह दृष्टि मनुष्य को एक पशु से अधिक नहीं मानती है। यह सत्य है कि यदि मनुष्य मात्र पशु है, तो नीति का कोई अर्थ नहीं है, किन्तु क्या आज मनुष्य का अवमूल्यन पशु के स्तर पर किया जा सकता है ? क्या मनुष्य निरा पशु है? यदि मनुष्य निरा पशु होता, तो निश्चय ही उसके लिए नीति की कोई आवश्यकता नहीं होती, किन्तु आज का मनुष्य पशु नहीं है। उसकी सामाजिकता उसके स्वभाव से निस्सृत है, अतः उसके लिए नीति की स्वीकृति आवश्यक है। मार्क्सवाद और जैन दर्शन सामाजिक न्याय और समता पर बल देते हैं, फिर भी दोनों में कुछ आधारभूत भिन्नताएँ हैं, जिन पर विचार कर लेना आवश्यक है ।
-
-
1. भौतिक एवं आध्यात्मिक आधारों में अन्तर मार्क्स नैतिकता की व्याख्या द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद के आधार पर करते हैं, अतः उनके नैतिक आदर्श के निर्धारण में आध्यात्मिकता का कोई स्थान नहीं है। मार्क्सवाद का आधार भौतिक है, जबकि जैन
-
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
-
www.jainelibrary.org