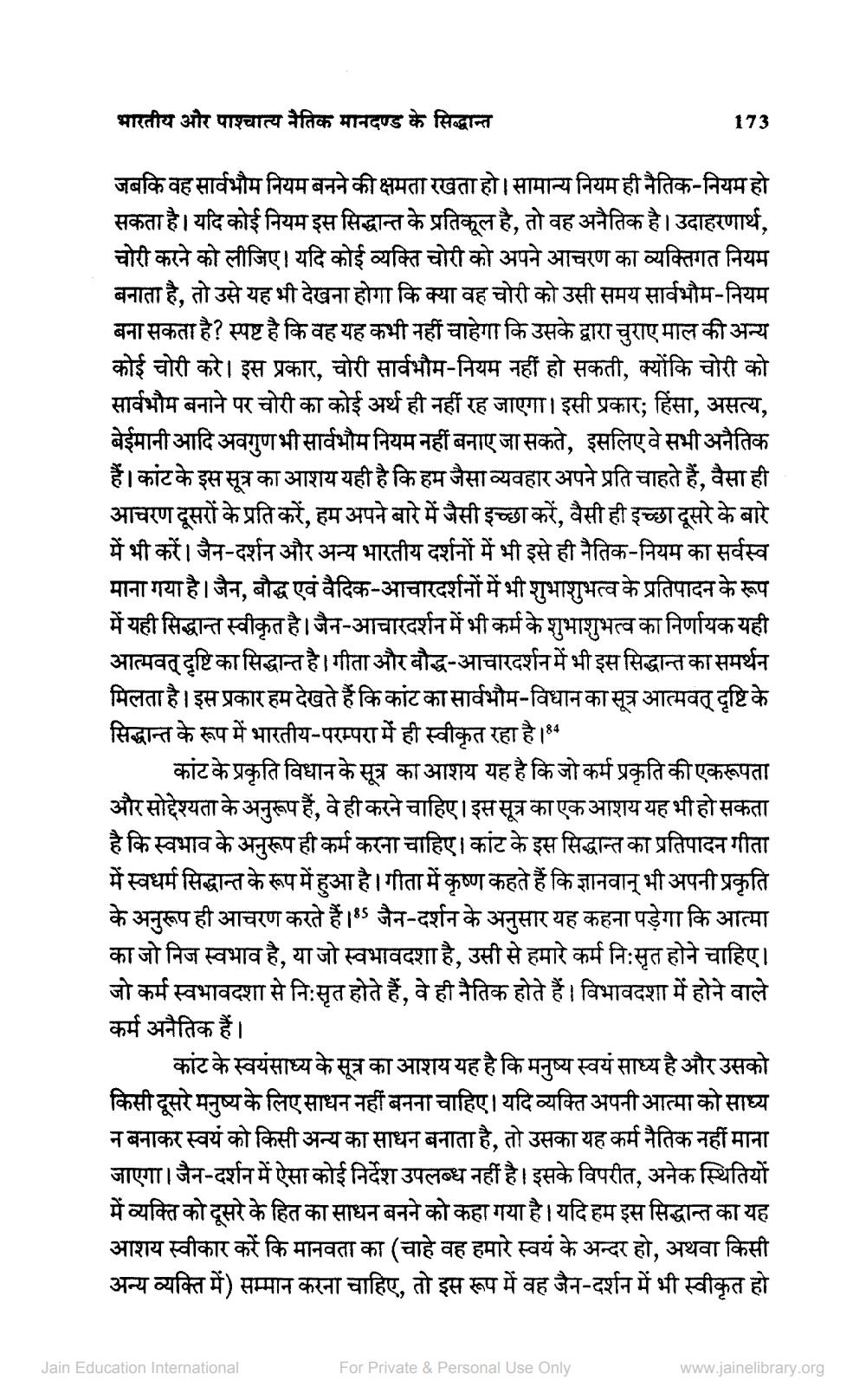________________
भारतीय और पाश्चात्य नैतिक मानदण्ड के सिद्धान्त
जबकि वह सार्वभौम नियम बनने की क्षमता रखता हो। सामान्य नियम ही नैतिक नियम हो सकता है। यदि कोई नियम इस सिद्धान्त के प्रतिकूल है, तो वह अनैतिक है। उदाहरणार्थ, चोरी करने को लीजिए। यदि कोई व्यक्ति चोरी को अपने आचरण का व्यक्तिगत नियम बनाता है, तो उसे यह भी देखना होगा कि क्या वह चोरी को उसी समय सार्वभौम-नियम बना सकता है? स्पष्ट है कि वह यह कभी नहीं चाहेगा कि उसके द्वारा चुराए माल की अन्य कोई चोरी करे। इस प्रकार, चोरी सार्वभौम-नियम नहीं हो सकती, क्योंकि चोरी को सार्वभौम बनाने पर चोरी का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। इसी प्रकार, हिंसा, असत्य, बेईमानी आदि अवगुण भी सार्वभौम नियम नहीं बनाए जा सकते, इसलिए वे सभी अनैतिक हैं। इस सूत्र का आशय यही है कि हम जैसा व्यवहार अपने प्रति चाहते हैं, वैसा ही आचरण दूसरों के प्रति करें, हम अपने बारे में जैसी इच्छा करें, वैसी ही इच्छा दूसरे के बारे में भी करें। जैन दर्शन और अन्य भारतीय दर्शनों में भी इसे ही नैतिक-नियम का सर्वस्व माना गया है। जैन, बौद्ध एवं वैदिक- आचारदर्शनों में भी शुभाशुभत्व के प्रतिपादन के रूप में यही सिद्धान्त स्वीकृत है । जैन आचारदर्शन में भी कर्म के शुभाशुभत्व का निर्णायक यही आत्मवत् दृष्टि का सिद्धान्त है। गीता और बौद्ध - आचारदर्शन में भी इस सिद्धान्त का समर्थन मिलता है । इस प्रकार हम देखते हैं कि कांट का सार्वभौम-विधान का सूत्र आत्मवत् दृष्टि के सिद्धान्त के रूप में भारतीय परम्परा में ही स्वीकृत रहा है। 84
T
hi के प्रकृति विधान के सूत्र का आशय यह है कि जो कर्म प्रकृति की एकरूपता और सोद्देश्यता के अनुरूप हैं, वे ही करने चाहिए। इस सूत्र का एक आशय यह भी हो सकता है कि स्वभाव के अनुरूप ही कर्म करना चाहिए। कांट के इस सिद्धान्त का प्रतिपादन गीता में स्वधर्म सिद्धान्त के रूप में हुआ है। गीता में कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानवान् भी अपनी प्रकृति के अनुरूप ही आचरण करते हैं। 5 जैन दर्शन के अनुसार यह कहना पड़ेगा कि आत्मा Tata स्वभाव है, या जो स्वभावदशा है, उसी से हमारे कर्म निःसृत होने चाहिए। कर्म स्वभाव से निःसृत होते हैं, वे ही नैतिक होते हैं। विभावदशा में होने वाले कर्म अनैतिक हैं।
-
कांट के स्वयंसाध्य के सूत्र का आशय यह है कि मनुष्य स्वयं साध्य है और उसको किसी दूसरे मनुष्य के लिए साधन नहीं बनना चाहिए। यदि व्यक्ति अपनी आत्मा को साध्य न बनाकर स्वयं को किसी अन्य का साधन बनाता है, तो उसका यह कर्म नैतिक नहीं माना जाएगा। जैन दर्शन में ऐसा कोई निर्देश उपलब्ध नहीं है। इसके विपरीत, अनेक स्थितियों
व्यक्ति को दूसरे के हित का साधन बनने को कहा गया है। यदि हम इस सिद्धान्त का यह आशय स्वीकार करें कि मानवता का (चाहे वह हमारे स्वयं के अन्दर हो, अथवा किसी अन्य व्यक्ति में) सम्मान करना चाहिए, तो इस रूप में वह जैन-दर्शन में भी स्वीकृत हो
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
173
www.jainelibrary.org