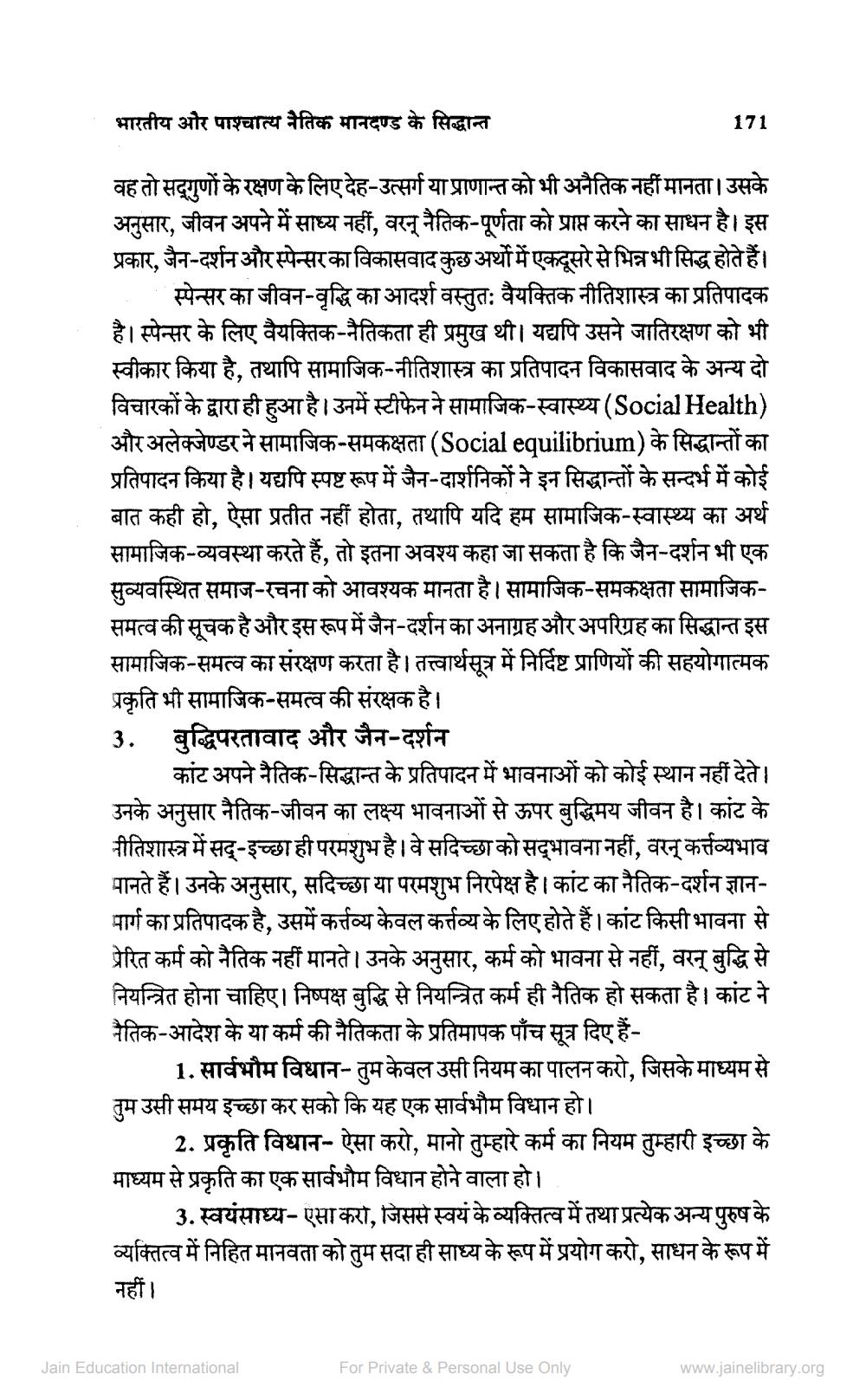________________
भारतीय और पाश्चात्य नैतिक मानदण्ड के सिद्धान्त
वह तो सद्गुणों के रक्षण के लिए देह - उत्सर्ग या प्राणान्त को भी अनैतिक नहीं मानता। उसके अनुसार, जीवन अपने में साध्य नहीं, वरनू नैतिक- पूर्णता को प्राप्त करने का साधन है। इस प्रकार, जैन-दर्शन और स्पेन्सर का विकासवाद कुछ अर्थो में एकदूसरे से भिन्न भी सिद्ध होते हैं। स्पेन्सर का जीवन-वृद्धि का आदर्श वस्तुतः वैयक्तिक नीतिशास्त्र का प्रतिपादक है। स्पेन्सर के लिए वैयक्तिक - नैतिकता ही प्रमुख थी । यद्यपि उसने जातिरक्षण को भी स्वीकार किया है, तथापि सामाजिक नीतिशास्त्र का प्रतिपादन विकासवाद के अन्य दो विचारकों के द्वारा ही हुआ है। उनमें स्टीफेन ने सामाजिक-स्वास्थ्य (Social Health) और अलेक्जेण्डर ने सामाजिक-समकक्षता (Social equilibrium) के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। यद्यपि स्पष्ट रूप में जैन- दार्शनिकों ने इन सिद्धान्तों के सन्दर्भ में कोई बात कही हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता, तथापि यदि हम सामाजिक स्वास्थ्य का अर्थ सामाजिक व्यवस्था करते हैं, तो इतना अवश्य कहा जा सकता है कि जैन-दर्शन भी एक सुव्यवस्थित समाज - रचना को आवश्यक मानता है। सामाजिक-स 5- समकक्षता सामाजिकसमत्व की सूचक है और इस रूप में जैन दर्शन का अनाग्रह और अपरिग्रह का सिद्धान्त इस सामाजिक समत्व का संरक्षण करता है । तत्त्वार्थसूत्र में निर्दिष्ट प्राणियों की सहयोगात्मक प्रकृति भी सामाजिक-स 5- समत्व की संरक्षक है ।
-
3.
बुद्धिपरतावाद और जैन दर्शन
कांट अपने नैतिक सिद्धान्त के प्रतिपादन में भावनाओं को कोई स्थान नहीं देते। उनके अनुसार नैतिक जीवन का लक्ष्य भावनाओं से ऊपर बुद्धिमय जीवन है। कांट के नीतिशास्त्र में सद्-इच्छा ही परमशुभ है । वे सदिच्छा को सद्भावना नहीं, वरन् कर्त्तव्यभाव मानते हैं। उनके अनुसार, सदिच्छा या परमशुभ निरपेक्ष है। कांट का नैतिक-दर्शन ज्ञानमार्ग का प्रतिपादक है, उसमें कर्त्तव्य केवल कर्त्तव्य के लिए होते हैं। कांट किसी भावना से प्रेरित कर्म को नैतिक नहीं मानते। उनके अनुसार, कर्म को भावना से नहीं, वरन् बुद्धि से नियन्त्रित होना चाहिए। निष्पक्ष बुद्धि से नियन्त्रित कर्म ही नैतिक हो सकता है। कांट ने नैतिक- आदेश के या कर्म की नैतिकता के प्रतिमापक पाँच सूत्र दिए हैं
--
171
1. सार्वभौम विधान - तुम केवल उसी नियम का पालन करो, जिसके माध्यम से तुम उसी समय इच्छा कर सको कि यह एक सार्वभौम विधान हो ।
2. प्रकृति विधान - ऐसा करो, मानो तुम्हारे कर्म का नियम तुम्हारी इच्छा के माध्यम से प्रकृति का एक सार्वभौम विधान होने वाला हो ।
3. स्वयंसाध्य - एसा करो, जिससे स्वयं के व्यक्तित्व में तथा प्रत्येक अन्य पुरुष के व्यक्तित्व में निहित मानवता को तुम सदा ही साध्य के रूप में प्रयोग करो, साधन के रूप में
नहीं ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org