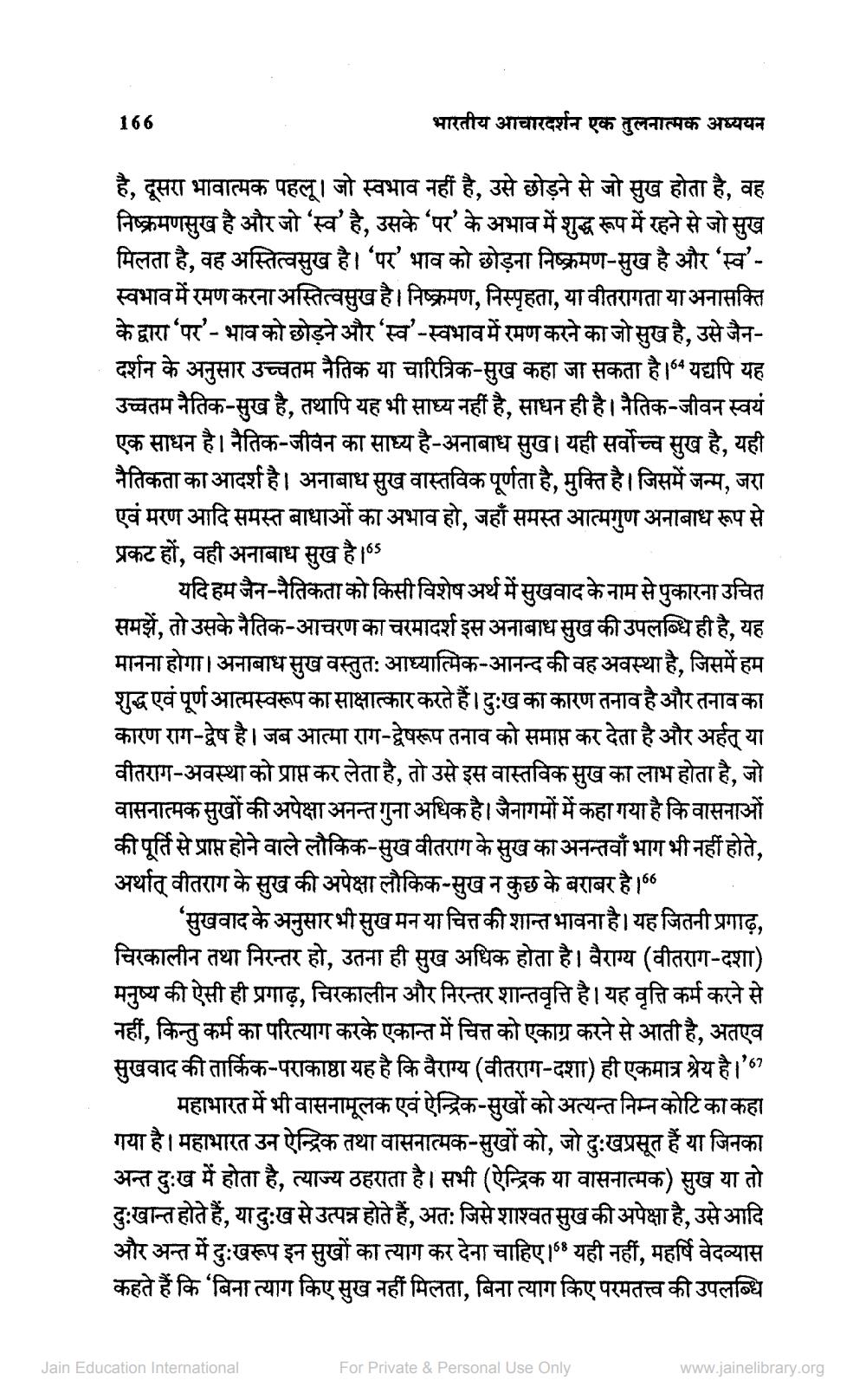________________
166
भारतीय आचारदर्शन एक तुलनात्मक अध्ययन
है, दूसरा भावात्मक पहलू। जो स्वभाव नहीं है, उसे छोड़ने से जो सुख होता है, वह निष्क्रमणसुख है और जो 'स्व' है, उसके 'पर' के अभाव में शुद्ध रूप में रहने से जो सुख मिलता है, वह अस्तित्वसुख है। 'पर' भाव को छोड़ना निष्क्रमण-सुख है और 'स्व'स्वभाव में रमण करना अस्तित्वसुख है। निष्क्रमण, निस्पृहता, या वीतरागता या अनासक्ति के द्वारा पर'- भाव को छोड़ने और 'स्व'-स्वभावमें रमण करने का जो सुख है, उसे जैनदर्शन के अनुसार उच्चतम नैतिक या चारित्रिक-सुख कहा जा सकता है। यद्यपि यह उच्चतम नैतिक-सुख है, तथापि यह भी साध्य नहीं है, साधन ही है। नैतिक-जीवन स्वयं एक साधन है। नैतिक-जीवन का साध्य है-अनाबाध सुख। यही सर्वोच्च सुख है, यही नैतिकता का आदर्श है। अनाबाध सुख वास्तविक पूर्णता है, मुक्ति है। जिसमें जन्म, जरा एवं मरण आदि समस्त बाधाओं का अभाव हो, जहाँ समस्त आत्मगुण अनाबाध रूप से प्रकट हों, वही अनाबाध सुख है।
यदि हम जैन-नैतिकता को किसी विशेष अर्थ में सुखवाद के नाम से पुकारना उचित समझें, तो उसके नैतिक-आचरण का चरमादर्श इस अनाबाध सुख की उपलब्धि ही है, यह मानना होगा। अनाबाध सुख वस्तुत: आध्यात्मिक-आनन्द की वह अवस्था है, जिसमें हम शुद्ध एवं पूर्ण आत्मस्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। दुःख का कारण तनाव है और तनाव का कारण राग-द्वेष है। जब आत्मा राग-द्वेषरूप तनाव को समाप्त कर देता है और अर्हत् या वीतराग-अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तो उसे इस वास्तविक सुख का लाभ होता है, जो वासनात्मक सुखों की अपेक्षाअनन्त गुना अधिक है। जैनागमों में कहा गया है कि वासनाओं की पूर्ति से प्राप्त होने वाले लौकिक-सुख वीतराग के सुख का अनन्तवाँ भाग भी नहीं होते, अर्थात् वीतराग के सुख की अपेक्षा लौकिक-सुख न कुछ के बराबर है।66
'सुखवाद के अनुसार भी सुख मन या चित्त की शान्तभावना है। यह जितनी प्रगाढ़, चिरकालीन तथा निरन्तर हो, उतना ही सुख अधिक होता है। वैराग्य (वीतराग-दशा) मनुष्य की ऐसी ही प्रगाढ़, चिरकालीन और निरन्तर शान्तवृत्ति है। यह वृत्ति कर्म करने से नहीं, किन्तु कर्म का परित्याग करके एकान्त में चित्त को एकाग्र करने से आती है, अतएव सुखवाद की तार्किक-पराकाष्ठा यह है कि वैराग्य (वीतराग-दशा) ही एकमात्र श्रेय है।'67
महाभारत में भी वासनामूलक एवं ऐन्द्रिक-सुखों को अत्यन्त निम्न कोटि का कहा गया है। महाभारत उन ऐन्द्रिक तथा वासनात्मक-सुखों को, जो दुःखप्रसूत हैं या जिनका अन्त दुःख में होता है, त्याज्य ठहराता है। सभी (ऐन्द्रिक या वासनात्मक) सुख या तो दुःखान्त होते हैं, यादुःख से उत्पन्न होते हैं, अत: जिसे शाश्वत सुख की अपेक्षा है, उसे आदि
और अन्त में दुःखरूप इन सुखों का त्याग कर देना चाहिए। यही नहीं, महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि 'बिना त्याग किए सुख नहीं मिलता, बिना त्याग किए परमतत्त्व की उपलब्धि
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org