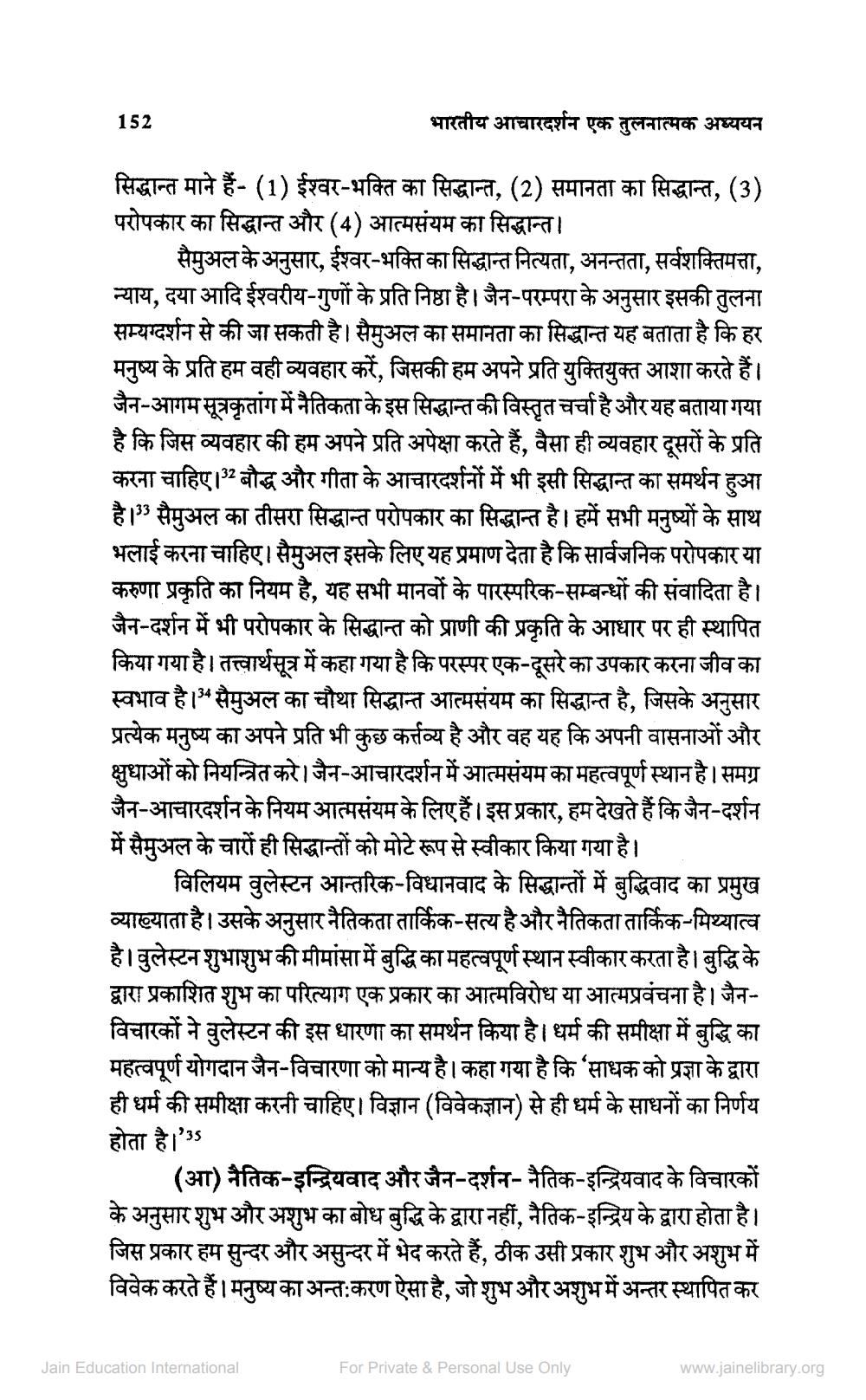________________
152
भारतीय आचारदर्शन एक तुलनात्मक अध्ययन
सिद्धान्त माने हैं- (1) ईश्वर-भक्ति का सिद्धान्त, (2) समानता का सिद्धान्त, (3) परोपकार का सिद्धान्त और (4) आत्मसंयम का सिद्धान्त।
सैमुअल के अनुसार, ईश्वर-भक्ति का सिद्धान्त नित्यता, अनन्तता, सर्वशक्तिमत्ता, न्याय, दया आदि ईश्वरीय-गुणों के प्रति निष्ठा है। जैन-परम्परा के अनुसार इसकी तुलना सम्यग्दर्शन से की जा सकती है। सैमुअल का समानता का सिद्धान्त यह बताता है कि हर मनुष्य के प्रति हम वही व्यवहार करें, जिसकी हम अपने प्रति युक्तियुक्त आशा करते हैं। जैन-आगमसूत्रकृतांग में नैतिकता के इस सिद्धान्त की विस्तृत चर्चा है और यह बताया गया है कि जिस व्यवहार की हम अपने प्रति अपेक्षा करते हैं, वैसा ही व्यवहार दूसरों के प्रति करना चाहिए। बौद्ध और गीता के आचारदर्शनों में भी इसी सिद्धान्त का समर्थन हुआ है। सैमुअल का तीसरा सिद्धान्त परोपकार का सिद्धान्त है। हमें सभी मनुष्यों के साथ भलाई करना चाहिए। सैमुअल इसके लिए यह प्रमाण देता है कि सार्वजनिक परोपकार या करुणा प्रकृति का नियम है, यह सभी मानवों के पारस्परिक सम्बन्धों की संवादिता है। जैन-दर्शन में भी परोपकार के सिद्धान्त को प्राणी की प्रकृति के आधार पर ही स्थापित किया गया है। तत्त्वार्थसूत्र में कहा गया है कि परस्पर एक-दूसरे का उपकार करना जीव का स्वभाव है। सैमुअल का चौथा सिद्धान्त आत्मसंयम का सिद्धान्त है, जिसके अनुसार प्रत्येक मनुष्य का अपने प्रति भी कुछ कर्तव्य है और वह यह कि अपनी वासनाओं और क्षुधाओं को नियन्त्रित करे। जैन-आचारदर्शन में आत्मसंयम का महत्वपूर्ण स्थान है। समग्र जैन-आचारदर्शन के नियम आत्मसंयम के लिए हैं। इस प्रकार, हम देखते हैं कि जैन-दर्शन में सैमुअल के चारों ही सिद्धान्तों को मोटे रूप से स्वीकार किया गया है।
विलियम वुलेस्टन आन्तरिक-विधानवाद के सिद्धान्तों में बुद्धिवाद का प्रमुख व्याख्याता है। उसके अनुसार नैतिकता तार्किक-सत्य है और नैतिकता तार्किक-मिथ्यात्व है। वुलेस्टन शुभाशुभ की मीमांसा में बुद्धि का महत्वपूर्ण स्थान स्वीकार करता है। बुद्धि के द्वारा प्रकाशित शुभ का परित्याग एक प्रकार का आत्मविरोध या आत्मप्रवंचना है। जैनविचारकों ने वुलेस्टन की इस धारणा का समर्थन किया है। धर्म की समीक्षा में बुद्धि का महत्वपूर्ण योगदान जैन-विचारणा को मान्य है। कहा गया है कि साधक को प्रज्ञा के द्वारा ही धर्म की समीक्षा करनी चाहिए। विज्ञान (विवेकज्ञान) से ही धर्म के साधनों का निर्णय होता है।'35
(आ) नैतिक-इन्द्रियवाद और जैन-दर्शन- नैतिक-इन्द्रियवाद के विचारकों के अनुसार शुभ और अशुभ का बोध बुद्धि के द्वारा नहीं, नैतिक-इन्द्रिय के द्वारा होता है। जिस प्रकार हम सुन्दर और असुन्दर में भेद करते हैं, ठीक उसी प्रकार शुभ और अशुभ में विवेक करते हैं। मनुष्य का अन्त:करण ऐसा है, जो शुभ और अशुभ में अन्तर स्थापित कर
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org