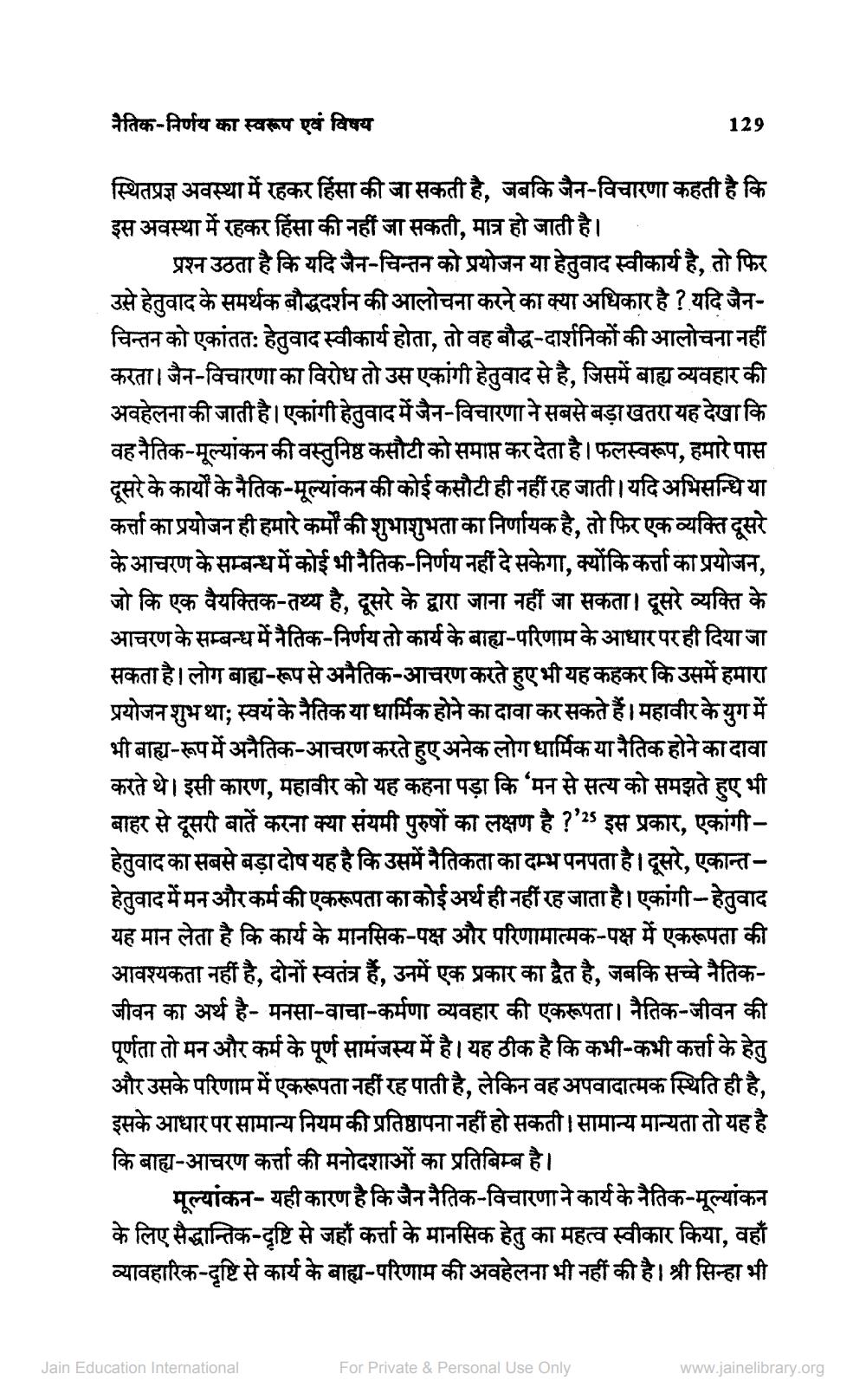________________
नैतिक निर्णय का स्वरूप एवं विषय
स्थितप्रज्ञ अवस्था में रहकर हिंसा की जा सकती है, जबकि जैन- विचारणा कहती है कि इस अवस्था में रहकर हिंसा की नहीं जा सकती, मात्र हो जाती है।
-
प्रश्न उठता है कि यदि जैन - चिन्तन को प्रयोजन या हेतुवाद स्वीकार्य है, तो फिर उसे हेतुवाद के समर्थक बौद्धदर्शन की आलोचना करने का क्या अधिकार है ? यदि जैनचिन्तन को एकांततः हेतुवाद स्वीकार्य होता, तो वह बौद्ध दार्शनिकों की आलोचना नहीं करता। जैन- विचारणा का विरोध तो उस एकांगी हेतुवाद से है, जिसमें बाह्य व्यवहार की अवहेलना की जाती है। एकांगी हेतुवाद में जैन- विचारणा ने सबसे बड़ा खतरा यह देखा कि वह नैतिक मूल्यांकन की वस्तुनिष्ठ कसौटी को समाप्त कर देता है। फलस्वरूप, हमारे पास दूसरे के कार्यों के नैतिक मूल्यांकन की कोई कसौटी ही नहीं रह जाती। यदि अभिसन्धिया कर्त्ता का प्रयोजन ही हमारे कर्मों की शुभाशुभता का निर्णायक है, तो फिर एक व्यक्ति दूसरे
आचरण के सम्बन्ध में कोई भी नैतिक निर्णय नहीं दे सकेगा, क्योंकि कर्त्ता का प्रयोजन, जो कि एक वैयक्तिक - तथ्य है, दूसरे के द्वारा जाना नहीं जा सकता। दूसरे व्यक्ति के आचरण के सम्बन्ध में नैतिक निर्णय तो कार्य के बाह्य परिणाम के आधार पर ही दिया जा सकता है। लोग बाह्य रूप से अनैतिक- आचरण करते हुए भी यह कहकर कि उसमें हमारा प्रयोजन शुभ था; स्वयं के नैतिक या धार्मिक होने का दावा कर सकते हैं। महावीर के युग में भी बाह्य-रूप में अनैतिक- आचरण करते हुए अनेक लोग धार्मिक या नैतिक होने का दावा करते थे। इसी कारण, महावीर को यह कहना पड़ा कि 'मन से सत्य को समझते हुए भी बाहर से दूसरी बातें करना क्या संयमी पुरुषों का लक्षण है ? 225 इस प्रकार, एकांगी
-
वाद का सबसे बड़ा दोष यह है कि उसमें नैतिकता का दम्भ पनपता है। दूसरे, एकान्तहेतुवाद में मन और कर्म की एकरूपता का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है। एकांगी - हेतुवाद यह मान लेता है कि कार्य के मानसिक पक्ष और परिणामात्मक-पक्ष में एकरूपता की आवश्यकता नहीं है, दोनों स्वतंत्र हैं, उनमें एक प्रकार का द्वैत है, जबकि सच्चे नैतिकजीवन का अर्थ है- मनसा-वाचा- - कर्मणा व्यवहार की एकरूपता । नैतिक जीवन की पूर्णता तो मन और कर्म के पूर्ण सामंजस्य में है। यह ठीक है कि कभी-कभी कर्ता के हेतु और उसके परिणाम में एकरूपता नहीं रह पाती है, लेकिन वह अपवादात्मक स्थिति ही है, इसके आधार पर सामान्य नियम की प्रतिष्ठापना नहीं हो सकती। सामान्य मान्यता तो यह है कि बाह्य- आचरण कर्ता की मनोदशाओं का प्रतिबिम्ब है।
मूल्यांकन- यही कारण है कि जैन नैतिक-विचारणा ने कार्य के नैतिक मूल्यांकन लिए सैद्धान्तिक दृष्टि से जहाँ कर्त्ता के मानसिक हेतु का महत्व स्वीकार किया, वहाँ व्यावहारिक दृष्टि से कार्य के बाह्य परिणाम की अवहेलना भी नहीं की है। श्री सिन्हा भी
Jain Education International
129
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org