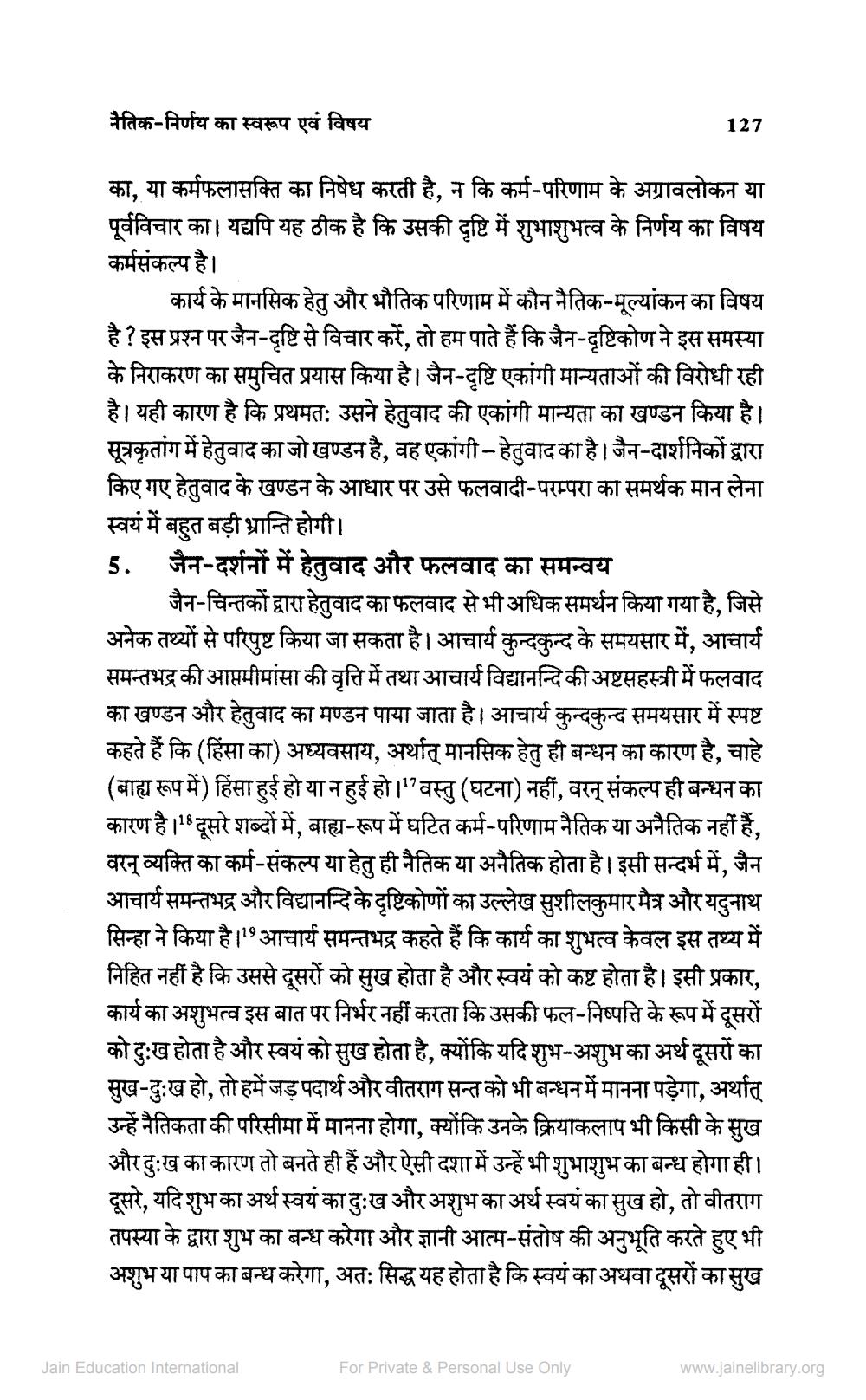________________
नैतिक-निर्णय का स्वरूप एवं विषय
127
का, या कर्मफलासक्ति का निषेध करती है, न कि कर्म-परिणाम के अग्रावलोकन या पूर्वविचार का। यद्यपि यह ठीक है कि उसकी दृष्टि में शुभाशुभत्व के निर्णय का विषय कर्मसंकल्प है।
__कार्य के मानसिक हेतु और भौतिक परिणाम में कौन नैतिक-मूल्यांकन का विषय है ? इस प्रश्न पर जैन-दृष्टि से विचार करें, तो हम पाते हैं कि जैन-दृष्टिकोण ने इस समस्या के निराकरण का समुचित प्रयास किया है। जैन-दृष्टि एकांगी मान्यताओं की विरोधी रही है। यही कारण है कि प्रथमत: उसने हेतुवाद की एकांगी मान्यता का खण्डन किया है। सूत्रकृतांग में हेतुवाद का जोखण्डन है, वह एकांगी-हेतुवाद का है। जैन-दार्शनिकों द्वारा किए गए हेतुवाद के खण्डन के आधार पर उसे फलवादी-परम्परा का समर्थक मान लेना स्वयं में बहुत बड़ी भ्रान्ति होगी। 5. जैन-दर्शनों में हेतुवाद और फलवाद का समन्वय
जैन-चिन्तकों द्वारा हेतुवाद का फलवाद से भी अधिक समर्थन किया गया है, जिसे अनेक तथ्यों से परिपुष्ट किया जा सकता है। आचार्य कुन्दकुन्द के समयसार में, आचार्य समन्तभद्र कीआप्तमीमांसा की वृत्ति में तथा आचार्य विद्यानन्दिकी अष्टसहस्त्री में फलवाद का खण्डन और हेतुवाद का मण्डन पाया जाता है। आचार्य कुन्दकुन्द समयसार में स्पष्ट कहते हैं कि (हिंसा का) अध्यवसाय, अर्थात् मानसिक हेतु ही बन्धन का कारण है, चाहे (बाह्य रूप में) हिंसा हुई हो या न हुई हो।"वस्तु (घटना) नहीं, वरन् संकल्प ही बन्धन का कारण है। दूसरे शब्दों में, बाह्य-रूप में घटित कर्म-परिणाम नैतिक या अनैतिक नहीं हैं. वरन व्यक्ति का कर्म-संकल्प या हेतु ही नैतिकया अनैतिक होता है। इसी सन्दर्भ में, जैन आचार्य समन्तभद्र और विद्यानन्दिके दृष्टिकोणों का उल्लेख सुशीलकुमार मैत्र और यदुनाथ सिन्हा ने किया है। आचार्य समन्तभद्र कहते हैं कि कार्य का शुभत्व केवल इस तथ्य में निहित नहीं है कि उससे दूसरों को सुख होता है और स्वयं को कष्ट होता है। इसी प्रकार, कार्य का अशुभत्व इस बात पर निर्भर नहीं करता कि उसकी फल-निष्पत्ति के रूप में दूसरों को दुःख होता है और स्वयं को सुख होता है, क्योंकि यदि शुभ-अशुभ का अर्थ दूसरों का सुख-दुःख हो, तो हमें जड़ पदार्थ और वीतराग सन्त को भी बन्धन में मानना पड़ेगा, अर्थात् उन्हें नैतिकता की परिसीमा में मानना होगा, क्योंकि उनके क्रियाकलाप भी किसी के सुख
और दुःख का कारण तो बनते ही हैं और ऐसी दशा में उन्हें भी शुभाशुभ का बन्ध होगा ही। दूसरे, यदिशुभ का अर्थ स्वयं का दुःख और अशुभ का अर्थ स्वयं का सुख हो, तो वीतराग तपस्या के द्वारा शुभ का बन्ध करेगा और ज्ञानी आत्म-संतोष की अनुभूति करते हुए भी अशुभ या पाप का बन्ध करेगा, अत: सिद्ध यह होता है कि स्वयं का अथवा दूसरों का सुख
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org