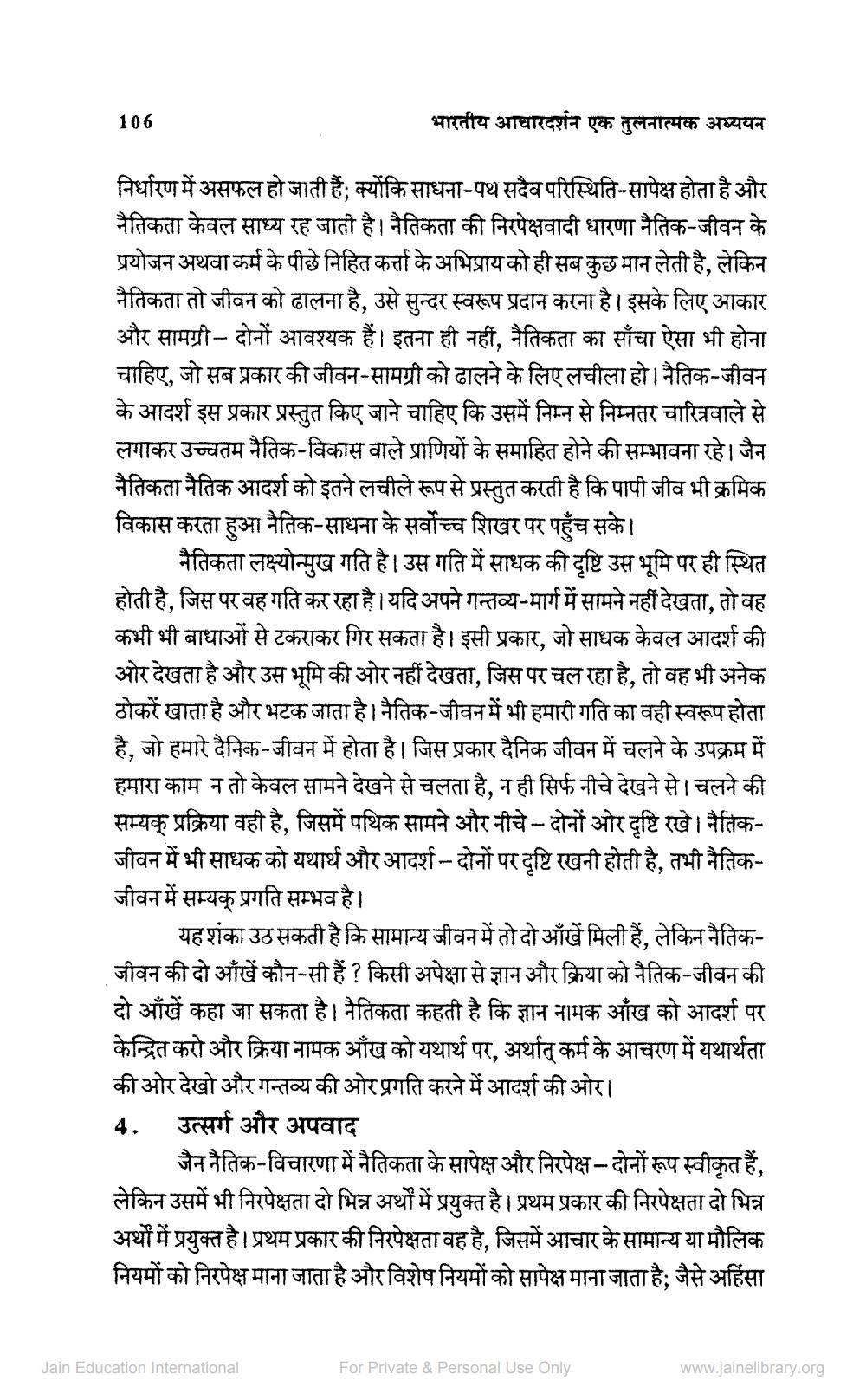________________
106
भारतीय आचारदर्शन एक तुलनात्मक अध्ययन
निर्धारण में असफल हो जाती हैं। क्योंकि साधना-पथ सदैव परिस्थिति-सापेक्ष होता है और नैतिकता केवल साध्य रह जाती है। नैतिकता की निरपेक्षवादी धारणा नैतिक-जीवन के प्रयोजन अथवा कर्म के पीछे निहित कर्ता के अभिप्राय को ही सब कुछ मान लेती है, लेकिन नैतिकता तो जीवन को ढालना है, उसे सुन्दर स्वरूप प्रदान करना है। इसके लिए आकार
और सामग्री- दोनों आवश्यक हैं। इतना ही नहीं, नैतिकता का साँचा ऐसा भी होना चाहिए, जो सब प्रकार की जीवन-सामग्री को ढालने के लिए लचीला हो। नैतिक-जीवन के आदर्श इस प्रकार प्रस्तुत किए जाने चाहिए कि उसमें निम्न से निम्नतर चारित्रवाले से लगाकर उच्चतम नैतिक-विकास वाले प्राणियों के समाहित होने की सम्भावना रहे। जैन नैतिकता नैतिक आदर्श को इतने लचीले रूप से प्रस्तुत करती है कि पापी जीव भी क्रमिक विकास करता हुआ नैतिक-साधना के सर्वोच्च शिखर पर पहुँच सके।
नैतिकता लक्ष्योन्मुख गति है। उस गति में साधक की दृष्टि उस भूमि पर ही स्थित होती है, जिस पर वह गति कर रहा है। यदि अपने गन्तव्य-मार्ग में सामने नहीं देखता, तो वह कभी भी बाधाओं से टकराकर गिर सकता है। इसी प्रकार, जो साधक केवल आदर्श की
ओर देखता है और उस भूमि की ओर नहीं देखता, जिस पर चल रहा है, तो वह भी अनेक ठोकरें खाता है और भटक जाता है। नैतिक-जीवन में भी हमारी गति का वही स्वरूप होता है, जो हमारे दैनिक जीवन में होता है। जिस प्रकार दैनिक जीवन में चलने के उपक्रम में हमारा काम न तो केवल सामने देखने से चलता है, न ही सिर्फ नीचे देखने से। चलने की सम्यक् प्रक्रिया वही है, जिसमें पथिक सामने और नीचे- दोनों ओर दृष्टि रखे। नैतिकजीवन में भी साधक को यथार्थ और आदर्श-दोनों पर दृष्टि रखनी होती है, तभी नैतिकजीवन में सम्यक् प्रगति सम्भव है।
यह शंका उठसकती है कि सामान्य जीवन में तो दो आँखें मिली हैं. लेकिन नैतिकजीवन की दो आँखें कौन-सी हैं ? किसी अपेक्षा से ज्ञान और क्रिया को नैतिक-जीवन की दो आँखें कहा जा सकता है। नैतिकता कहती है कि ज्ञान नामक आँख को आदर्श पर केन्द्रित करो और क्रिया नामक आँख को यथार्थ पर, अर्थात् कर्म के आचरण में यथार्थता की ओर देखो और गन्तव्य की ओर प्रगति करने में आदर्श की ओर। 4. उत्सर्ग और अपवाद
जैन नैतिक-विचारणा में नैतिकता के सापेक्ष और निरपेक्ष-दोनों रूप स्वीकृत हैं, लेकिन उसमें भी निरपेक्षता दो भिन्न अर्थों में प्रयुक्त है। प्रथम प्रकार की निरपेक्षता दो भिन्न अर्थों में प्रयुक्त है। प्रथम प्रकार की निरपेक्षता वह है, जिसमें आचार के सामान्य या मौलिक नियमों को निरपेक्ष माना जाता है और विशेष नियमों को सापेक्ष माना जाता है; जैसे अहिंसा
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org