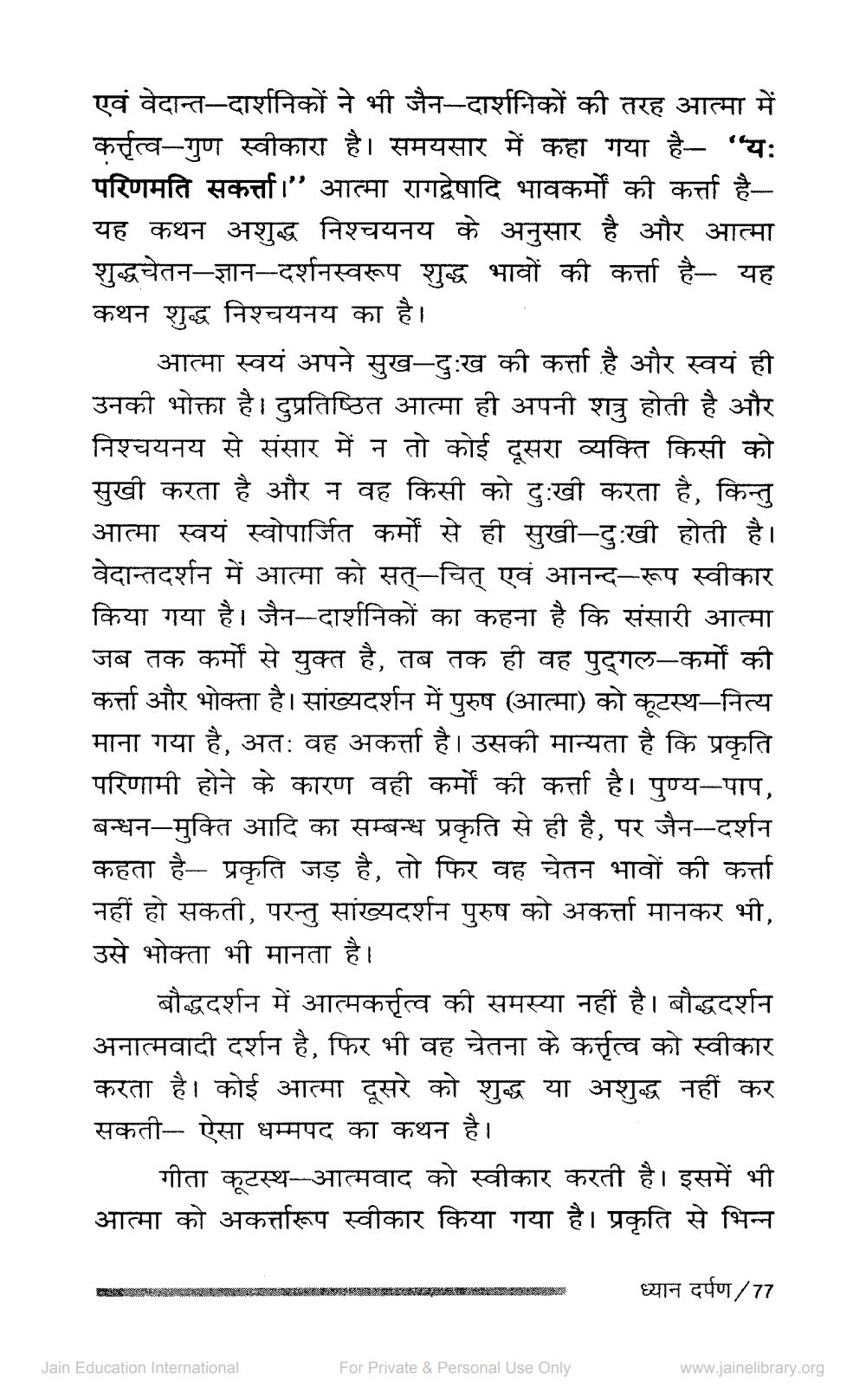________________
एवं वेदान्त–दार्शनिकों ने भी जैन–दार्शनिकों की तरह आत्मा में कर्तृत्व-गुण स्वीकारा है। समयसार में कहा गया है- “यः परिणमति सकर्ता।" आत्मा रागद्वेषादि भावकर्मों की कर्ता हैयह कथन अशुद्ध निश्चयनय के अनुसार है और आत्मा शुद्धचेतन-ज्ञान-दर्शनस्वरूप शुद्ध भावों की कर्ता है- यह कथन शुद्ध निश्चयनय का है।
आत्मा स्वयं अपने सुख-दुःख की कर्ता है और स्वयं ही उनकी भोक्ता है। दुप्रतिष्ठित आत्मा ही अपनी शत्रु होती है और निश्चयनय से संसार में न तो कोई दूसरा व्यक्ति किसी को सुखी करता है और न वह किसी को दु:खी करता है, किन्तु आत्मा स्वयं स्वोपार्जित कर्मों से ही सुखी-दु:खी होती है। वेदान्तदर्शन में आत्मा को सत्-चित् एवं आनन्द-रूप स्वीकार किया गया है। जैन-दार्शनिकों का कहना है कि संसारी आत्मा जब तक कर्मों से युक्त है, तब तक ही वह पुद्गल-कर्मों की कर्ता और भोक्ता है। सांख्यदर्शन में पुरुष (आत्मा) को कूटस्थ नित्य माना गया है, अत: वह अकर्ता है। उसकी मान्यता है कि प्रकृति परिणामी होने के कारण वही कर्मों की कर्ता है। पुण्य-पाप, बन्धन–मुक्ति आदि का सम्बन्ध प्रकृति से ही है, पर जैन-दर्शन कहता है- प्रकृति जड़ है, तो फिर वह चेतन भावों की कर्ता नहीं हो सकती, परन्तु सांख्यदर्शन पुरुष को अकर्त्ता मानकर भी, उसे भोक्ता भी मानता है।
बौद्धदर्शन में आत्मकर्तृत्व की समस्या नहीं है। बौद्धदर्शन अनात्मवादी दर्शन है, फिर भी वह चेतना के कर्तृत्व को स्वीकार करता है। कोई आत्मा दूसरे को शुद्ध या अशुद्ध नहीं कर सकती-- ऐसा धम्मपद का कथन है।
गीता कूटस्थ-आत्मवाद को स्वीकार करती है। इसमें भी आत्मा को अकर्त्तारूप स्वीकार किया गया है। प्रकृति से भिन्न
ध्यान दर्पण/77
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org