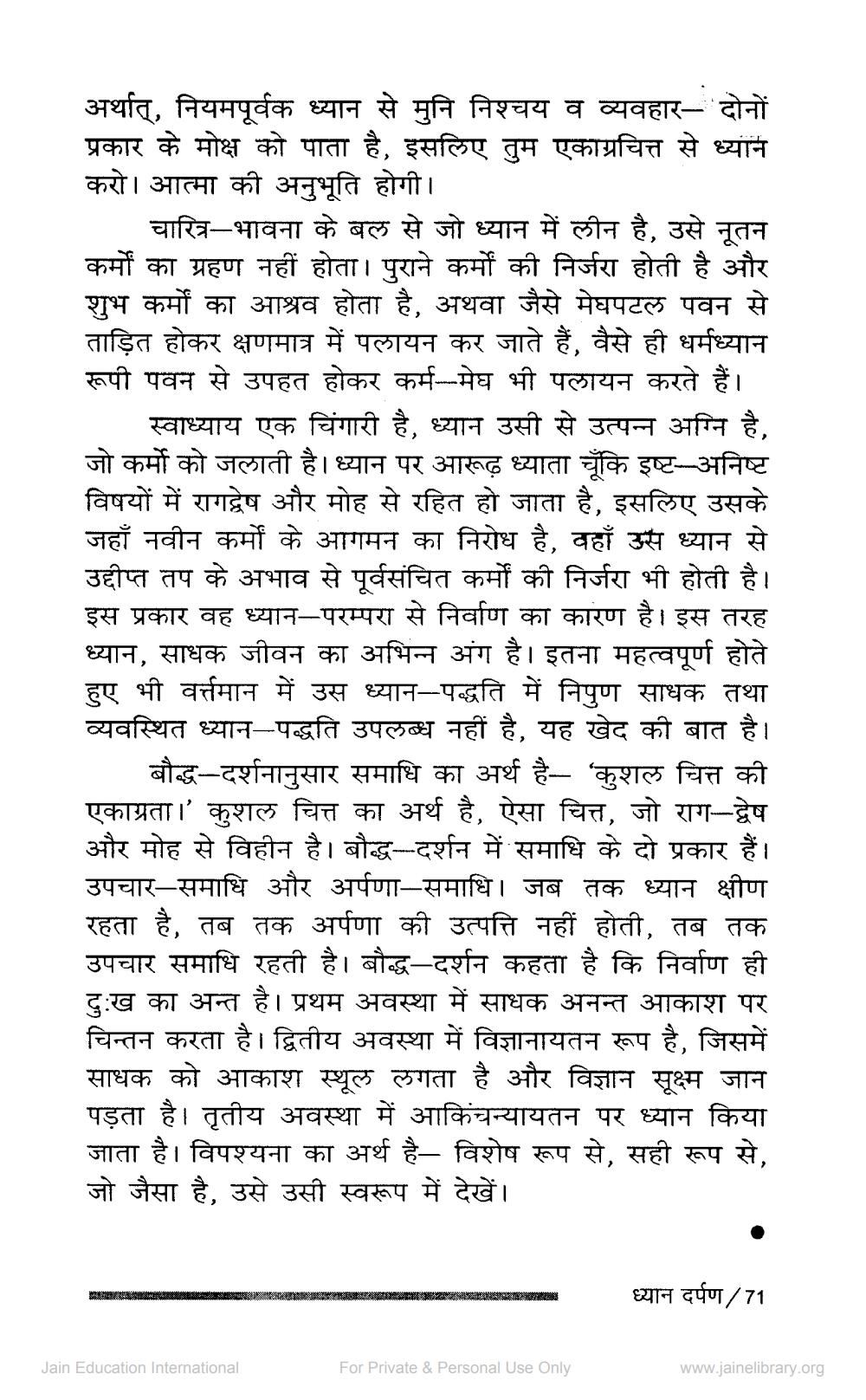________________
अर्थात्, नियमपूर्वक ध्यान से मुनि निश्चय व व्यवहार- दोनों प्रकार के मोक्ष को पाता है, इसलिए तुम एकाग्रचित्त से ध्यान करो। आत्मा की अनुभूति होगी।
चारित्र-भावना के बल से जो ध्यान में लीन है, उसे नूतन कर्मों का ग्रहण नहीं होता। पुराने कर्मों की निर्जरा होती है और शुभ कर्मों का आश्रव होता है, अथवा जैसे मेघपटल पवन से ताड़ित होकर क्षणमात्र में पलायन कर जाते हैं, वैसे ही धर्मध्यान रूपी पवन से उपहत होकर कर्म-मेघ भी पलायन करते हैं।
स्वाध्याय एक चिंगारी है, ध्यान उसी से उत्पन्न अग्नि है, जो कर्मो को जलाती है। ध्यान पर आरूढ़ ध्याता चूँकि इष्ट-अनिष्ट विषयों में रागद्वेष और मोह से रहित हो जाता है, इसलिए उसके जहाँ नवीन कर्मों के आगमन का निरोध है, वहाँ उस ध्यान से उद्दीप्त तप के अभाव से पूर्वसंचित कर्मों की निर्जरा भी होती है। इस प्रकार वह ध्यान-परम्परा से निर्वाण का कारण है। इस तरह ध्यान, साधक जीवन का अभिन्न अंग है। इतना महत्वपूर्ण होते हुए भी वर्तमान में उस ध्यान-पद्धति में निपुण साधक तथा व्यवस्थित ध्यान-पद्धति उपलब्ध नहीं है, यह खेद की बात है।
बौद्ध-दर्शनानुसार समाधि का अर्थ है- 'कुशल चित्त की एकाग्रता।' कुशल चित्त का अर्थ है, ऐसा चित्त, जो राग-द्वेष
और मोह से विहीन है। बौद्ध-दर्शन में समाधि के दो प्रकार हैं। उपचार-समाधि और अर्पणा-समाधि। जब तक ध्यान क्षीण रहता है, तब तक अर्पणा की उत्पत्ति नहीं होती, तब तक उपचार समाधि रहती है। बौद्ध दर्शन कहता है कि निर्वाण ही दु:ख का अन्त है। प्रथम अवस्था में साधक अनन्त आकाश पर चिन्तन करता है। द्वितीय अवस्था में विज्ञानायतन रूप है, जिसमें साधक को आकाश स्थूल लगता है और विज्ञान सूक्ष्म जान पड़ता है। तृतीय अवस्था में आकिंचन्यायतन पर ध्यान किया जाता है। विपश्यना का अर्थ है- विशेष रूप से, सही रूप से, जो जैसा है, उसे उसी स्वरूप में देखें।
ध्यान दर्पण/71
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org