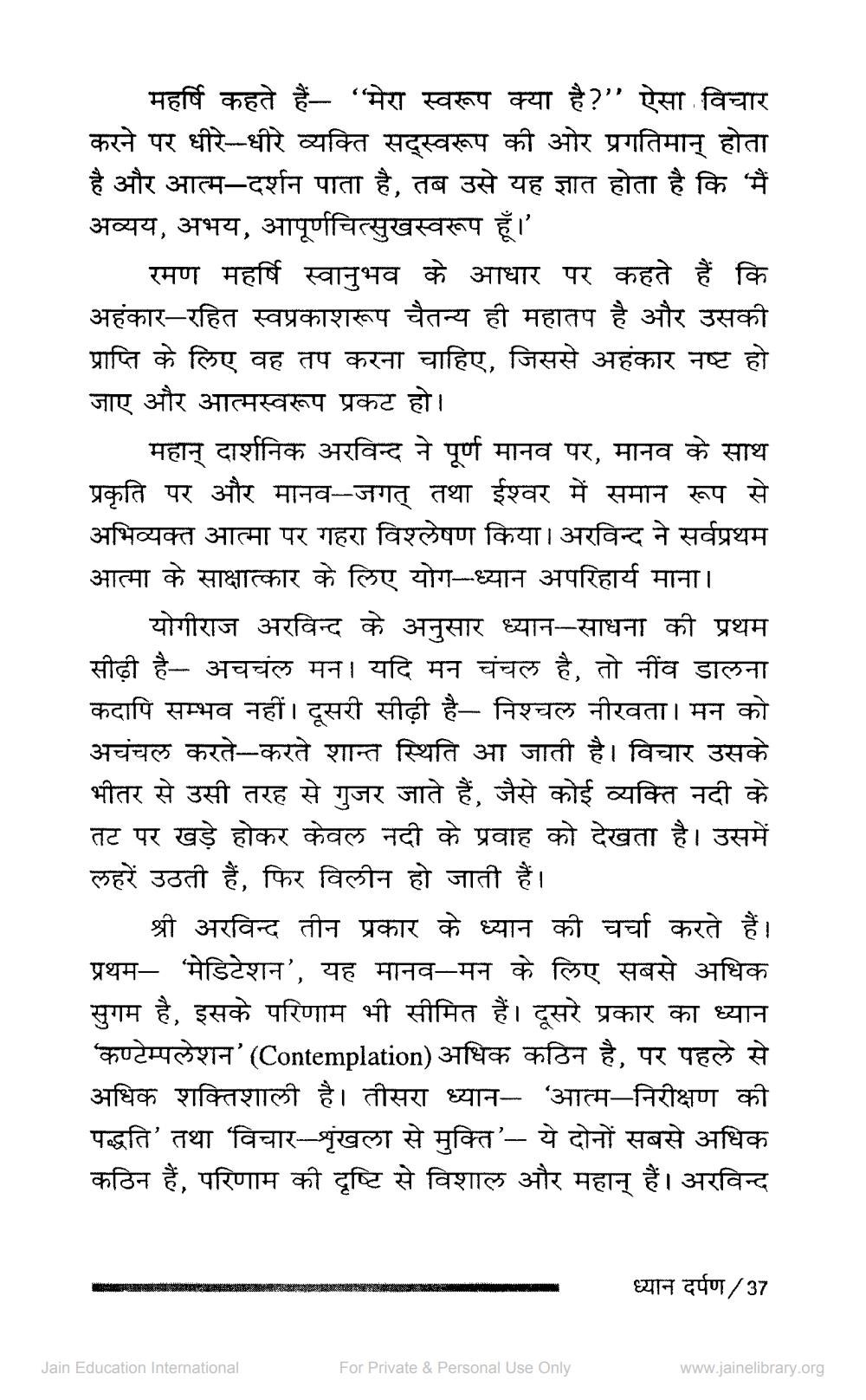________________
महर्षि कहते हैं- "मेरा स्वरूप क्या है?'' ऐसा विचार करने पर धीरे-धीरे व्यक्ति सद्स्वरूप की ओर प्रगतिमान् होता है और आत्म-दर्शन पाता है, तब उसे यह ज्ञात होता है कि 'मैं अव्यय, अभय, आपूर्णचित्सुखस्वरूप हूँ।'
रमण महर्षि स्वानुभव के आधार पर कहते हैं कि अहंकार-रहित स्वप्रकाशरूप चैतन्य ही महातप है और उसकी प्राप्ति के लिए वह तप करना चाहिए, जिससे अहंकार नष्ट हो जाए और आत्मस्वरूप प्रकट हो।
महान् दार्शनिक अरविन्द ने पूर्ण मानव पर, मानव के साथ प्रकृति पर और मानव-जगत् तथा ईश्वर में समान रूप से अभिव्यक्त आत्मा पर गहरा विश्लेषण किया। अरविन्द ने सर्वप्रथम आत्मा के साक्षात्कार के लिए योग-ध्यान अपरिहार्य माना।
योगीराज अरविन्द के अनुसार ध्यान-साधना की प्रथम सीढ़ी है- अचचंल मन। यदि मन चंचल है, तो नींव डालना कदापि सम्भव नहीं। दूसरी सीढ़ी है- निश्चल नीरवता। मन को अचंचल करते-करते शान्त स्थिति आ जाती है। विचार उसके भीतर से उसी तरह से गुजर जाते हैं, जैसे कोई व्यक्ति नदी के तट पर खड़े होकर केवल नदी के प्रवाह को देखता है। उसमें लहरें उठती हैं, फिर विलीन हो जाती हैं।
श्री अरविन्द तीन प्रकार के ध्यान की चर्चा करते हैं। प्रथम- 'मेडिटेशन', यह मानव-मन के लिए सबसे अधिक सुगम है, इसके परिणाम भी सीमित हैं। दूसरे प्रकार का ध्यान 'कण्टेम्पलेशन' (Contemplation) अधिक कठिन है, पर पहले से
अधिक शक्तिशाली है। तीसरा ध्यान- 'आत्म-निरीक्षण की पद्धति' तथा 'विचार-शृंखला से मुक्ति'- ये दोनों सबसे अधिक कठिन हैं, परिणाम की दृष्टि से विशाल और महान् हैं। अरविन्द
ध्यान दर्पण/37
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org